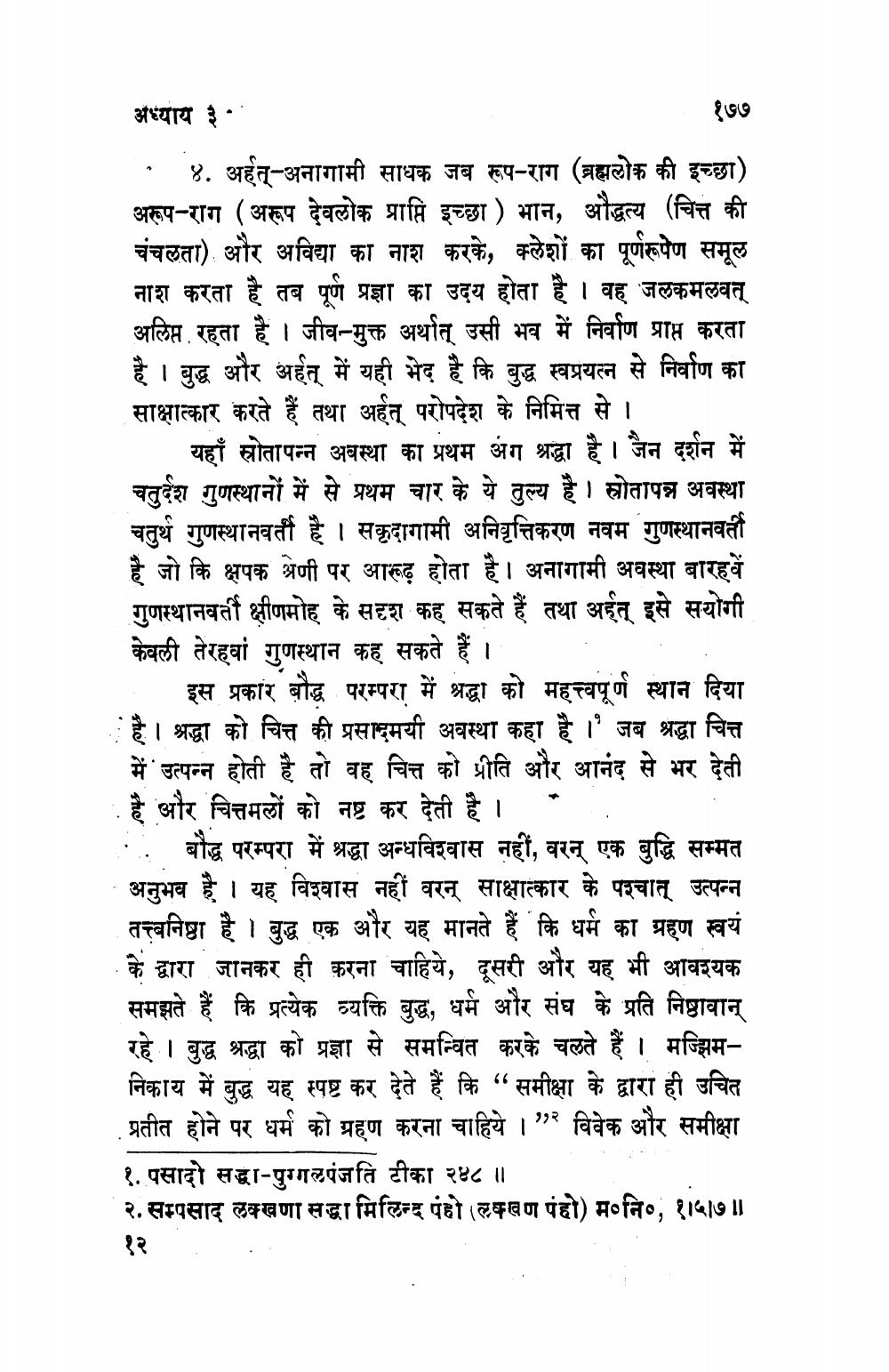________________
अध्याय ३ .
१७७
४. अर्हत्-अनागामी साधक जब रूप-राग (ब्रह्मलोक की इच्छा) अरूप-राग (अरूप देवलोक प्राप्ति इच्छा ) भान, औद्धत्य (चित्त की चंचलता) और अविद्या का नाश करके, क्लेशों का पूर्णरूपेण समूल नाश करता है तब पूर्ण प्रज्ञा का उदय होता है । वह जलकमलवत् अलिप्त रहता है । जीव-मुक्त अर्थात् उसी भव में निर्वाण प्राप्त करता है । बुद्ध और अर्हत् में यही भेद है कि बुद्ध स्वप्रयत्न से निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं तथा अर्हत् परोपदेश के निमित्त से ।
यहाँ स्रोतापन्न अवस्था का प्रथम अंग श्रद्धा है । जैन दर्शन में चतुर्दश गुणस्थानों में से प्रथम चार के ये तुल्य है । स्रोतापन्न अवस्था चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है । सकृदागामी अनिवृत्तिकरण नवम गुणस्थानवर्ती है जो कि क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है। अनागामी अवस्था बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोह के सदृश कह सकते हैं तथा अईत् इसे सयोगी केवली तेरहवां गुणस्थान कह सकते हैं।
इस प्रकार बौद्ध परम्परा में श्रद्धा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। श्रद्धा को चित्त की प्रसादमयी अवस्था कहा है ।' जब श्रद्धा चित्त में उत्पन्न होती है तो वह चित्त को प्रीति और आनंद से भर देती .. है और चित्तमलों को नष्ट कर देती है। . .
. . बौद्ध परम्परा में श्रद्धा अन्धविश्वास नहीं, वरन् एक बुद्धि सम्मत · अनुभव है । यह विश्वास नहीं वरन् साक्षात्कार के पश्चात् उत्पन्न तत्त्वनिष्ठा है । बुद्ध एक और यह मानते हैं कि धर्म का ग्रहण स्वयं के द्वारा जानकर ही करना चाहिये, दूसरी और यह भी आवश्यक समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति निष्ठावान् रहे । बुद्ध श्रद्धा को प्रज्ञा से समन्वित करके चलते हैं । मज्झिमनिकाय में बुद्ध यह स्पष्ट कर देते हैं कि " समीक्षा के द्वारा ही उचित प्रतीत होने पर धर्म को ग्रहण करना चाहिये । "२ विवेक और समीक्षा १. पसादो सद्धा-पुग्गलपंजति टीका २४८ ।। २. सम्पसाद लक्खणा सद्धा मिलिन्द पंहो लक्षण पंहो) म०नि०, ११५७॥