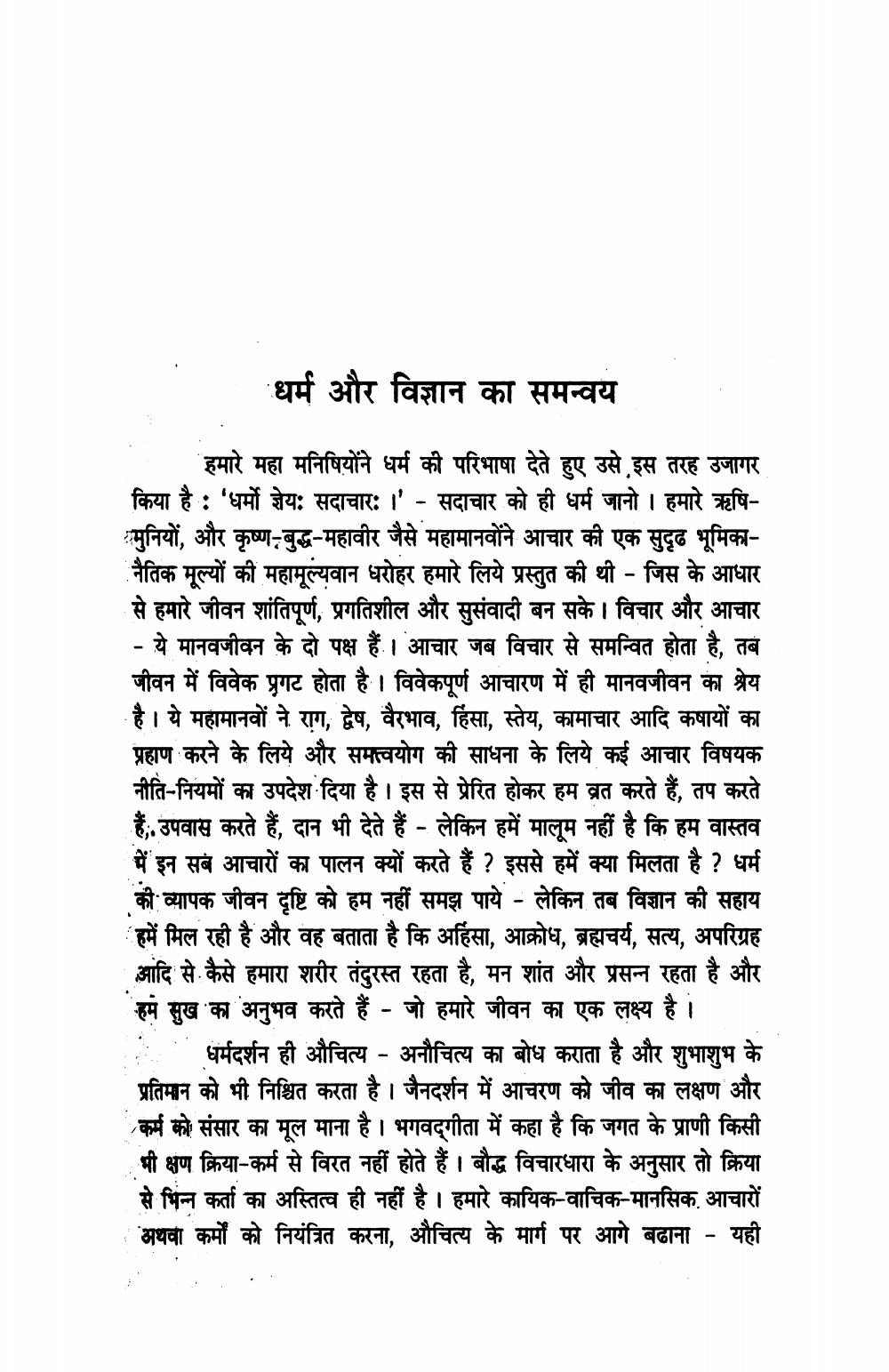________________
धर्म और विज्ञान का समन्वय
हमारे महा मनिषियोंने धर्म की परिभाषा देते हुए उसे इस तरह उजागर किया है : 'धर्मो ज्ञेयः सदाचारः ।' सदाचार को ही धर्म जानो । हमारे ऋषिसमुनियों, और कृष्ण - बुद्ध - महावीर जैसे महामानवोंने आचार की एक सुदृढ भूमिकानैतिक मूल्यों की महामूल्यवान धरोहर हमारे लिये प्रस्तुत की थी - जिस के आधार से हमारे जीवन शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सुसंवादी बन सके। विचार और आचार
ये मानवजीवन के दो पक्ष हैं । आचार जब विचार से समन्वित होता है, तब जीवन में विवेक प्रगट होता है । विवेकपूर्ण आचारण में ही मानवजीवन का श्रेय है। ये महामानवों ने राग, द्वेष, वैरभाव, हिंसा, स्तेय, कामाचार आदि कषायों का प्रहाण करने के लिये और समत्वयोग की साधना के लिये कई आचार विषयक नीति-नियमों का उपदेश दिया है। इस से प्रेरित होकर हम व्रत करते हैं, तप करते हैं;. उपवास करते हैं, दान भी देते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम वास्तव मैं इन सब आचारों का पालन क्यों करते हैं ? इससे हमें क्या मिलता है ? धर्म की व्यापक जीवन दृष्टि को हम नहीं समझ पाये लेकिन तब विज्ञान की सहाय हमें मिल रही है और वह बताता है कि अहिंसा, आक्रोध, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह आदि से कैसे हमारा शरीर तंदुरस्त रहता है, मन शांत और प्रसन्न रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं- जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है ।
-
धर्मदर्शन ही औचित्य - अनौचित्य का बोध कराता है और शुभाशुभ के प्रतिमान को भी निश्चित करता है। जैनदर्शन में आचरण को जीव का लक्षण और कर्म को संसार का मूल माना है । भगवद्गीता में कहा है कि जगत के प्राणी किसी भी क्षण क्रिया-कर्म से विरत नहीं होते हैं । बौद्ध विचारधारा के अनुसार तो क्रिया से भिन्न कर्ता का अस्तित्व ही नहीं है । हमारे कायिक- वाचिक-मानसिक, आचारों अथवा कर्मों को नियंत्रित करना, औचित्य के मार्ग पर आगे बढाना यही
-