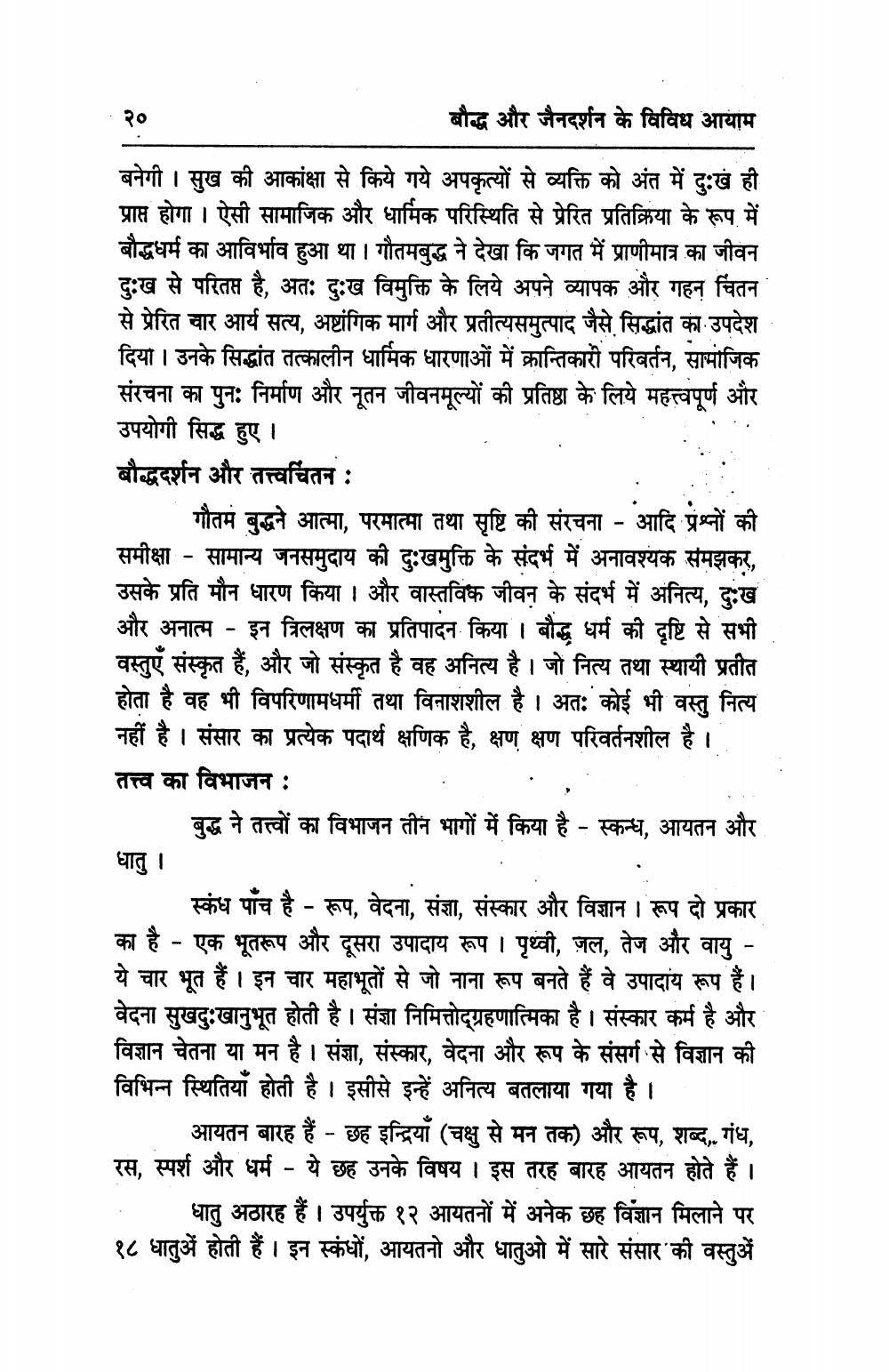________________
बौद्ध और जैनदर्शन के विविध आयाम
बनेगी । सुख की आकांक्षा से किये गये अपकृत्यों से व्यक्ति को अंत में दुःख ही प्राप्त होगा । ऐसी सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति से प्रेरित प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधर्म का आविर्भाव हुआ था । गौतमबुद्ध ने देखा कि जगत में प्राणीमात्र का जीवन दुःख से परितप्त है, अतः दुःख विमुक्ति के लिये अपने व्यापक और गहन चिंतन से प्रेरित चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्यसमुत्पाद जैसे सिद्धांत का उपदेश दिया । उनके सिद्धांत तत्कालीन धार्मिक धारणाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन, सामाजिक संरचना का पुनः निर्माण और नूतन जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए ।
बौद्धदर्शन और तत्त्वचिंतन :
२०
गौतम बुद्धने आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि की संरचना - आदि प्रश्नों की
सामान्य जनसमुदाय की दुःखमुक्ति के संदर्भ में अनावश्यक समझकर,
समीक्षा उसके प्रति मौन धारण किया । और वास्तविक जीवन के संदर्भ में अनित्य, दुःख और अनात्म इन त्रिलक्षण का प्रतिपादन किया । बौद्ध धर्म की दृष्टि से सभी वस्तुएँ संस्कृत हैं, और जो संस्कृत है वह अनित्य है । जो नित्य तथा स्थायी प्रतीत होता है वह भी विपरिणामधर्मी तथा विनाशशील है । अतः कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है ।
तत्त्व का विभाजन :
धातु ।
-
-
बुद्ध
ने तत्त्वों का विभाजन तीन भागों में किया है- स्कन्ध, आयतन और
स्कंध पाँच है - रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान । रूप दो प्रकार का है - एक भूतरूप और दूसरा उपादाय रूप । पृथ्वी, जल, तेज और वायु · ये चार भूत हैं । इन चार महाभूतों से जो नाना रूप बनते हैं वे उपादाय रूप हैं । वेदना सुखदुःखानुभूत होती है । संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका है । संस्कार कर्म है और विज्ञान चेतना या मन है । संज्ञा, संस्कार, वेदना और रूप के संसर्ग से विज्ञान की विभिन्न स्थितियाँ होती है । इसीसे इन्हें अनित्य बतलाया गया है ।
आयतन बारह हैं - छह इन्द्रियाँ (चक्षु से मन तक) और रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म- ये छह उनके विषय । इस तरह बारह आयतन होते हैं । धातु अठारह हैं । उपर्युक्त १२ आयतनों में अनेक छह विज्ञान मिलाने पर १८ धातुओं होती हैं । इन स्कंधों, आयतनो और धातुओ में सारे संसार की वस्तुओं
I