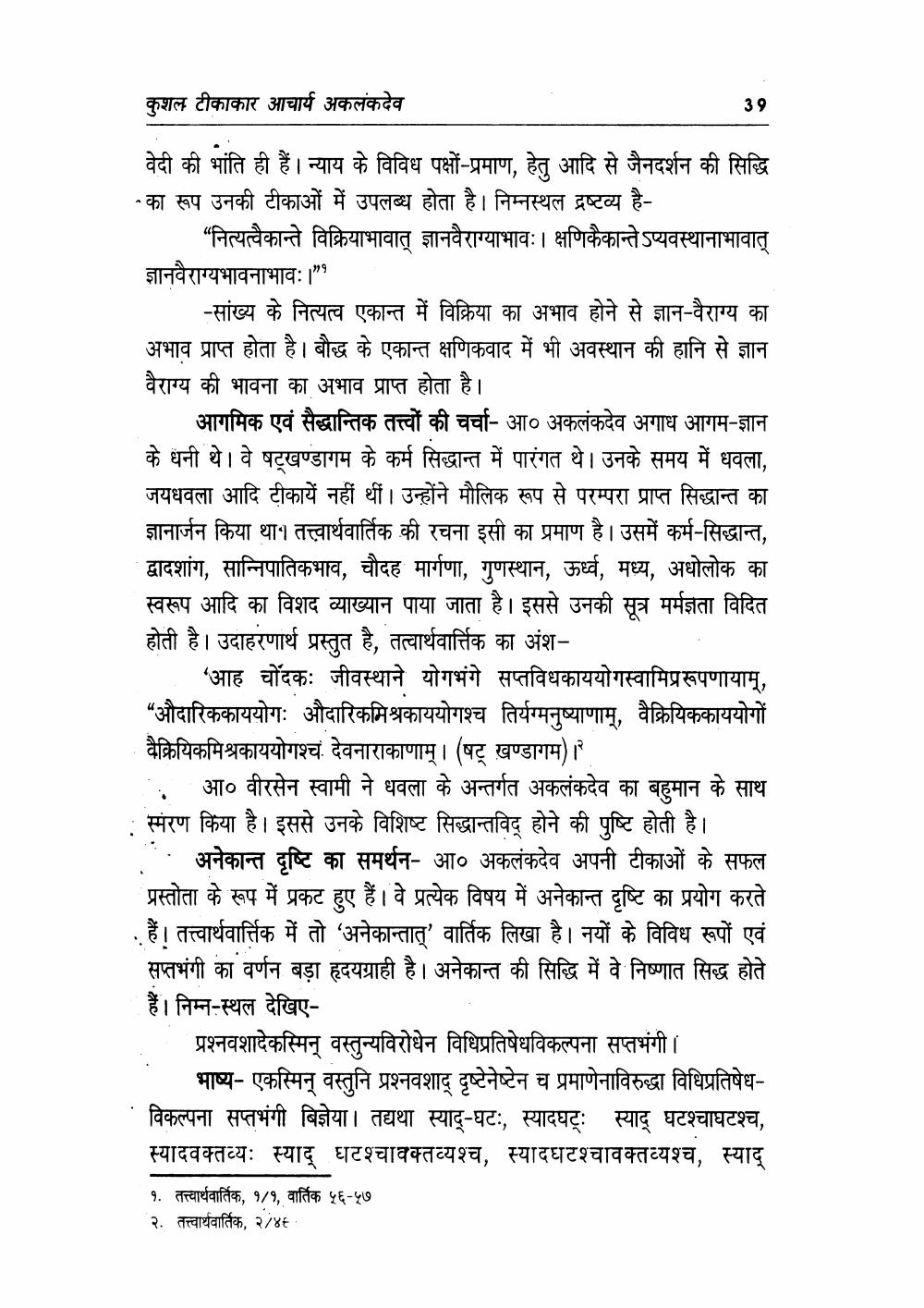________________
कुशल टीकाकार आचार्य अकलंकदेव
वेदी की भांति ही हैं। न्याय के विविध पक्षों-प्रमाण, हेतु आदि से जैनदर्शन की सिद्धि - का रूप उनकी टीकाओं में उपलब्ध होता है। निम्नस्थल द्रष्टव्य है
___ “नित्यत्वैकान्ते विक्रियाभावात् ज्ञानवैराग्याभावः । क्षणिकैकान्तेऽप्यवस्थानाभावात् ज्ञानवैराग्यभावनाभावः।१
-सांख्य के नित्यत्व एकान्त में विक्रिया का अभाव होने से ज्ञान-वैराग्य का अभाव प्राप्त होता है। बौद्ध के एकान्त क्षणिकवाद में भी अवस्थान की हानि से ज्ञान वैराग्य की भावना का अभाव प्राप्त होता है। ___ आगमिक एवं सैद्धान्तिक तत्त्वों की चर्चा- आ० अकलंकदेव अगाध आगम-ज्ञान के धनी थे। वे षट्खण्डागम के कर्म सिद्धान्त में पारंगत थे। उनके समय में धवला, जयधवला आदि टीकायें नहीं थीं। उन्होंने मौलिक रूप से परम्परा प्राप्त सिद्धान्त का ज्ञानार्जन किया था। तत्त्वार्थवार्तिक की रचना इसी का प्रमाण है। उसमें कर्म-सिद्धान्त, द्वादशांग, सान्निपातिकभाव, चौदह मार्गणा, गुणस्थान, ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक का स्वरूप आदि का विशद व्याख्यान पाया जाता है। इससे उनकी सूत्र मर्मज्ञता विदित होती है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत है, तत्वार्थवार्त्तिक का अंश
'आह चोंदकः जीवस्थाने योगभंगे सप्तविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायाम्, “औदारिककाययोगः औदारिकमिश्रकाययोगश्च तिर्यग्मनुष्याणाम्, वैक्रियिककाययोगों वैक्रियिकमिश्रकाययोगश्च देवनाराकाणाम् । (षट् खण्डागम)।
. आ० वीरसेन स्वामी ने धवला के अन्तर्गत अकलंकदेव का बहुमान के साथ : स्मरण किया है। इससे उनके विशिष्ट सिद्धान्तविद् होने की पुष्टि होती है।
- अनेकान्त दृष्टि का समर्थन- आ० अकलंकदेव अपनी टीकाओं के सफल प्रस्तोता के रूप में प्रकट हुए हैं। वे प्रत्येक विषय में अनेकान्त दृष्टि का प्रयोग करते . हैं। तत्त्वार्थवार्त्तिक में तो 'अनेकान्तात्' वार्तिक लिखा है। नयों के विविध रूपों एवं
सप्तभंगी का वर्णन बड़ा हृदयग्राही है। अनेकान्त की सिद्धि में वे निष्णात सिद्ध होते हैं। निम्न-स्थल देखिए
प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभंगी।
भाष्य- एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नवशाद् दृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाविरुद्धा विधिप्रतिषेध• विकल्पना सप्तभंगी बिज्ञेया। तद्यथा स्याद्-घटः, स्यादघटः स्याद् घटश्चाघटश्च, स्यादवक्तव्यः स्याद् घटश्चावक्तव्यश्च, स्यादघटश्चावक्तव्यश्च, स्याद् १. तत्त्वार्थवार्तिक, १/१, वार्तिक ५६-५७ २. तत्त्वार्थवार्तिक, २/४६