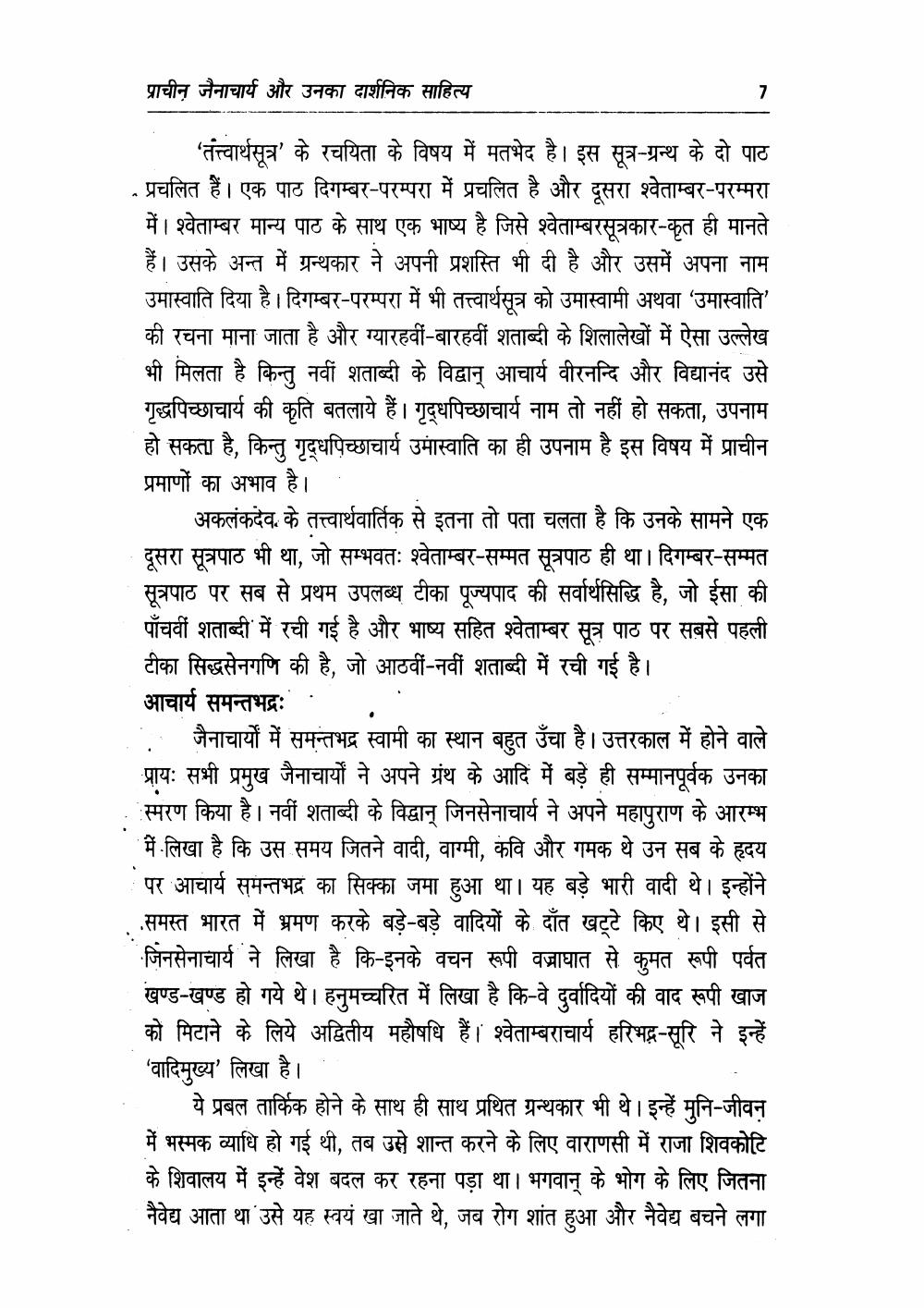________________
प्राचीन जैनाचार्य और उनका दार्शनिक साहित्य
'तत्त्वार्थसूत्र' के रचयिता के विषय में मतभेद है। इस सूत्र-ग्रन्थ के दो पाठ . प्रचलित हैं। एक पाठ दिगम्बर-परम्परा में प्रचलित है और दूसरा श्वेताम्बर-परम्परा में। श्वेताम्बर मान्य पाठ के साथ एक भाष्य है जिसे श्वेताम्बरसूत्रकार-कृत ही मानते हैं। उसके अन्त में ग्रन्थकार ने अपनी प्रशस्ति भी दी है और उसमें अपना नाम उमास्वाति दिया है। दिगम्बर-परम्परा में भी तत्त्वार्थसूत्र को उमास्वामी अथवा 'उमास्वाति' की रचना माना जाता है और ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के शिलालेखों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है किन्तु नवीं शताब्दी के विद्वान् आचार्य वीरनन्दि और विद्यानंद उसे गृद्धपिच्छाचार्य की कृति बतलाये हैं। गृद्धपिच्छाचार्य नाम तो नहीं हो सकता, उपनाम हो सकता है, किन्तु गृद्धपिच्छाचार्य उमास्वाति का ही उपनाम है इस विषय में प्राचीन प्रमाणों का अभाव है।
अकलंकदेव. के तत्त्वार्थवार्तिक से इतना तो पता चलता है कि उनके सामने एक दूसरा सूत्रपाठ भी था, जो सम्भवतः श्वेताम्बर-सम्मत सूत्रपाठ ही था। दिगम्बर-सम्मत सूत्रपाठ पर सब से प्रथम उपलब्ध टीका पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि है, जो ईसा की पाँचवीं शताब्दी में रची गई है और भाष्य सहित श्वेताम्बर सूत्र पाठ पर सबसे पहली टीका सिद्धसेनगणि की है, जो आठवी-नवीं शताब्दी में रची गई है। आचार्य समन्तभद्रः - .. . जैनाचार्यों में समन्तभद्र स्वामी का स्थान बहुत उँचा है। उत्तरकाल में होने वाले प्रायः सभी प्रमुख जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथ के आदि में बड़े ही सम्मानपूर्वक उनका स्मरण किया है। नवीं शताब्दी के विद्वान् जिनसेनाचार्य ने अपने महापुराण के आरम्भ में लिखा है कि उस समय जितने वादी, वाग्मी, कवि और गमक थे उन सब के हृदय पर आचार्य समन्तभद्र का सिक्का जमा हुआ था। यह बड़े भारी वादी थे। इन्होंने समस्त भारत में भ्रमण करके बड़े-बड़े वादियों के दाँत खट्टे किए थे। इसी से जिनसेनाचार्य ने लिखा है कि-इनके वचन रूपी वज्राघात से कुमत रूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गये थे। हनुमच्चरित में लिखा है कि-वे दुर्वादियों की वाद रूपी खाज को मिटाने के लिये अद्वितीय महौषधि हैं। श्वेताम्बराचार्य हरिभद्र-सूरि ने इन्हें 'वादिमुख्य' लिखा है।
ये प्रबल तार्किक होने के साथ ही साथ प्रथित ग्रन्थकार भी थे। इन्हें मुनि-जीवन में भस्मक व्याधि हो गई थी, तब उसे शान्त करने के लिए वाराणसी में राजा शिवकोटि के शिवालय में इन्हें वेश बदल कर रहना पड़ा था। भगवान् के भोग के लिए जितना नैवेद्य आता था उसे यह स्वयं खा जाते थे, जब रोग शांत हुआ और नैवेद्य बचने लगा