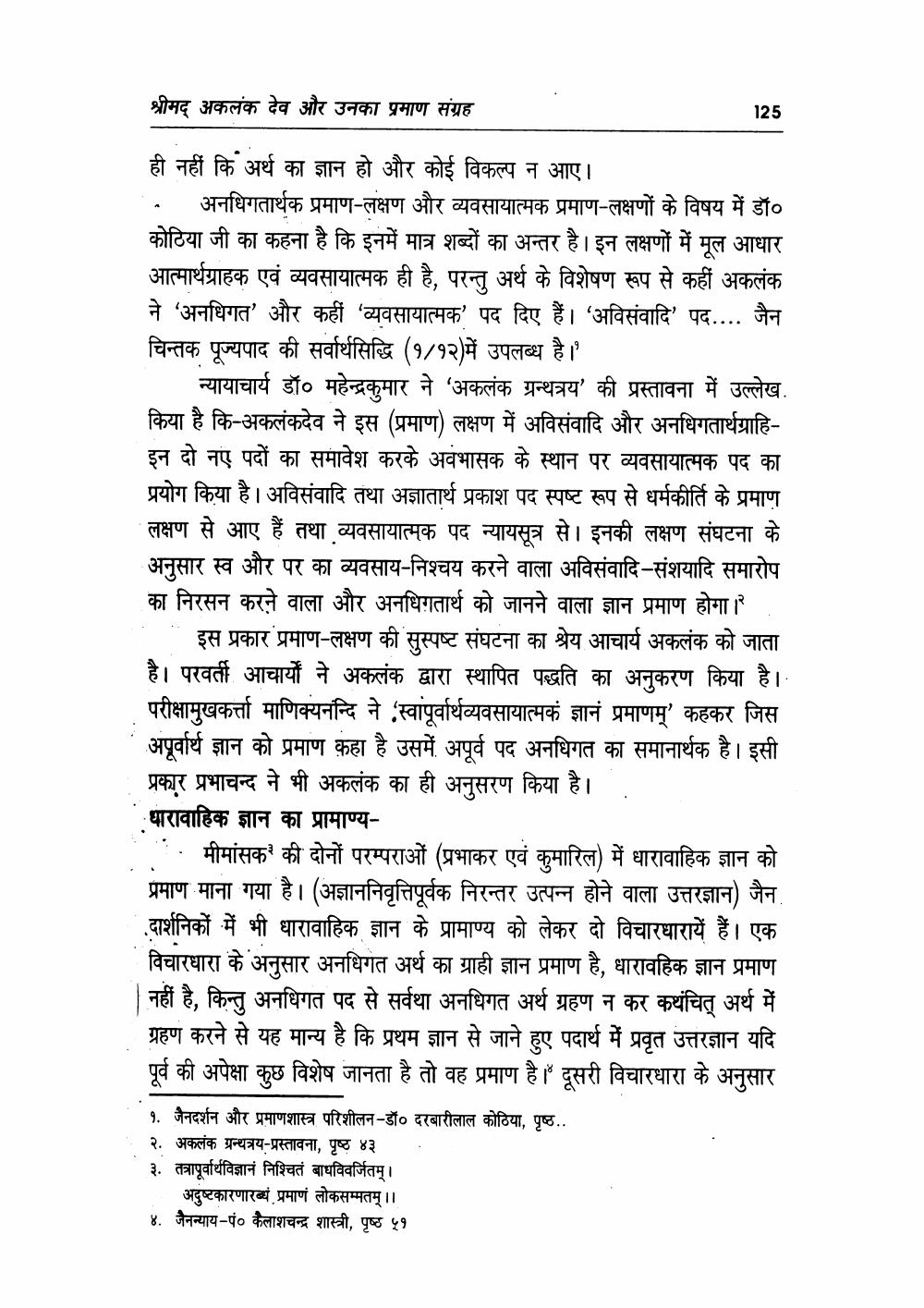________________
श्रीमद् अकलंक देव और उनका प्रमाण संग्रह
ही नहीं कि अर्थ का ज्ञान हो और कोई विकल्प न आए।
अनधिगतार्थक प्रमाण - लक्षण और व्यवसायात्मक प्रमाण - लक्षणों के विषय में डॉ० कोठिया जी का कहना है कि इनमें मात्र शब्दों का अन्तर है । इन लक्षणों में मूल आधार आत्मार्थग्राहक एवं व्यवसायात्मक ही है, परन्तु अर्थ के विशेषण रूप से कहीं अकलंक ने 'अनधिगत' और कहीं 'व्यवसायात्मक' पद दिए हैं। 'अविसंवादि' पद.... जैन चिन्तक पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि (१/१२ ) में उपलब्ध है ।'
न्यायाचार्य डॉ० महेन्द्रकुमार ने 'अकलंक ग्रन्थत्रय' की प्रस्तावना में उल्लेख. किया है कि-अकलंकदेव ने इस (प्रमाण) लक्षण में अविसंवादि और अनधिगतार्थग्राहिइन दो नए पदों का समावेश करके अवभासक के स्थान पर व्यवसायात्मक पद का प्रयोग किया है। अविसंवादि तथा अज्ञातार्थ प्रकाश पद स्पष्ट रूप से धर्मकीर्ति के प्रमाण लक्षण से आए हैं तथा व्यवसायात्मक पद न्यायसूत्र से । इनकी लक्षण संघटना के अनुसार स्व और पर का व्यवसाय - निश्चय करने वाला अविसंवादि-संशयादि समारोप का निरसन करने वाला और अनधिगतार्थ को जानने वाला ज्ञान प्रमाण होगा।
125
इस प्रकार प्रमाण-लक्षण की सुस्पष्ट संघटना का श्रेय आचार्य अकलंक को जाता है। परवर्ती आचार्यों ने अकलंक द्वारा स्थापित पद्धति का अनुकरण किया है । परीक्षामुखकर्त्ता माणिक्यनंन्दि ने स्वांपूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्' कहकर जिस अपूर्वार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा है उसमें अपूर्व पद अनधिगत का समानार्थक है। इसी प्रकार प्रभाचन्द ने भी अकलंक का ही अनुसरण किया है ।
धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य
मीमांसक' की दोनों परम्पराओं (प्रभाकर एवं कुमारिल) में धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना गया है। ( अज्ञाननिवृत्तिपूर्वक निरन्तर उत्पन्न होने वाला उत्तरज्ञान ) जैन. दार्शनिकों में भी धारावाहिक ज्ञान के प्रामाण्य को लेकर दो विचारधारायें हैं। एक विचारधारा के अनुसार अनधिगत अर्थ का ग्राही ज्ञान प्रमाण है, धारावहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, किन्तु अनधिगत पद से सर्वथा अनधिगत अर्थ ग्रहण न कर कथंचित् अर्थ में ग्रहण करने से यह मान्य है कि प्रथम ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में प्रवृत उत्तरज्ञान यदि पूर्व की अपेक्षा कुछ विशेष जानता है तो वह प्रमाण है। दूसरी विचारधारा के अनुसार
१. जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन - डॉ० दरबारीलाल कोठिया, पृष्ठ..
२. अकलंक ग्रन्थत्रय - प्रस्तावना, पृष्ठ ४३
३. तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधविवर्जितम् ।
अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ।। ४. जैनन्याय- पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, पृष्ठ ५१