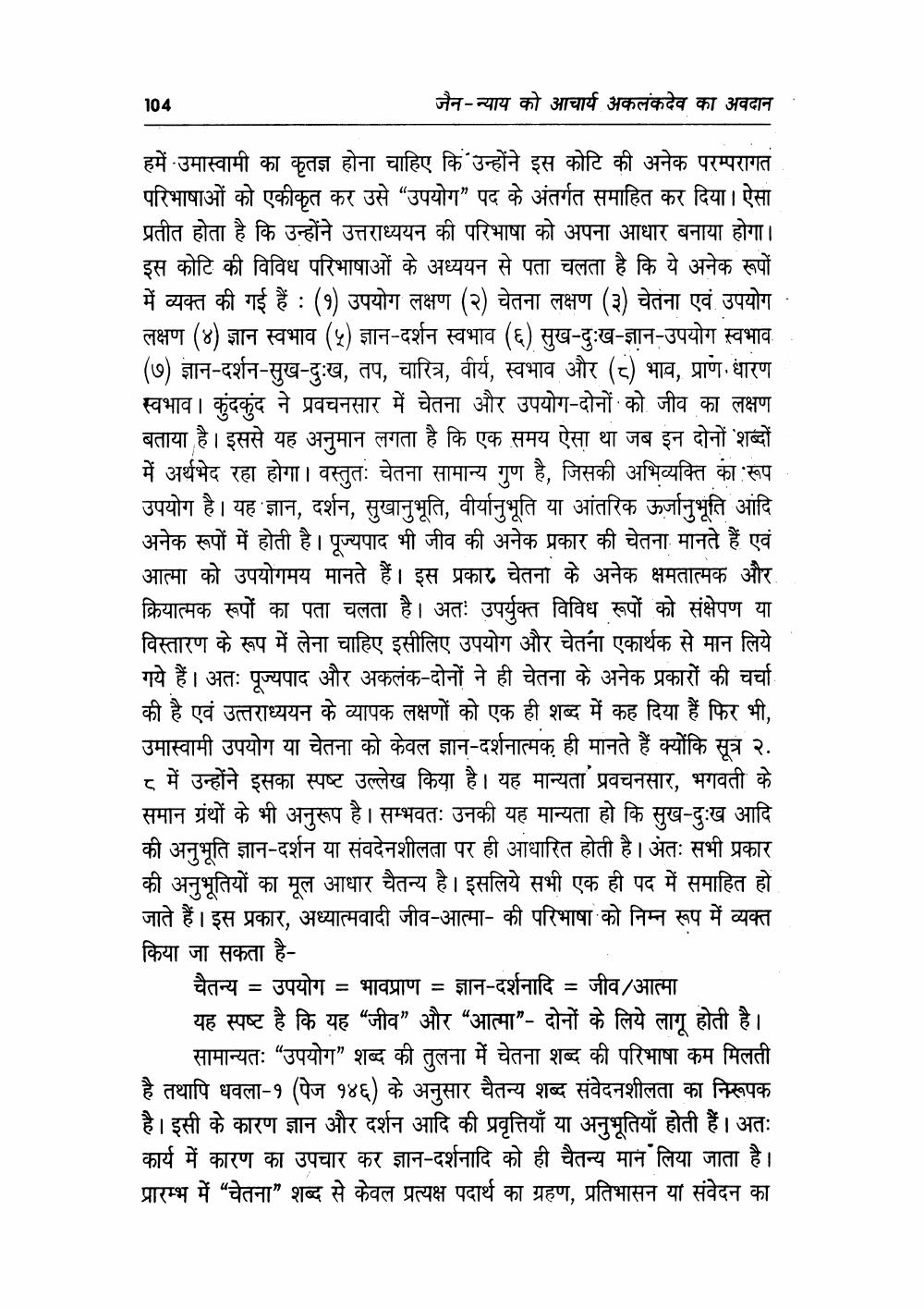________________
जैन - न्याय को आचार्य अकलंकदेव का अवदान
हमें उमास्वामी का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इस कोटि की अनेक परम्परागत परिभाषाओं को एकीकृत कर उसे “उपयोग” पद के अंतर्गत समाहित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उत्तराध्ययन की परिभाषा को अपना आधार बनाया होगा । इस कोटि की विविध परिभाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि ये अनेक रूपों में व्यक्त की गई हैं : (१) उपयोग लक्षण (२) चेतना लक्षण (३) चेतना एवं उपयोग लक्षण (४) ज्ञान स्वभाव (५) ज्ञान - दर्शन स्वभाव (६) सुख-दुःख-ज्ञान-उपयोग स्वभाव (७) ज्ञान-दर्शन-सुख-दुःख, तप, चारित्र, वीर्य, स्वभाव और (८) भाव, प्राण धारण स्वभाव । कुंदकुंद ने प्रवचनसार में चेतना और उपयोग दोनों को जीव का लक्षण बताया है। इससे यह अनुमान लगता है कि एक समय ऐसा था जब इन दोनों शब्दों में अर्थभेद रहा होगा। वस्तुतः चेतना सामान्य गुण है, जिसकी अभिव्यक्ति का रूप उपयोग है। यह 'ज्ञान, दर्शन, सुखानुभूति, वीर्यानुभूति या आंतरिक ऊर्जानुभूति आंदि अनेक रूपों में होती है। पूज्यपाद भी जीव की अनेक प्रकार की चेतना मानते हैं एवं आत्मा को उपयोगमय मानते हैं । इस प्रकार चेतना के अनेक क्षमतात्मक और क्रियात्मक रूपों का पता चलता है। अतः उपर्युक्त विविध रूपों को संक्षेपण या विस्तारण के रूप में लेना चाहिए इसीलिए उपयोग और चेतना एकार्थक से मान लिये गये हैं । अतः पूज्यपाद और अकलंक - दोनों ने ही चेतना के अनेक प्रकारों की चर्चा की है एवं उत्तराध्ययन के व्यापक लक्षणों को एक ही शब्द में कह दिया हैं फिर भी, उमास्वामी उपयोग या चेतना को केवल ज्ञान - दर्शनात्मक ही मानते हैं क्योंकि सूत्र २. ८में उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । यह मान्यता प्रवचनसार, भगवती के समान ग्रंथों के भी अनुरूप है । सम्भवतः उनकी यह मान्यता हो कि सुख-दुःख आदि की अनुभूति ज्ञान-दर्शन या संवदेनशीलता पर ही आधारित होती है । अंतः सभी प्रकार की अनुभूतियों का मूल आधार चैतन्य है । इसलिये सभी एक ही पद में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार, अध्यात्मवादी जीव - आत्मा की परिभाषा को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है
104
चैतन्य = उपयोग = भावप्राण = ज्ञान- दर्शनादि = जीव / आत्मा
यह स्पष्ट है कि यह “जीव” और “आत्मा ” - दोनों के लिये लागू होती है । सामान्यतः “उपयोग” शब्द की तुलना में चेतना शब्द की परिभाषा कम मिलती है तथापि धवला - १ (पेज १४६ ) के अनुसार चैतन्य शब्द संवेदनशीलता का निरूपक है। इसी के कारण ज्ञान और दर्शन आदि की प्रवृत्तियाँ या अनुभूतियाँ होती हैं। अतः कार्य में कारण का उपचार कर ज्ञान - दर्शनादि को ही चैतन्य मान लिया जाता है । प्रारम्भ में “चेतना” शब्द से केवल प्रत्यक्ष पदार्थ का ग्रहण, प्रतिभासन या संवेदन का