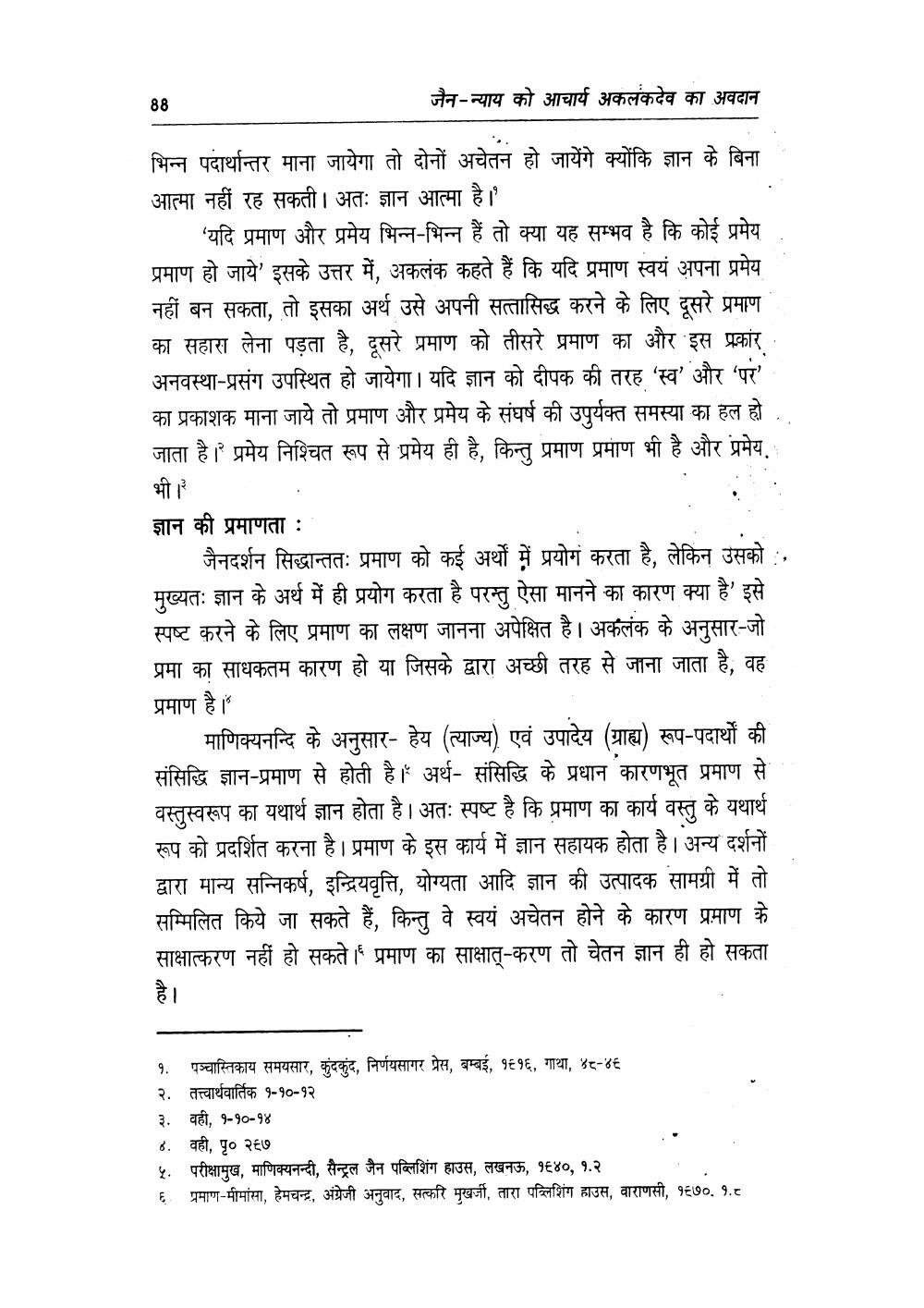________________
जैन-न्याय को आचार्य अकलंकदेव का अवदान
भिन्न पदार्थान्तर माना जायेगा तो दोनों अचेतन हो जायेंगे क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रह सकती। अतः ज्ञान आत्मा है।' ___ 'यदि प्रमाण और प्रमेय भिन्न-भिन्न हैं तो क्या यह सम्भव है कि कोई प्रमेय प्रमाण हो जाये' इसके उत्तर में, अकलंक कहते हैं कि यदि प्रमाण स्वयं अपना प्रमेय नहीं बन सकता, तो इसका अर्थ उसे अपनी सत्तासिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे प्रमाण को तीसरे प्रमाण का और इस प्रकार अनवस्था-प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। यदि ज्ञान को दीपक की तरह 'स्व' और 'पर' का प्रकाशक माना जाये तो प्रमाण और प्रमेय के संघर्ष की उपुर्यक्त समस्या का हल हो . जाता है। प्रमेय निश्चित रूप से प्रमेय ही है, किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और प्रमेय. भी। ज्ञान की प्रमाणता :
जैनदर्शन सिद्धान्ततः प्रमाण को कई अर्थों में प्रयोग करता है, लेकिन उसको :, मुख्यतः ज्ञान के अर्थ में ही प्रयोग करता है परन्तु ऐसा मानने का कारण क्या है' इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमाण का लक्षण जानना अपेक्षित है। अकलंक के अनुसार-जो प्रमा का साधकतम कारण हो या जिसके द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है, वह प्रमाण है।
माणिक्यनन्दि के अनुसार- हेय (त्याज्य) एवं उपादेय (ग्राह्य) रूप-पदार्थों की संसिद्धि ज्ञान-प्रमाण से होती है। अर्थ- संसिद्धि के प्रधान कारणभूत प्रमाण से वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रमाण का कार्य वस्तु के यथार्थ रूप को प्रदर्शित करना है। प्रमाण के इस कार्य में ज्ञान सहायक होता है। अन्य दर्शनों द्वारा मान्य सन्निकर्ष, इन्द्रियवृत्ति, योग्यता आदि ज्ञान की उत्पादक सामग्री में तो सम्मिलित किये जा सकते हैं, किन्तु वे स्वयं अचेतन होने के कारण प्रमाण के साक्षात्करण नहीं हो सकते। प्रमाण का साक्षात्-करण तो चेतन ज्ञान ही हो सकता
१. पञ्चास्तिकाय समयसार, कुंदकुंद, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१६, गाथा, ४५-४६ २. तत्त्वार्थवार्तिक १-१०-१२ ३. वही, १-१०-१४ ४. वही, पृ० २६७ ५. परीक्षामुख, माणिक्यनन्दी, सैन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, १६४०, १.२ ६ प्रमाण-मीमांसा, हेमचन्द्र, अंग्रेजी अनुवाद, सत्करि मुखर्जी, तारा पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी, १६७०. १.८