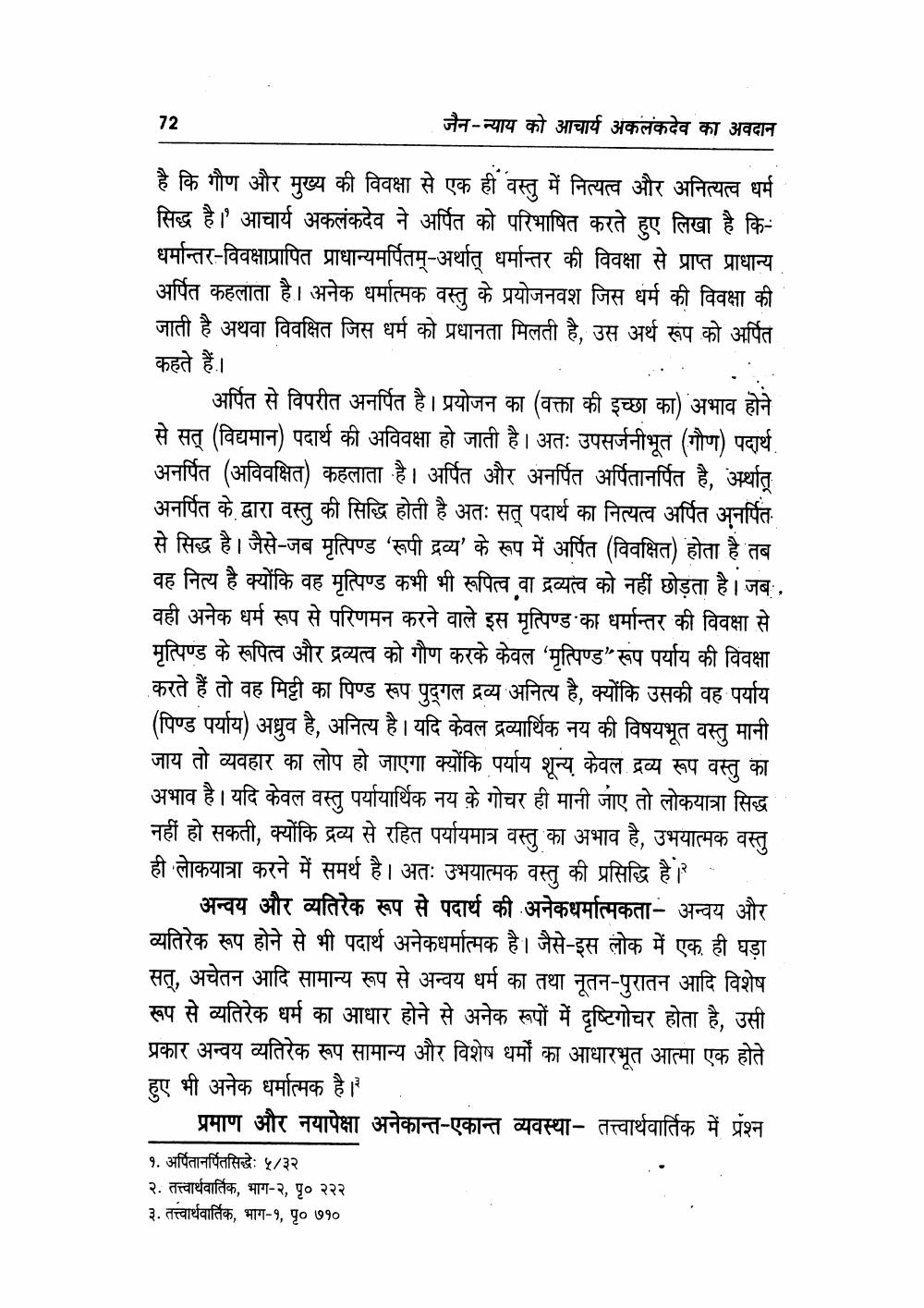________________
जैन-न्याय को आचार्य अकलंकदेव का अवदान
है कि गौण और मुख्य की विवक्षा से एक ही वस्तु में नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म सिद्ध है।' आचार्य अकलंकदेव ने अर्पित को परिभाषित करते हुए लिखा है किधर्मान्तर-विवक्षाप्रापित प्राधान्यमर्पितम्-अर्थात् धर्मान्तर की विवक्षा से प्राप्त प्राधान्य अर्पित कहलाता है। अनेक धर्मात्मक वस्तु के प्रयोजनवश जिस धर्म की विवक्षा की जाती है अथवा विवक्षित जिस धर्म को प्रधानता मिलती है, उस अर्थ रूप को अर्पित कहते हैं।
अर्पित से विपरीत अनर्पित है। प्रयोजन का (वक्ता की इच्छा का) अभाव होने से सत् (विद्यमान) पदार्थ की अविवक्षा हो जाती है। अतः उपसर्जनीभूत (गौण) पदार्थ अनर्पित (अविवक्षित) कहलाता है। अर्पित और अनर्पित अर्पितानर्पित है, अर्थातू अनर्पित के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है अतः सत् पदार्थ का नित्यत्व अर्पित अनर्पितसे सिद्ध है। जैसे-जब मृत्पिण्ड 'रूपी द्रव्य' के रूप में अर्पित (विवक्षित) होता है तब वह नित्य है क्योंकि वह मृत्पिण्ड कभी भी रूपित्व वा द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता है। जब , वही अनेक धर्म रूप से परिणमन करने वाले इस मृत्पिण्ड का धर्मान्तर की विवक्षा से मृत्पिण्ड के रूपित्व और द्रव्यत्व को गौण करके केवल ‘मृत्पिण्ड” रूप पर्याय की विवक्षा करते हैं तो वह मिट्टी का पिण्ड रूप पुद्गल द्रव्य अनित्य है, क्योंकि उसकी वह पर्याय (पिण्ड पर्याय) अध्रुव है, अनित्य है। यदि केवल द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु मानी जाय तो व्यवहार का लोप हो जाएगा क्योंकि पर्याय शून्य केवल द्रव्य रूप वस्तु का अभाव है। यदि केवल वस्तु पर्यायार्थिक नय के गोचर ही मानी जाए तो लोकयात्रा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य से रहित पर्यायमात्र वस्तु का अभाव है, उभयात्मक वस्तु ही लोकयात्रा करने में समर्थ है। अतः उभयात्मक वस्तु की प्रसिद्धि है। ____ अन्वय और व्यतिरेक रूप से पदार्थ की अनेकधर्मात्मकता- अन्वय और व्यतिरेक रूप होने से भी पदार्थ अनेकधर्मात्मक है। जैसे-इस लोक में एक ही घड़ा सत्, अचेतन आदि सामान्य रूप से अन्वय धर्म का तथा नूतन-पुरातन आदि विशेष रूप से व्यतिरेक धर्म का आधार होने से अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार अन्वय व्यतिरेक रूप सामान्य और विशेष धर्मों का आधारभूत आत्मा एक होते हुए भी अनेक धर्मात्मक है। .
प्रमाण और नयापेक्षा अनेकान्त-एकान्त व्यवस्था- तत्त्वार्थवार्तिक में प्रश्न १. अर्पितानर्पितसिद्धेः ५/३२ २. तत्त्वार्थवार्तिक, भाग-२, पृ० २२२ ३. तत्त्वार्थवार्तिक, भाग-१, पृ० ७१०