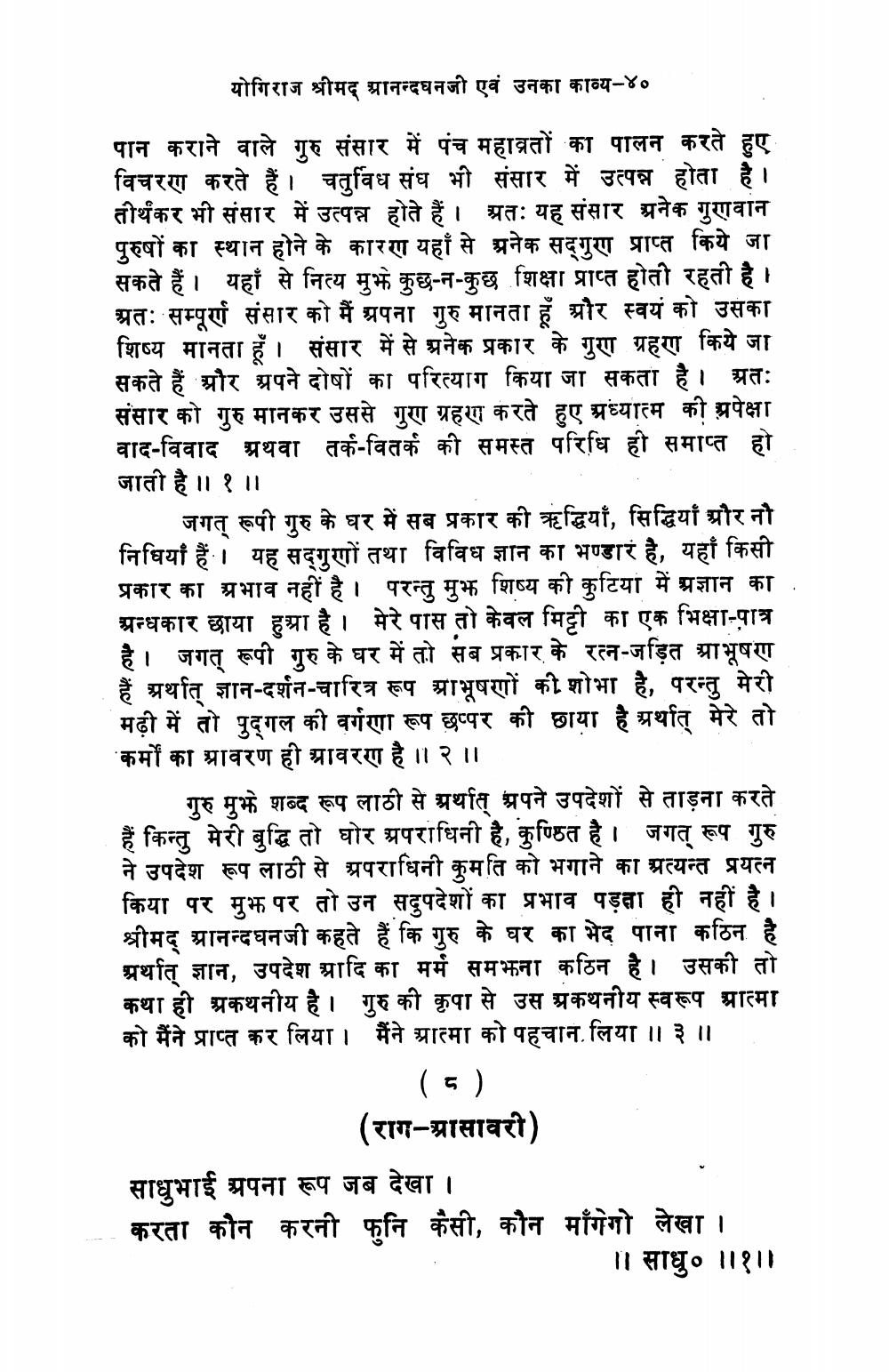________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी एवं उनका काव्य-४०
पान कराने वाले गुरु संसार में पंच महाव्रतों का पालन करते हुए विचरण करते हैं। चतुर्विध संघ भी संसार में उत्पन्न होता है। तीर्थकर भी संसार में उत्पन्न होते हैं। अतः यह संसार अनेक गुणवान पुरुषों का स्थान होने के कारण यहाँ से अनेक सद्गुण प्राप्त किये जा सकते हैं। यहाँ से नित्य मुझे कुछ-न-कुछ शिक्षा प्राप्त होती रहती है। अतः सम्पूर्ण संसार को मैं अपना गुरु मानता हूँ और स्वयं को उसका शिष्य मानता हूँ। संसार में से अनेक प्रकार के गुण ग्रहण किये जा सकते हैं और अपने दोषों का परित्याग किया जा सकता है। अतः संसार को गुरु मानकर उससे गुण ग्रहण करते हुए अध्यात्म की अपेक्षा वाद-विवाद अथवा तर्क-वितर्क की समस्त परिधि ही समाप्त हो जाती है ॥ १॥
जगत् रूपी गुरु के घर में सब प्रकार की ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ और नौ निधियां हैं। यह सद्गुणों तथा विविध ज्ञान का भण्डारं है, यहाँ किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। परन्तु मुझ शिष्य की कुटिया में प्रज्ञान का अन्धकार छाया हुआ है। मेरे पास तो केवल मिट्टी का एक भिक्षा-पात्र है। जगत् रूपी गुरु के घर में तो सब प्रकार के रत्न-जड़ित आभूषण हैं अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप आभूषणों की शोभा है, परन्तु मेरी मढ़ी में तो पुद्गल की वर्गणा रूप छप्पर की छाया है अर्थात् मेरे तो कर्मों का प्रावरण ही आवरण है ।। २ ।।
गुरु मुझे शब्द रूप लाठी से अर्थात् अपने उपदेशों से ताड़ना करते हैं किन्तु मेरी बुद्धि तो घोर अपराधिनी है, कुण्ठित है। जगत रूप गुरु ने उपदेश रूप लाठी से अपराधिनी कुमति को भगाने का अत्यन्त प्रयत्न किया पर मुझ पर तो उन सदुपदेशों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। श्रीमद् आनन्दघनजी कहते हैं कि गुरु के घर का भेद पाना कठिन है अर्थात् ज्ञान, उपदेश आदि का मर्म समझना कठिन है। उसकी तो कथा ही अकथनीय है। गुरु की कृपा से उस अकथनीय स्वरूप प्रात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया। मैंने आत्मा को पहचान लिया ॥३॥
(८)
(राग-प्रासावरी) साधुभाई अपना रूप जब देखा। करता कौन करनी फुनि कैसी, कौन मांगेगो लेखा ।
॥ साधु० ॥१॥