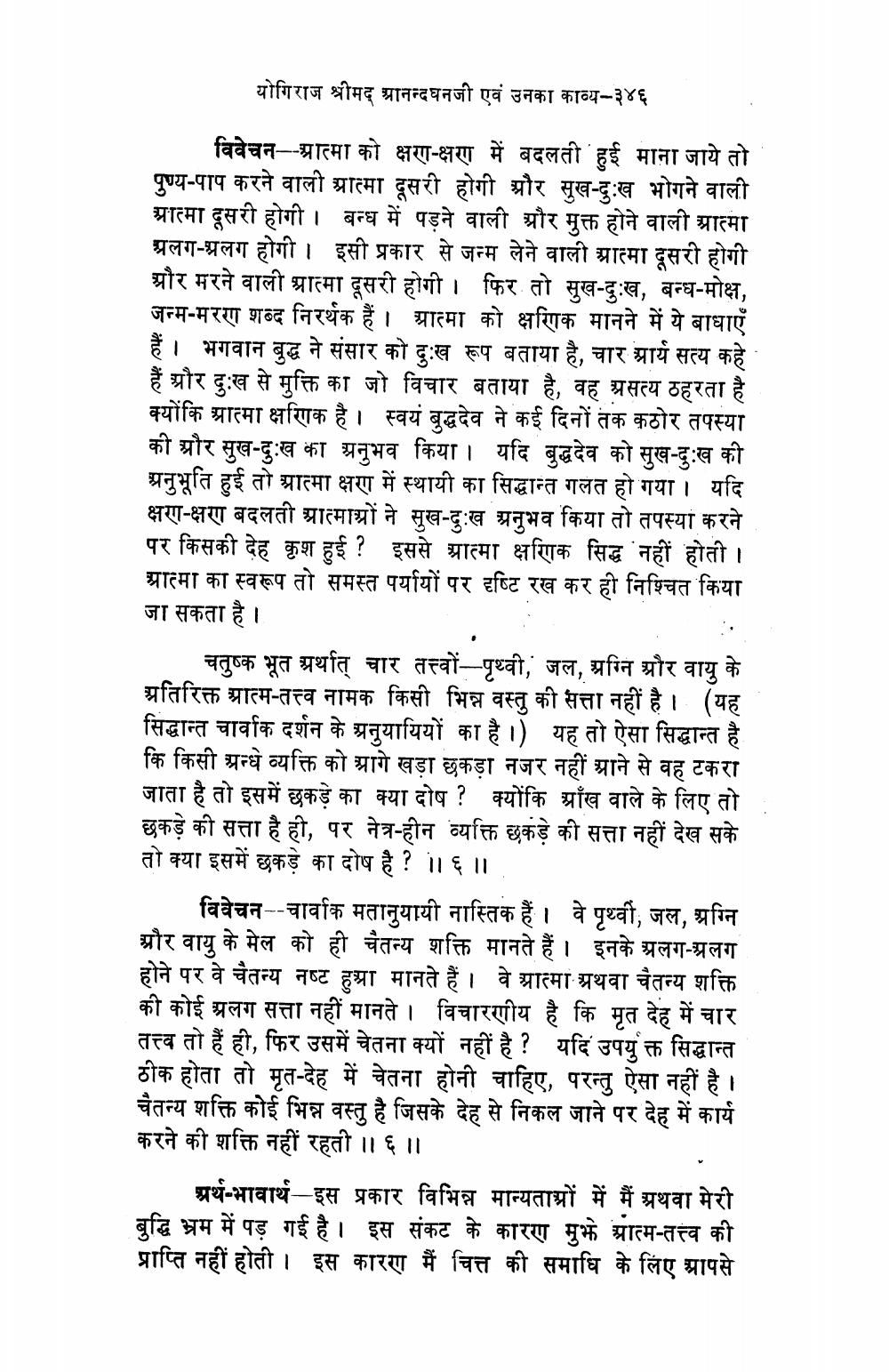________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी एवं उनका काव्य-३४६
विवेचन--आत्मा को क्षण-क्षण में बदलती हुई माना जाये तो पुण्य-पाप करने वाली आत्मा दूसरी होगी और सुख-दुःख भोगने वाली आत्मा दूसरी होगी। बन्ध में पड़ने वाली और मुक्त होने वाली आत्मा अलग-अलग होगी। इसी प्रकार से जन्म लेने वाली आत्मा दूसरी होगी और मरने वाली प्रात्मा दूसरी होगी। फिर तो सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष, जन्म-मरण शब्द निरर्थक हैं। आत्मा को क्षणिक मानने में ये बाधाएँ हैं। भगवान बुद्ध ने संसार को दुःख रूप बताया है, चार आर्य सत्य कहे हैं और दुःख से मुक्ति का जो विचार बताया है, वह असत्य ठहरता है क्योंकि आत्मा क्षणिक है। स्वयं बुद्धदेव ने कई दिनों तक कठोर तपस्या की और सुख-दुःख का अनुभव किया। यदि बुद्धदेव को सुख-दुःख की अनुभूति हुई तो आत्मा क्षण में स्थायी का सिद्धान्त गलत हो गया। यदि क्षण-क्षण बदलती आत्माओं ने सुख-दुःख अनुभव किया तो तपस्या करने पर किसकी देह कृश हुई ? इससे प्रात्मा क्षणिक सिद्ध नहीं होती। आत्मा का स्वरूप तो समस्त पर्यायों पर दृष्टि रख कर ही निश्चित किया जा सकता है।
चतुष्क भूत अर्थात् चार तत्त्वों-पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अतिरिक्त आत्म-तत्त्व नामक किसी भिन्न वस्तु की सत्ता नहीं है। (यह सिद्धान्त चार्वाक दर्शन के अनुयायियों का है।) यह तो ऐसा सिद्धान्त है कि किसी अन्धे व्यक्ति को आगे खड़ा छकड़ा नजर नहीं आने से वह टकरा जाता है तो इसमें छकड़े का क्या दोष ? क्योंकि आँख वाले के लिए तो छकड़े की सत्ता है ही, पर नेत्र-हीन व्यक्ति छकड़े की सत्ता नहीं देख सके तो क्या इसमें छकड़े का दोष है ? ॥ ६ ।। .
विवेचन--चार्वाक मतानुयायी नास्तिक हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मेल को ही चैतन्य शक्ति मानते हैं। इनके अलग-अलग होने पर वे चैतन्य नष्ट हुआ मानते हैं। वे आत्मा अथवा चैतन्य शक्ति की कोई अलग सत्ता नहीं मानते। विचारणीय है कि मृत देह में चार तत्त्व तो हैं ही, फिर उसमें चेतना क्यों नहीं है ? यदि उपयुक्त सिद्धान्त ठीक होता तो मृत-देह में चेतना होनी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है। चैतन्य शक्ति कोई भिन्न वस्तु है जिसके देह से निकल जाने पर देह में कार्य करने की शक्ति नहीं रहती ।। ६ ।।
अर्थ-भावार्थ-इस प्रकार विभिन्न मान्यतामों में मैं अथवा मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। इस संकट के कारण मुझे आत्म-तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण मैं चित्त की समाधि के लिए आपसे