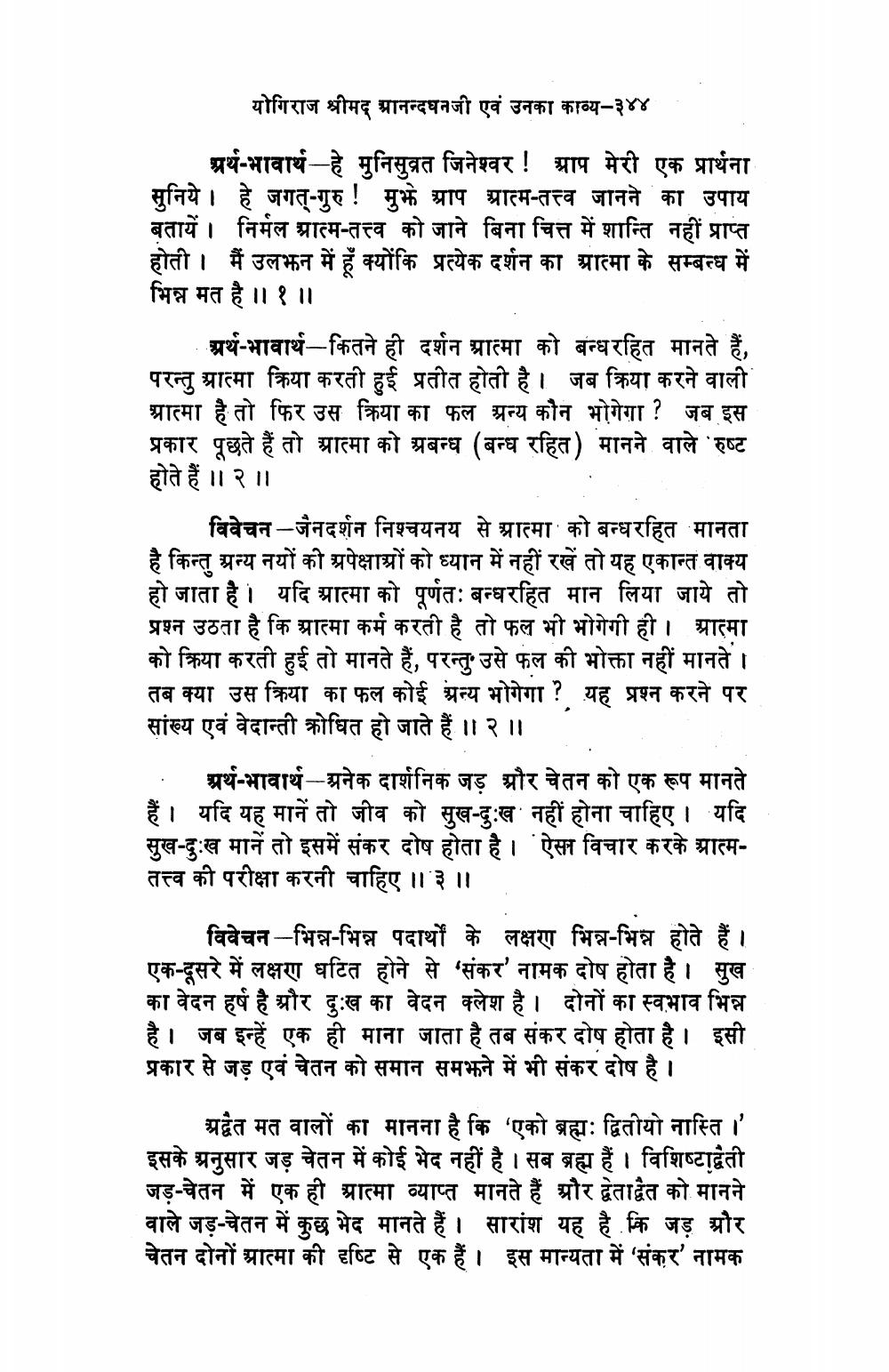________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दधनजी एवं उनका काव्य-३४४
अर्थ-भावार्थ-हे मुनिसुव्रत जिनेश्वर! आप मेरी एक प्रार्थना सुनिये। हे जगत्-गुरु ! मुझे आप प्रात्म-तत्त्व जानने का उपाय बतायें। निर्मल आत्म-तत्त्व को जाने बिना चित्त में शान्ति नहीं प्राप्त होती। मैं उलझन में हूँ क्योंकि प्रत्येक दर्शन का आत्मा के सम्बन्ध में भिन्न मत है ॥ १॥
.. अर्थ-भावार्थ-कितने ही दर्शन प्रात्मा को बन्धरहित मानते हैं, परन्तु प्रात्मा क्रिया करती हुई प्रतीत होती है। जब क्रिया करने वाली
आत्मा है तो फिर उस क्रिया का फल अन्य कौन भोगेगा? जब इस प्रकार पूछते हैं तो आत्मा को प्रबन्ध (बन्ध रहित) मानने वाले 'रुष्ट होते हैं ॥ २ ॥
विवेचन-जैनदर्शन निश्चयनय से प्रात्मा को बन्धरहित मानता है किन्तु अन्य नयों की अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखें तो यह एकान्त वाक्य हो जाता है। यदि आत्मा को पूर्णतः बन्धरहित मान लिया जाये तो प्रश्न उठता है कि आत्मा कर्म करती है तो फल भी भोगेगी ही। आत्मा को क्रिया करती हुई तो मानते हैं, परन्तु उसे फल की भोक्ता नहीं मानते । तब क्या उस क्रिया का फल कोई अन्य भोगेगा? यह प्रश्न करने पर सांख्य एवं वेदान्ती क्रोधित हो जाते हैं ॥ २॥
अर्थ-भावार्थ-अनेक दार्शनिक जड़ और चेतन को एक रूप मानते हैं। यदि यह मानें तो जीव को सुख-दु:ख नहीं होना चाहिए। यदि सुख-दुःख मानें तो इसमें संकर दोष होता है। ऐसा विचार करके आत्मतत्त्व की परीक्षा करनी चाहिए ॥ ३ ॥
विवेचन-भिन्न-भिन्न पदार्थों के लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैं। एक-दूसरे में लक्षण घटित होने से 'संकर' नामक दोष होता है। सुख का वेदन हर्ष है और दुःख का वेदन क्लेश है। दोनों का स्वभाव भिन्न है। जब इन्हें एक ही माना जाता है तब संकर दोष होता है। इसी प्रकार से जड़ एवं चेतन को समान समझने में भी संकर दोष है।
अद्वैत मत वालों का मानना है कि ‘एको ब्रह्मः द्वितीयो नास्ति ।' इसके अनुसार जड़ चेतन में कोई भेद नहीं है । सब ब्रह्म हैं। विशिष्टाद्वैती जड़-चेतन में एक ही प्रात्मा व्याप्त मानते हैं और द्वेताद्वैत को मानने वाले जड़-चेतन में कुछ भेद मानते हैं। सारांश यह है कि जड़ और चेतन दोनों आत्मा की दृष्टि से एक हैं। इस मान्यता में 'संकर' नामक