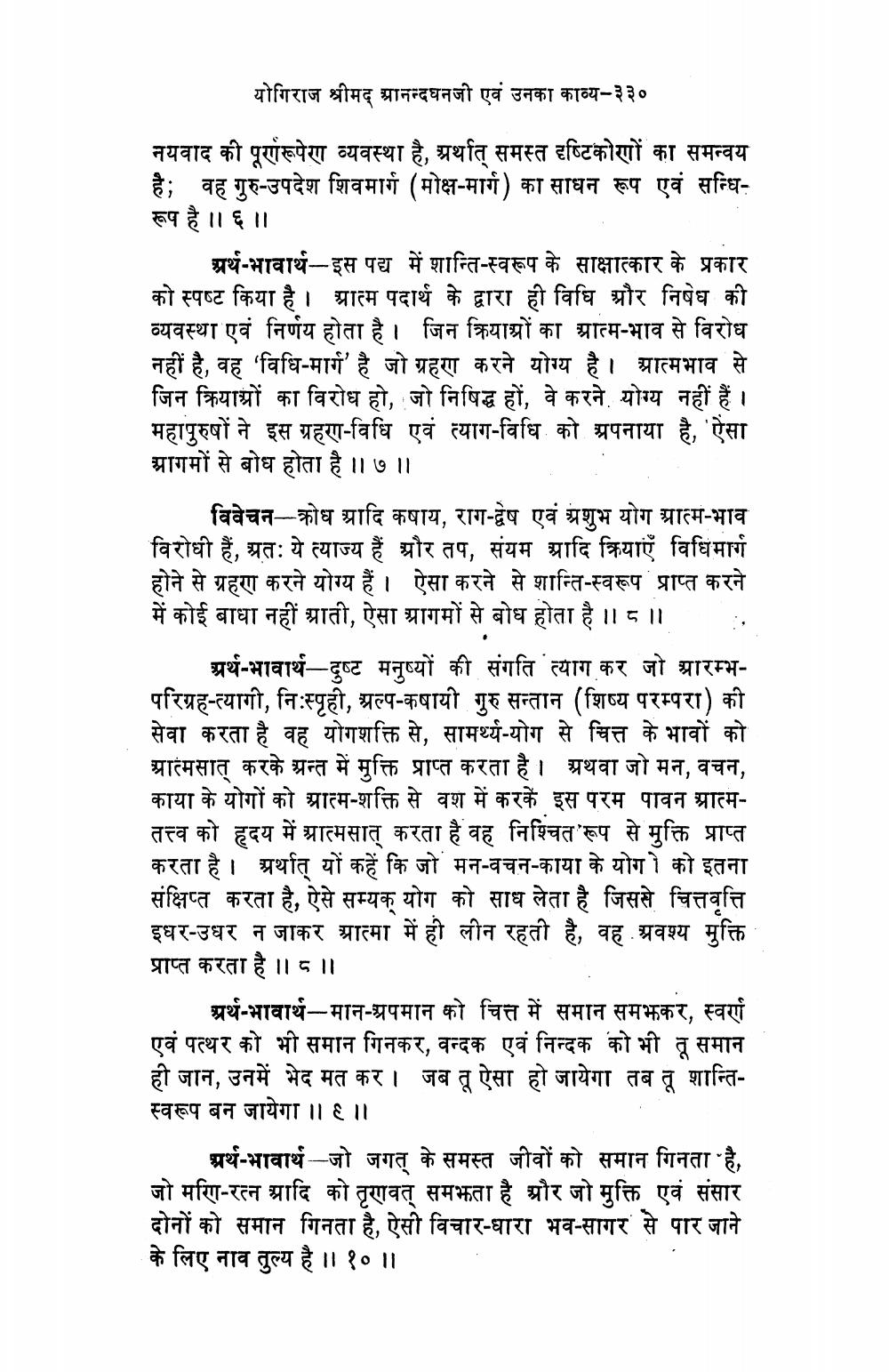________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी एवं उनका काव्य-३३०
नयवाद की पूर्णरूपेण व्यवस्था है, अर्थात् समस्त दृष्टिकोणों का समन्वय है; वह गुरु-उपदेश शिवमार्ग (मोक्ष-मार्ग) का साधन रूप एवं सन्धिरूप है ॥ ६॥
अर्थ-भावार्थ-इस पद्य में शान्ति-स्वरूप के साक्षात्कार के प्रकार को स्पष्ट किया है। प्रात्म पदार्थ के द्वारा ही विधि और निषेध की व्यवस्था एवं निर्णय होता है। जिन क्रियाओं का आत्म-भाव से विरोध नहीं है, वह 'विधि-मार्ग' है जो ग्रहण करने योग्य है। आत्मभाव से जिन क्रियानों का विरोध हो, जो निषिद्ध हों, वे करने योग्य नहीं हैं। महापुरुषों ने इस ग्रहण-विधि एवं त्याग-विधि को अपनाया है, ऐसा आगमों से बोध होता है ।। ७ ।।
विवेचन-क्रोध आदि कषाय, राग-द्वेष एवं अशुभ योग प्रात्म-भाव विरोधी हैं, अतः ये त्याज्य हैं और तप, संयम आदि क्रियाएँ विधिमार्ग होने से ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा करने से शान्ति-स्वरूप प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं पाती, ऐसा अागमों से बोध होता है ।। ८ ॥
अर्थ-भावार्थ-दुष्ट मनुष्यों की संगति त्याग कर जो प्रारम्भपरिग्रह-त्यागी, निःस्पृही, अल्प-कषायी गुरु सन्तान (शिष्य परम्परा) की सेवा करता है वह योगशक्ति से, सामर्थ्य-योग से चित्त के भावों को आत्मसात् करके अन्त में मुक्ति प्राप्त करता है। अथवा जो मन, वचन, काया के योगों को आत्म-शक्ति से वश में करके इस परम पावन आत्मतत्त्व को हृदय में आत्मसात् करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात् यों कहें कि जो मन-वचन-काया के योगो को इतना संक्षिप्त करता है, ऐसे सम्यक योग को साध लेता है जिससे चित्तवृत्ति इधर-उधर न जाकर आत्मा में ही लीन रहती है, वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है ।। ८ ॥
अर्थ-भावार्थ-मान-अपमान को चित्त में समान समझकर, स्वर्ण एवं पत्थर को भी समान गिनकर, वन्दक एवं निन्दक को भी तू समान ही जान, उनमें भेद मत कर। जब तू ऐसा हो जायेगा तब तू शान्तिस्वरूप बन जायेगा ॥६॥
अर्थ-भावार्थ-जो जगत् के समस्त जीवों को समान गिनता है, जो मरिण-रत्न आदि को तृणवत् समझता है और जो मुक्ति एवं संसार दोनों को समान गिनता है, ऐसी विचार-धारा भव-सागर से पार जाने के लिए नाव तुल्य है ।। १० ।।