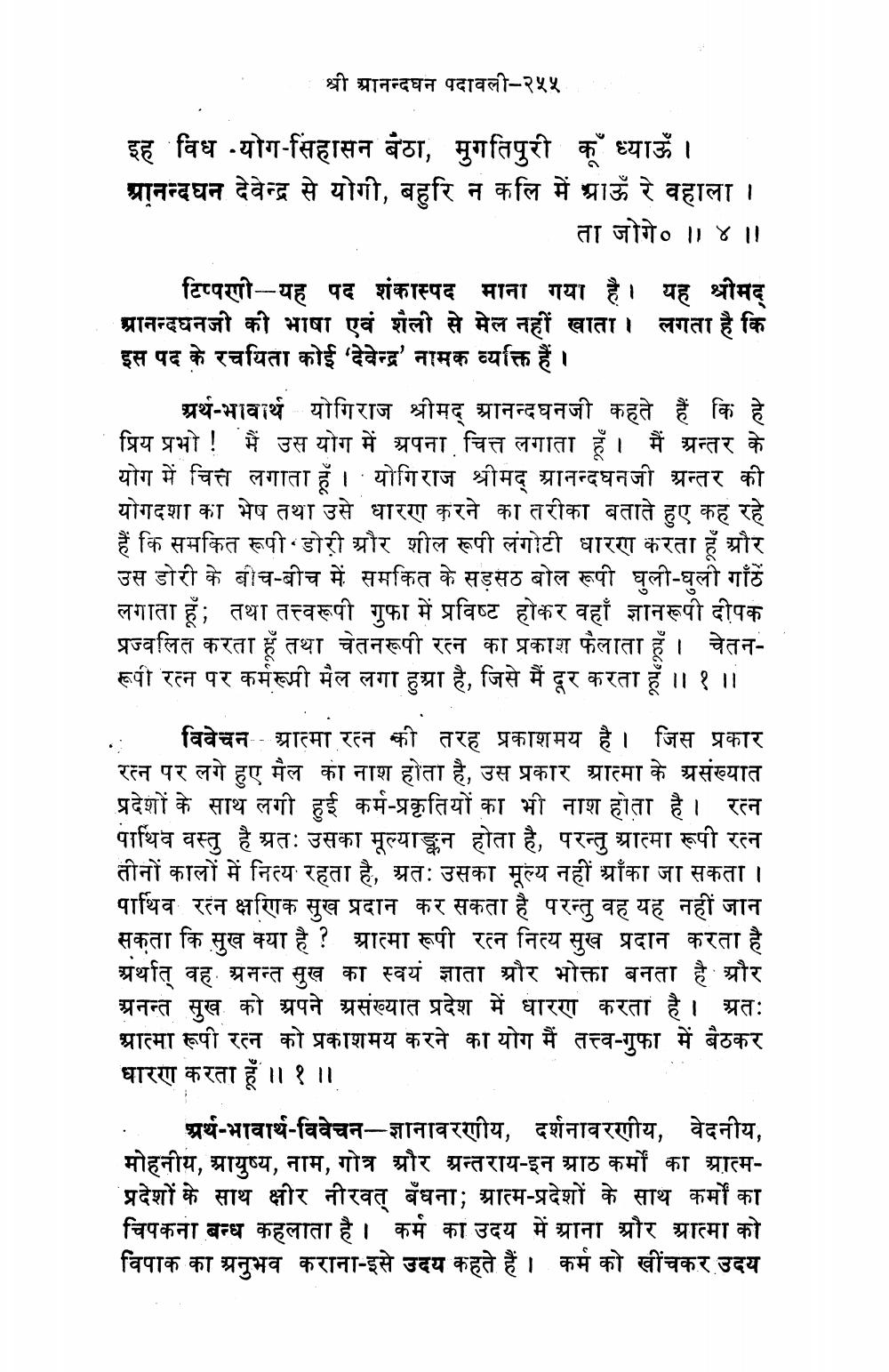________________
। श्री आनन्दघन पदावली-२५५
इह विध · योग-सिंहासन बैठा, मुगतिपुरी . ध्याऊँ । प्रानन्दघन देवेन्द्र से योगी, बहुरि न कलि में पाऊँ रे वहाला ।
ता जोगे० ।। ४ ॥
टिप्पणी-यह पद शंकास्पद माना गया है। यह श्रीमद् प्रानन्दघनजी की भाषा एवं शैली से मेल नहीं खाता। लगता है कि इस पद के रचयिता कोई 'देवेन्द्र' नामक व्यक्ति हैं।
अर्थ-भावार्थ योगिराज श्रीमद् अानन्दघनजी कहते हैं कि हे प्रिय प्रभो ! मैं उस योग में अपना चित्त लगाता हूँ। मैं अन्तर के योग में चित्त लगाता हूँ। · योगिराज श्रीमद् अानन्दघनजी अन्तर की योगदशा का भेष तथा उसे धारण करने का तरीका बताते हुए कह रहे हैं कि समकित रूपी डोरी और शील रूपी लंगोटी धारण करता हूँ और उस डोरी के बीच-बीच में समकित के सड़सठ बोल रूपी घुली-घुली गाँठें लगाता हूँ; तथा तत्त्वरूपी गुफा में प्रविष्ट होकर वहाँ ज्ञानरूपी दीपक प्रज्वलित करता हूँ तथा चेतनरूपी रत्न का प्रकाश फैलाता हूँ। चेतनरूपी रत्न पर कर्मरूपी मैल लगा हुआ है, जिसे मैं दूर करता हूँ। १ ।।
.: विवेचन - प्रात्मा रत्न की तरह प्रकाशमय है। जिस प्रकार रत्न पर लगे हुए मैल का नाश होता है, उस प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के साथ लगी हुई कर्म-प्रकृतियों का भी नाश होता है। रत्न पार्थिव वस्तु है अतः उसका मूल्याङ्कन होता है, परन्तु आत्मा रूपी रत्न तीनों कालों में नित्य रहता है, अत: उसका मूल्य नहीं प्राँका जा सकता। पार्थिव रत्न क्षणिक सुख प्रदान कर सकता है परन्तु वह यह नहीं जान सकता कि सुख क्या है ? आत्मा रूपी रत्न नित्य सुख प्रदान करता है अर्थात् वह अनन्त सुख का स्वयं ज्ञाता और भोक्ता बनता है और अनन्त सुख को अपने असंख्यात प्रदेश में धारण करता है। अतः आत्मा रूपी रत्न को प्रकाशमय करने का योग मैं तत्त्व-गुफा में बैठकर धारण करता हूँ॥१॥
अर्थ-भावार्थ-विवेचन-ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय-इन आठ कर्मों का आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर नीरवत् बँधना; आत्म-प्रदेशों के साथ कर्मों का चिपकना बन्ध कहलाता है। कर्म का उदय में आना और आत्मा को विपाक का अनुभव कराना-इसे उदय कहते हैं। कर्म को खींचकर उदय