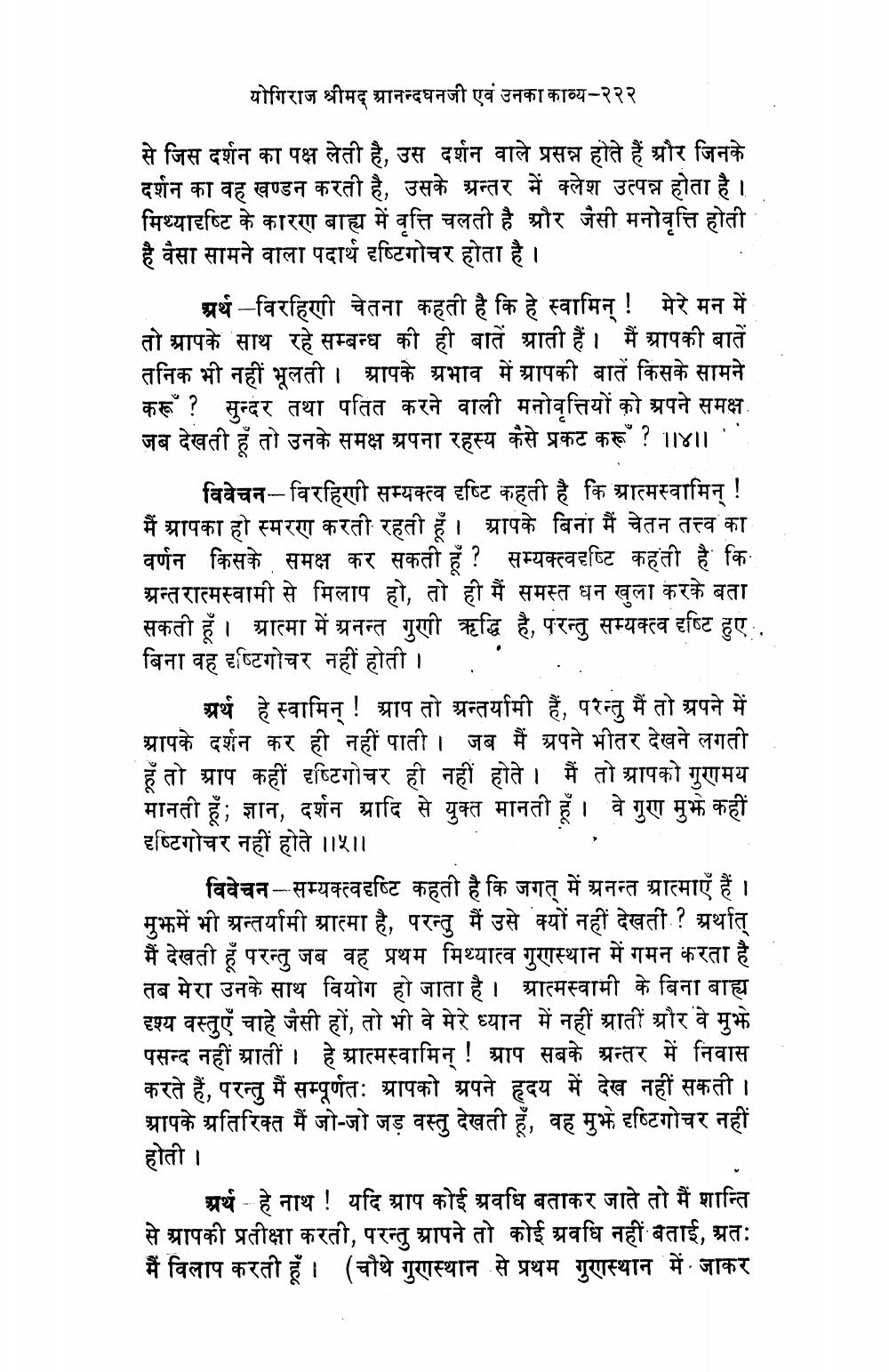________________
योगिराज श्रीमद् अानन्दघनजी एवं उनका काव्य-२२२
से जिस दर्शन का पक्ष लेती है, उस दर्शन वाले प्रसन्न होते हैं और जिनके दर्शन का वह खण्डन करती है, उसके अन्तर में क्लेश उत्पन्न होता है। मिथ्यादृष्टि के कारण बाह्य में वत्ति चलती है और जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा सामने वाला पदार्थ दृष्टिगोचर होता है।
अर्थ-विरहिणी चेतना कहती है कि हे स्वामिन् ! मेरे मन में तो आपके साथ रहे सम्बन्ध की ही बातें आती हैं। मैं आपकी बातें तनिक भी नहीं भूलती। आपके अभाव में आपकी बातें किसके सामने करूँ ? सुन्दर तथा पतित करने वाली मनोवृत्तियों को अपने समक्ष जब देखती हूँ तो उनके समक्ष अपना रहस्य कैसे प्रकट करू ? ।।४।।
विवेचन-विरहिणी सम्यक्त्व दृष्टि कहती है कि आत्मस्वामिन् ! मैं आपका हो स्मरण करती रहती हूँ। आपके बिना मैं चेतन तत्त्व का वर्णन किसके समक्ष कर सकती हूँ ? सम्यक्त्वदृष्टि कहती है कि अन्तरात्मस्वामी से मिलाप हो, तो ही मैं समस्त धन खुला करके बता सकती हूँ। आत्मा में अनन्त गुणी ऋद्धि है, परन्तु सम्यक्त्व दृष्टि हुए . बिना वह दृष्टिगोचर नहीं होती।
अर्थ हे स्वामिन ! आप तो अन्तर्यामी हैं, परन्तु मैं तो अपने में आपके दर्शन कर ही नहीं पाती। जब मैं अपने भीतर देखने लगती हँ तो आप कहीं दृष्टिगोचर ही नहीं होते। मैं तो आपको गुणमय मानती हूँ; ज्ञान, दर्शन आदि से युक्त मानती हूँ। वे गुण मुझे कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते ॥५॥
विवेचन-सम्यक्त्वदृष्टि कहती है कि जगत् में अनन्त आत्माएँ हैं। मुझमें भी अन्तर्यामी आत्मा है, परन्तु मैं उसे क्यों नहीं देखती ? अर्थात् मैं देखती हूँ परन्तु जब वह प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में गमन करता है तब मेरा उनके साथ वियोग हो जाता है। प्रात्मस्वामी के बिना बाह्य दृश्य वस्तुएँ चाहे जैसी हों, तो भी वे मेरे ध्यान में नहीं आतीं और वे मुझे पसन्द नहीं आतीं। हे आत्मस्वामिन् ! आप सबके अन्तर में निवास करते हैं, परन्तु मैं सम्पूर्णतः आपको अपने हृदय में देख नहीं सकती। आपके अतिरिक्त मैं जो-जो जड़ वस्तु देखती हूँ, वह मुझे दृष्टिगोचर नहीं होती।
अर्थ- हे नाथ ! यदि आप कोई अवधि बताकर जाते तो मैं शान्ति से आपकी प्रतीक्षा करती, परन्तु आपने तो कोई अवधि नहीं बताई, अतः मैं विलाप करती हूँ। (चौथे गुणस्थान से प्रथम गुणस्थान में जाकर