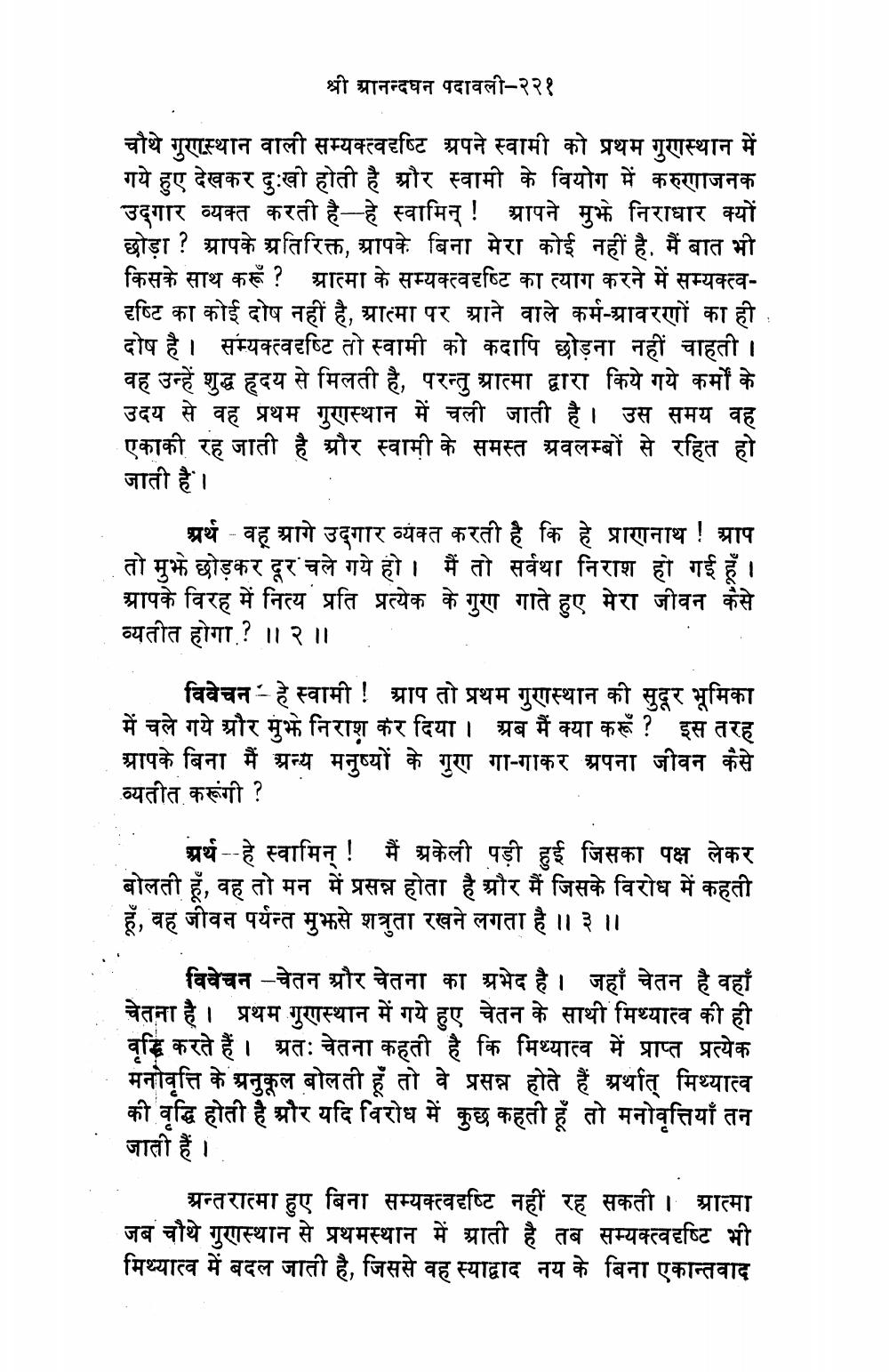________________
श्री आनन्दघन पदावली-२२१
चौथे गुणस्थान वाली सम्यक्त्वदृष्टि अपने स्वामी को प्रथम गुणस्थान में गये हुए देखकर दुःखी होती है और स्वामी के वियोग में करुणाजनक उद्गार व्यक्त करती है-हे स्वामिन् ! आपने मुझे निराधार क्यों छोड़ा? आपके अतिरिक्त, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, मैं बात भी किसके साथ करूँ ? आत्मा के सम्यक्त्वदृष्टि का त्याग करने में सम्यक्त्वदृष्टि का कोई दोष नहीं है, आत्मा पर आने वाले कर्म-आवरणों का ही दोष है। सम्यक्त्वदृष्टि तो स्वामी को कदापि छोड़ना नहीं चाहती। वह उन्हें शुद्ध हृदय से मिलती है, परन्तु आत्मा द्वारा किये गये कर्मों के उदय से वह प्रथम गुणस्थान में चली जाती है। उस समय वह एकाकी रह जाती है और स्वामी के समस्त अवलम्बों से रहित हो जाती है।
अर्थ - वह आगे उद्गार व्यक्त करती है कि हे प्राणनाथ ! आप तो मुझे छोड़कर दूर चले गये हो। मैं तो सर्वथा निराश हो गई हूँ। आपके विरह में नित्य प्रति प्रत्येक के गुण गाते हुए मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? ॥२॥
विवेचन - हे स्वामी ! आप तो प्रथम गुणस्थान की सुदूर भूमिका में चले गये और मुझे निराश कर दिया। अब मैं क्या करूँ? इस तरह आपके बिना मैं अन्य मनुष्यों के गुण गा-गाकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? - अर्थ --हे स्वामिन् ! मैं अकेली पड़ी हुई जिसका पक्ष लेकर बोलती हैं, वह तो मन में प्रसन्न होता है और मैं जिसके विरोध में कहती हूँ, वह जीवन पर्यन्त मुझसे शत्रुता रखने लगता है ।। ३ ।।
विवेचन -चेतन और चेतना का अभेद है। जहाँ चेतन है वहाँ चेतना है। प्रथम गुणस्थान में गये हुए चेतन के साथी मिथ्यात्व की ही वृद्धि करते हैं। अतः चेतना कहती है कि मिथ्यात्व में प्राप्त प्रत्येक मनोवृत्ति के अनुकूल बोलती हैं तो वे प्रसन्न होते हैं अर्थात मिथ्यात्व की वृद्धि होती है और यदि विरोध में कुछ कहती हूँ तो मनोवृत्तियाँ तन जाती हैं।
अन्तरात्मा हुए बिना सम्यक्त्वदृष्टि नहीं रह सकती। आत्मा जब चौथे गुणस्थान से प्रथमस्थान में आती है तब सम्यक्त्वदृष्टि भी मिथ्यात्व में बदल जाती है, जिससे वह स्याद्वाद नय के बिना एकान्तवाद