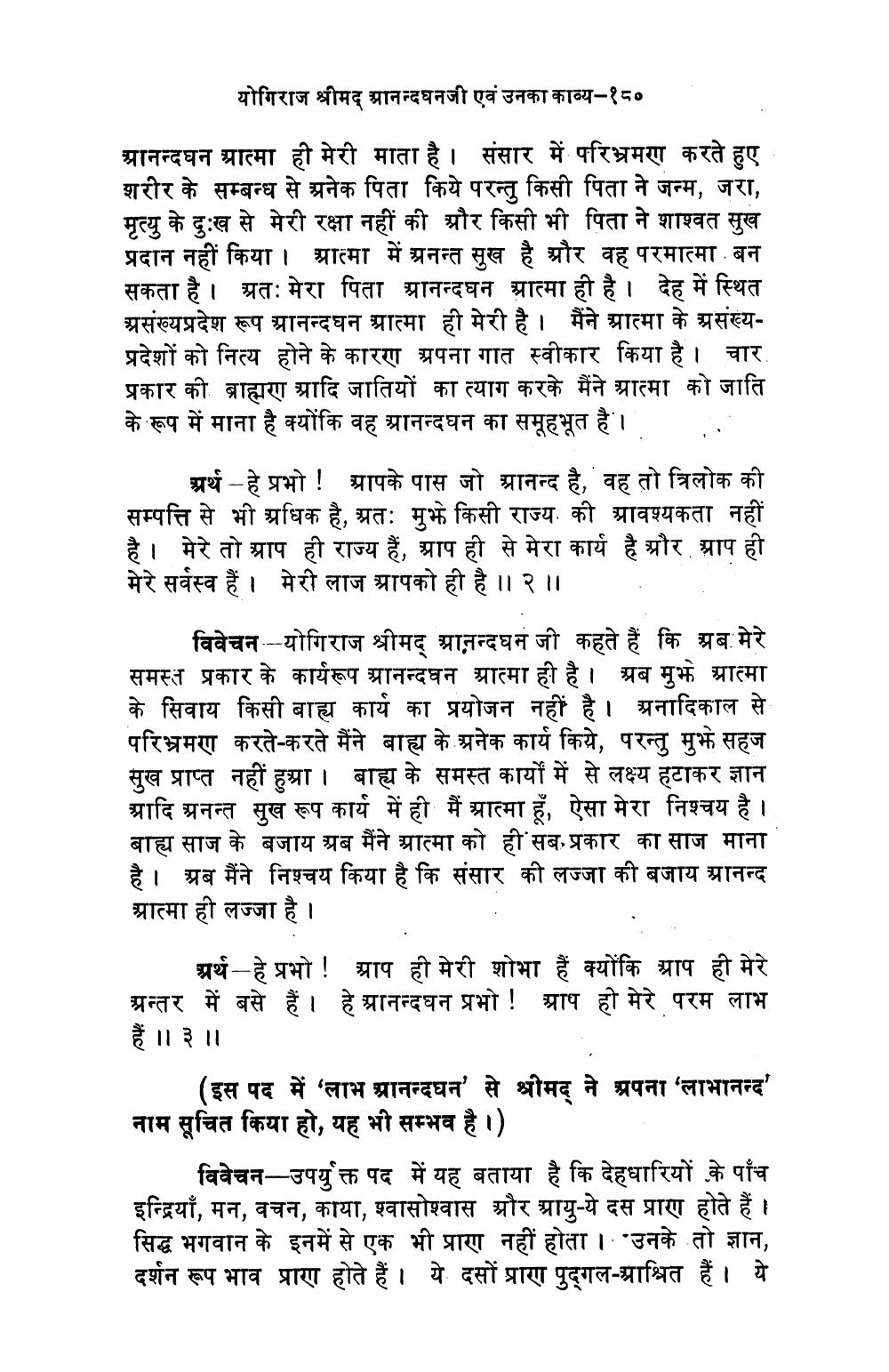________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी एवं उनका काव्य-१८०
आनन्दघन आत्मा ही मेरी माता है। संसार में परिभ्रमण करते हुए शरीर के सम्बन्ध से अनेक पिता किये परन्तु किसी पिता ने जन्म, जरा, मृत्यु के दुःख से मेरी रक्षा नहीं की और किसी भी पिता ने शाश्वत सुख प्रदान नहीं किया। आत्मा में अनन्त सुख है और वह परमात्मा बन सकता है। अतः मेरा पिता आनन्दघन आत्मा ही है। देह में स्थित असंख्यप्रदेश रूप आनन्दघन आत्मा ही मेरी है। मैंने आत्मा के असंख्यप्रदेशों को नित्य होने के कारण अपना गात स्वीकार किया है। चार प्रकार की ब्राह्मण आदि जातियों का त्याग करके मैंने आत्मा को जाति के रूप में माना है क्योंकि वह आनन्दघन का समूहभूत है।
अर्थ -हे प्रभो ! आपके पास जो आनन्द है, वह तो त्रिलोक की सम्पत्ति से भी अधिक है, अत: मुझे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। मेरे तो आप ही राज्य हैं, आप ही से मेरा कार्य है और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरी लाज आपको ही है ।। २ ।।
विवेचन-योगिराज श्रीमद् आनन्दघन जी कहते हैं कि अब मेरे समस्त प्रकार के कार्यरूप आनन्दघन आत्मा ही है। अब मुझे आत्मा के सिवाय किसी बाह्य कार्य का प्रयोजन नहीं है। अनादिकाल से परिभ्रमण करते-करते मैंने बाह्य के अनेक कार्य किये, परन्तु मुझे सहज सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाह्य के समस्त कार्यों में से लक्ष्य हटाकर ज्ञान आदि अनन्त सुख रूप कार्य में ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है। बाह्य साज के बजाय अब मैंने आत्मा को ही सब प्रकार का साज माना है। अब मैंने निश्चय किया है कि संसार की लज्जा की बजाय आनन्द आत्मा ही लज्जा है।
अर्थ-हे प्रभो! आप ही मेरी शोभा हैं क्योंकि आप ही मेरे अन्तर में बसे हैं। हे आनन्दघन प्रभो! आप हो मेरे परम लाभ
(इस पद में 'लाभ प्रानन्दघन' से श्रीमद् ने अपना 'लाभानन्द' नाम सूचित किया हो, यह भी सम्भव है।)
विवेचन-उपर्युक्त पद में यह बताया है कि देहधारियों के पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास और आयु-ये दस प्राण होते हैं। सिद्ध भगवान के इनमें से एक भी प्राण नहीं होता। 'उनके तो ज्ञान, दर्शन रूप भाव प्राण होते हैं। ये दसों प्राण पुद्गल-आश्रित हैं। ये