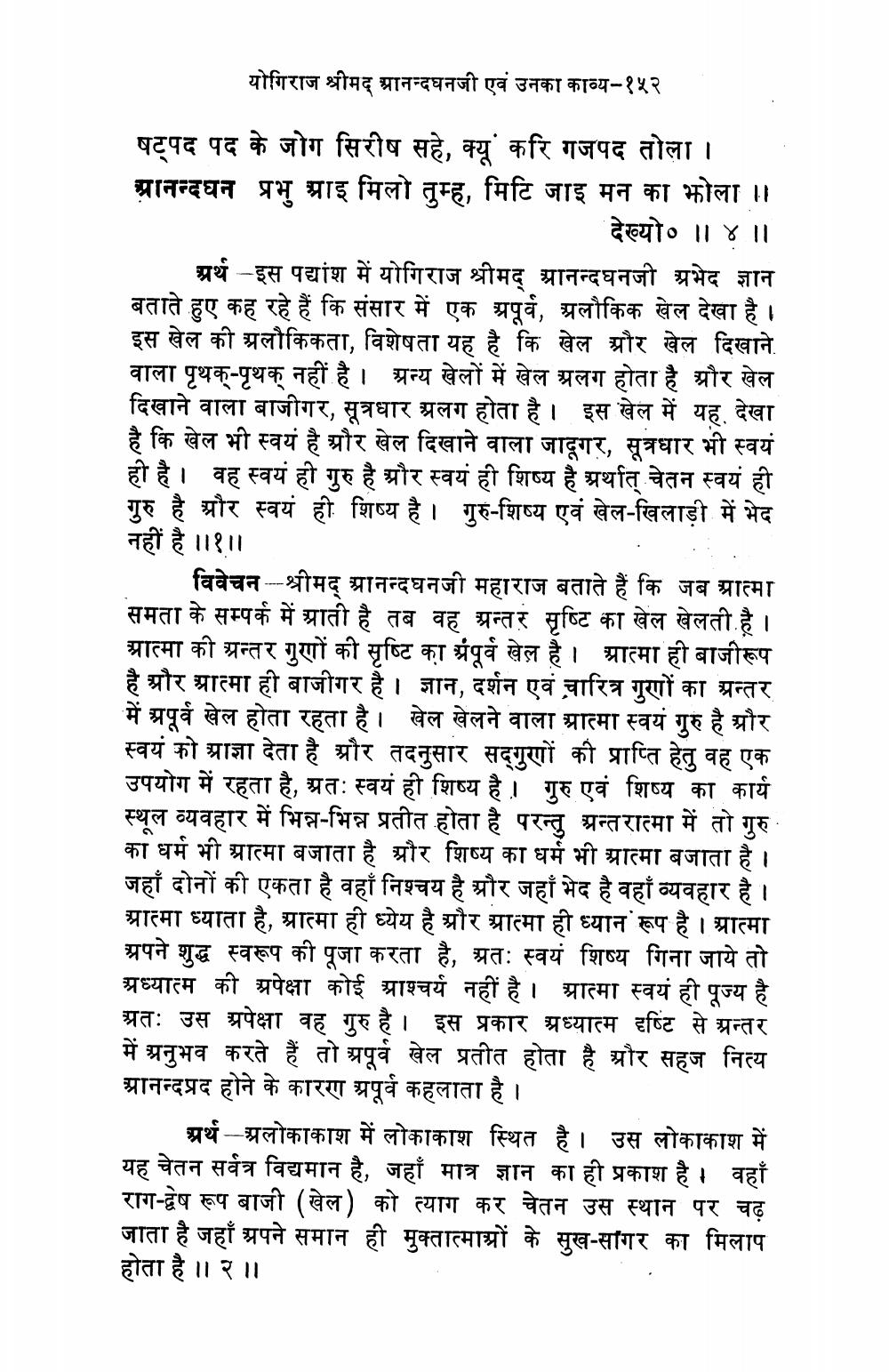________________
योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी एवं उनका काव्य-१५२
षट्पद पद के जोग सिरीष सहे, क्यू करि गजपद तोला। आनन्दघन प्रभु आइ मिलो तुम्ह, मिटि जाइ मन का झोला ।।
देख्यो० ॥ ४ ॥ अर्थ – इस पद्यांश में योगिराज श्रीमद् आनन्दघनजी अभेद ज्ञान बताते हुए कह रहे हैं कि संसार में एक अपूर्व, अलौकिक खेल देखा है। इस खेल की अलौकिकता, विशेषता यह है कि खेल और खेल दिखाने वाला पृथक्-पृथक् नहीं है। अन्य खेलों में खेल अलग होता है और खेल दिखाने वाला बाजीगर, सूत्रधार अलग होता है। इस खेल में यह. देखा है कि खेल भी स्वयं है और खेल दिखाने वाला जादूगर, सूत्रधार भी स्वयं ही है। वह स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही शिष्य है अर्थात् चेतन स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही शिष्य है। गुरु-शिष्य एवं खेल-खिलाड़ी में भेद नहीं है ॥१॥
विवेचन-श्रीमद् आनन्दघनजी महाराज बताते हैं कि जब आत्मा समता के सम्पर्क में आती है तब वह अन्तर सृष्टि का खेल खेलती है। आत्मा की अन्तर गुरणों की सृष्टि का अंपूर्व खेल है। आत्मा ही बाजीरूप है और आत्मा ही बाजीगर है। ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र गुणों का अन्तर में अपूर्व खेल होता रहता है। खेल खेलने वाला आत्मा स्वयं गुरु है और स्वयं को आज्ञा देता है और तदनुसार सदगुणों की प्राप्ति हेतु वह एक उपयोग में रहता है, अतः स्वयं ही शिष्य है। गुरु एवं शिष्य का कार्य स्थूल व्यवहार में भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है परन्तु अन्तरात्मा में तो गुरु का धर्म भी आत्मा बजाता है और शिष्य का धर्म भी आत्मा बजाता है। जहाँ दोनों की एकता है वहाँ निश्चय है और जहाँ भेद है वहाँ व्यवहार है। आत्मा ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही ध्यान रूप है । आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की पूजा करता है, अतः स्वयं शिष्य गिना जाये तो अध्यात्म की अपेक्षा कोई आश्चर्य नहीं है। आत्मा स्वयं ही पूज्य है अतः उस अपेक्षा वह गुरु है। इस प्रकार अध्यात्म दृष्टि से अन्तर में अनुभव करते हैं तो अपूर्व खेल प्रतीत होता है और सहज नित्य आनन्दप्रद होने के कारण अपूर्व कहलाता है।
अर्थ-अलोकाकाश में लोकाकाश स्थित है। उस लोकाकाश में यह चेतन सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ मात्र ज्ञान का ही प्रकाश है। वहाँ राग-द्वेष रूप बाजी (खेल) को त्याग कर चेतन उस स्थान पर चढ़ जाता है जहाँ अपने समान ही मुक्तात्माओं के सुख-सांगर का मिलाप होता है ॥ २ ॥