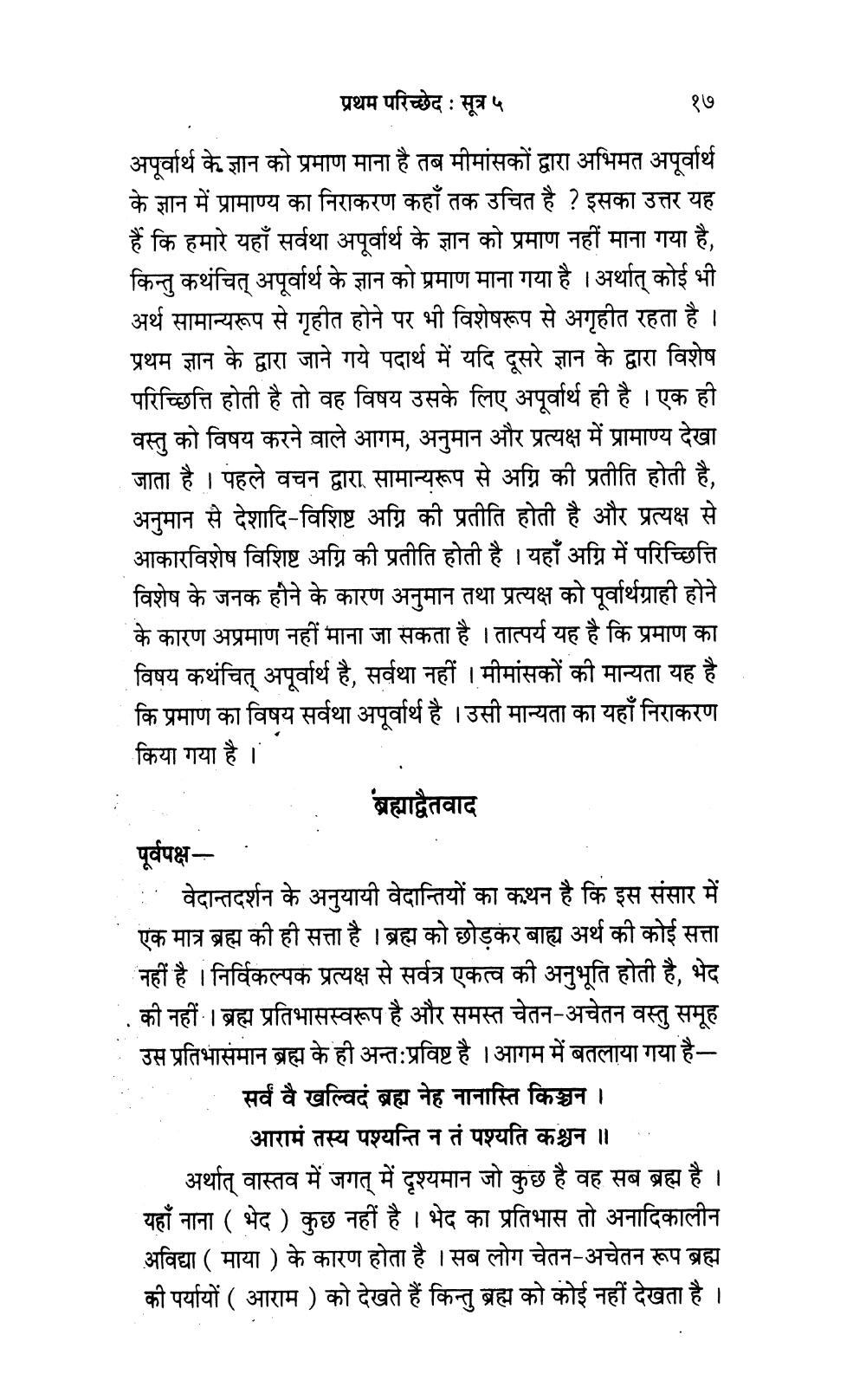________________
प्रथम परिच्छेद : सूत्र ५
१७
अपूर्वार्थ के ज्ञान को प्रमाण माना है तब मीमांसकों द्वारा अभिमत अपूर्वार्थ के ज्ञान में प्रामाण्य का निराकरण कहाँ तक उचित है ? इसका उत्तर यह हैं कि हमारे यहाँ सर्वथा अपूर्वार्थ के ज्ञान को प्रमाण नहीं माना गया है, किन्तु कथंचित् अपूर्वार्थ के ज्ञान को प्रमाण माना गया है । अर्थात् कोई भी अर्थ सामान्यरूप से गृहीत होने पर भी विशेषरूप से अगृहीत रहता है । प्रथम ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थ में यदि दूसरे ज्ञान के द्वारा विशेष परिच्छित्ति होती है तो वह विषय उसके लिए अपूर्वार्थ ही है । एक ही वस्तु को विषय करने वाले आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष में प्रामाण्य देखा जाता है । पहले वचन द्वारा सामान्यरूप से अग्नि की प्रतीति होती है, अनुमान से देशादि-विशिष्ट अग्नि की प्रतीति होती है और प्रत्यक्ष से आकारविशेष विशिष्ट अग्नि की प्रतीति होती है । यहाँ अग्नि में परिच्छित्ति विशेष के जनक होने के कारण अनुमान तथा प्रत्यक्ष को पूर्वार्थग्राही होने के कारण अप्रमाण नहीं माना जा सकता है । तात्पर्य यह है कि प्रमाण का विषय कथंचित् अपूर्वार्थ है, सर्वथा नहीं । मीमांसकों की मान्यता यह है कि प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ है । उसी मान्यता का यहाँ निराकरण किया गया है।
ब्रह्माद्वैतवाद पूर्वपक्ष
- वेदान्तदर्शन के अनुयायी वेदान्तियों का कथन है कि इस संसार में एक मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है । ब्रह्म को छोड़कर बाह्य अर्थ की कोई सत्ता नहीं है । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से सर्वत्र एकत्व की अनुभूति होती है, भेद . की नहीं । ब्रह्म प्रतिभासस्वरूप है और समस्त चेतन-अचेतन वस्तु समूह - उस प्रतिभासमान ब्रह्म के ही अन्तःप्रविष्ट है ।आगम में बतलाया गया है
सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।
आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥ .. अर्थात् वास्तव में जगत् में दृश्यमान जो कुछ है वह सब ब्रह्म है । यहाँ नाना ( भेद ) कुछ नहीं है । भेद का प्रतिभास तो अनादिकालीन अविद्या ( माया ) के कारण होता है । सब लोग चेतन-अचेतन रूप ब्रह्म की पर्यायों ( आराम ) को देखते हैं किन्तु ब्रह्म को कोई नहीं देखता है ।