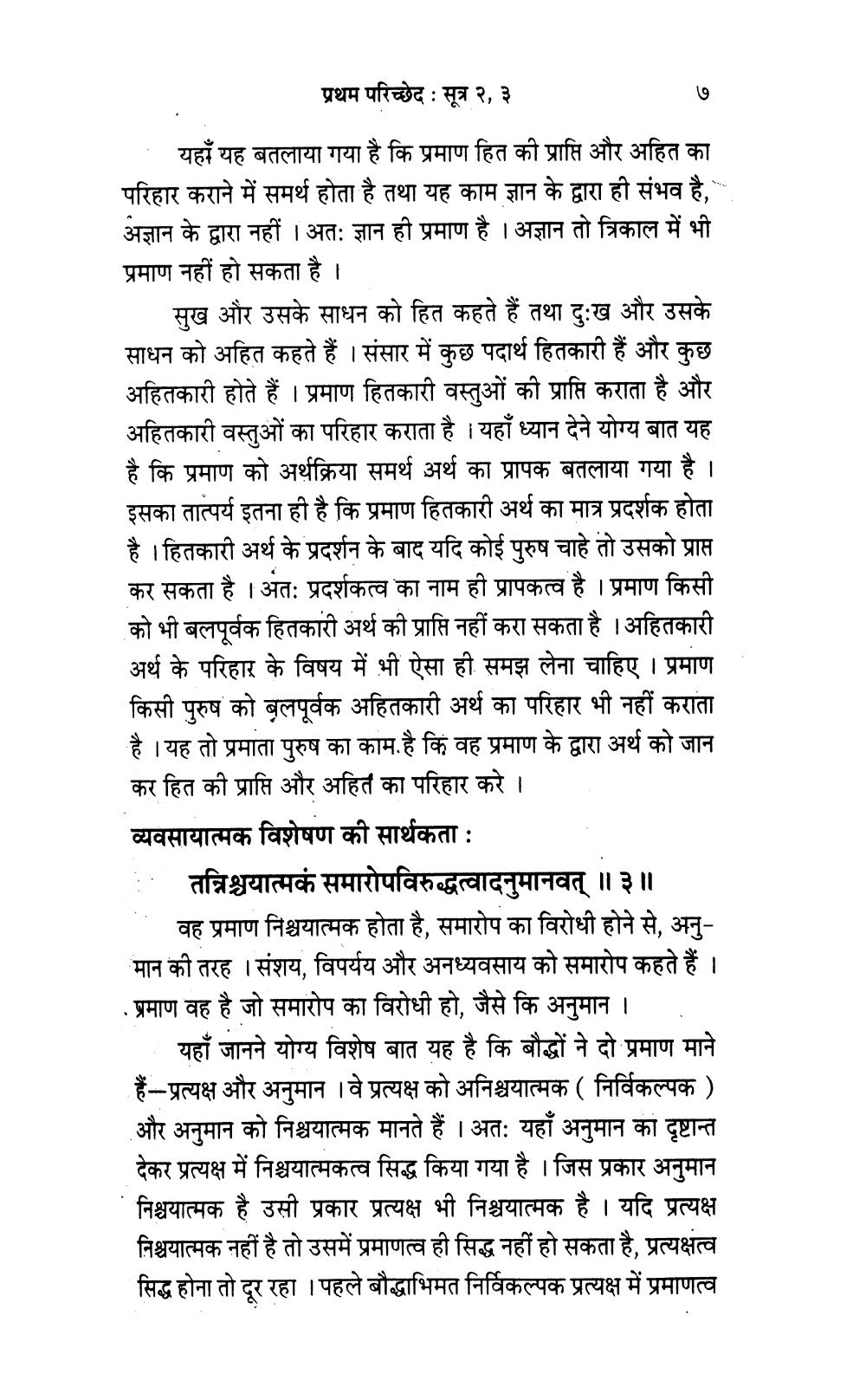________________
प्रथम परिच्छेद: सूत्र २, ३
यहाँ यह बतलाया गया है कि प्रमाण हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराने में समर्थ होता है तथा यह काम ज्ञान के द्वारा ही संभव है, अज्ञान के द्वारा नहीं । अतः ज्ञान ही प्रमाण है । अज्ञान तो त्रिकाल में भी प्रमाण नहीं हो सकता है ।
७
सुख और उसके साधन को हित कहते हैं तथा दुःख और उसके साधन को अहित कहते हैं । संसार में कुछ पदार्थ हितकारी हैं और कुछ अहितकारी होते हैं । प्रमाण हितकारी वस्तुओं की प्राप्ति कराता है और अहितकारी वस्तुओं का परिहार कराता है । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रमाण को अर्थक्रिया समर्थ अर्थ का प्रापक बतलाया गया है । इसका तात्पर्य इतना ही है कि प्रमाण हितकारी अर्थ का मात्र प्रदर्शक होता है । हितकारी अर्थ के प्रदर्शन के बाद यदि कोई पुरुष चाहे तो उसको प्राप्त कर सकता है । अतः प्रदर्शकत्व का नाम ही प्रापकत्व है । प्रमाण किसी को भी बलपूर्वक हितकारी अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकता है । अहितकारी अर्थ के परिहार के विषय में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए । प्रमाण किसी पुरुष को बलपूर्वक अहितकारी अर्थ का परिहार भी नहीं कराता है । यह तो प्रमाता पुरुष का काम है कि वह प्रमाण के द्वारा अर्थ को जान करहित की प्राप्ति और अहित का परिहार करे ।
1
व्यवसायात्मक विशेषण की सार्थकता :
तनिश्रयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत् ॥ ३ ॥
वह प्रमाण निश्चयात्मक होता है, समारोप का विरोधी होने से, अनुमान की तरह । संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय को समारोप कहते हैं । प्रमाण वह है जो समारोप का विरोधी हो, जैसे कि अनुमान ।
यहाँ जानने योग्य विशेष बात यह है कि बौद्धों ने दो प्रमाण माने - प्रत्यक्ष और अनुमान । वे प्रत्यक्ष को अनिश्चयात्मक ( निर्विकल्पक ) और अनुमान को निश्चयात्मक मानते हैं । अतः यहाँ अनुमान का दृष्टान्त देकर प्रत्यक्ष में निश्चयात्मकत्व सिद्ध किया गया है । जिस प्रकार अनुमान निश्चयात्मक है उसी प्रकार प्रत्यक्ष भी निश्चयात्मक है । यदि प्रत्यक्ष निश्चयात्मक नहीं है तो उसमें प्रमाणत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षत्व सिद्ध होना तो दूर रहा । पहले बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में प्रमाणत्व
I