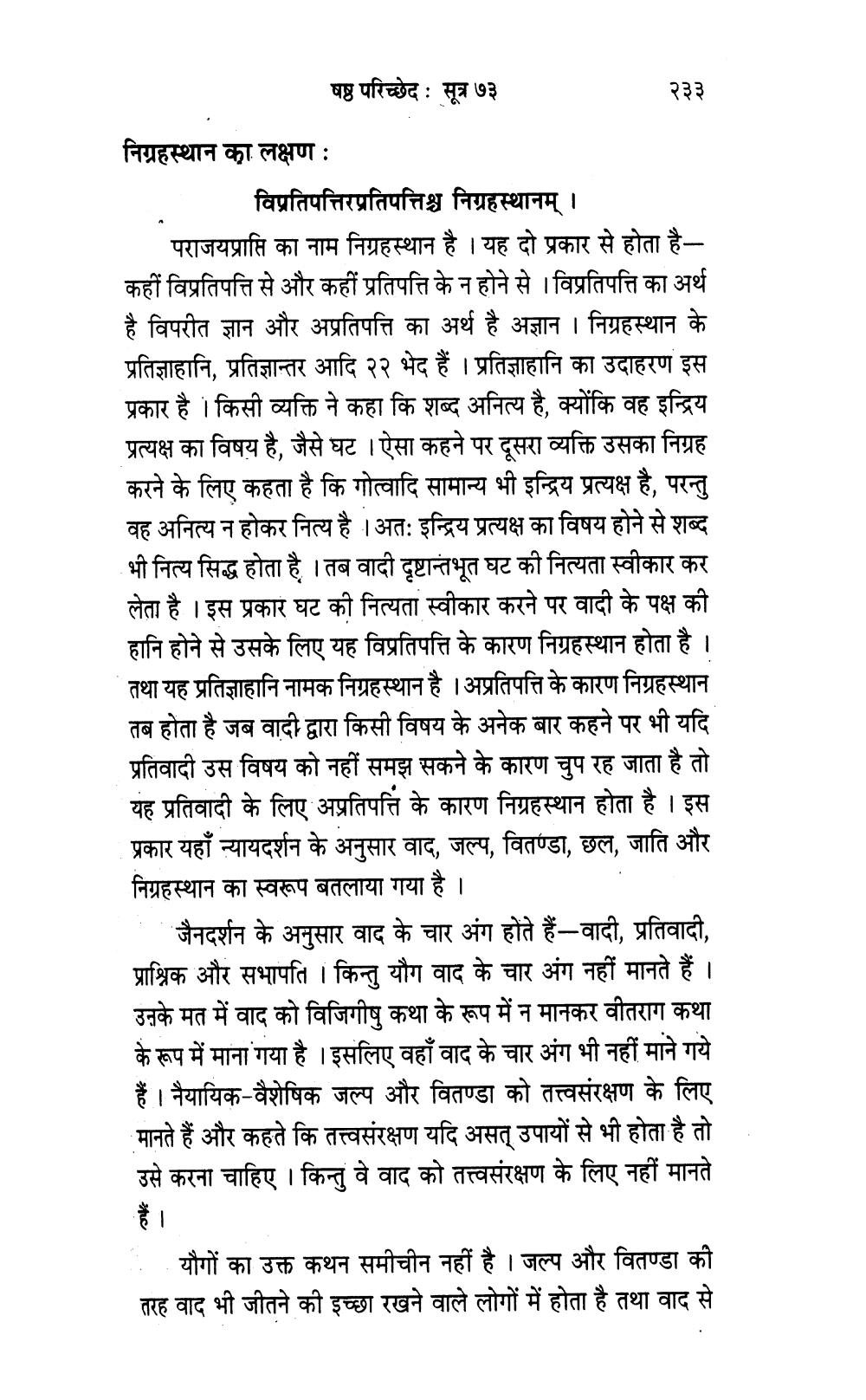________________
षष्ठ परिच्छेद : सूत्र ७३
निग्रहस्थान का लक्षण :
२३३
विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ।
पराजयप्राप्ति का नाम निग्रहस्थान है । यह दो प्रकार से होता हैकहीं विप्रतिपत्ति से और कहीं प्रतिपत्ति के न होने से । विप्रतिपत्ति का अर्थ है विपरीत ज्ञान और अप्रतिपत्ति का अर्थ है अज्ञान । निग्रहस्थान के प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदि २२ भेद हैं । प्रतिज्ञाहानि का उदाहरण इस प्रकार है । किसी व्यक्ति ने कहा कि शब्द अनित्य है, क्योंकि वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय है, जैसे घट । ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति उसका निग्रह करने के लिए कहता है कि गोत्वादि सामान्य भी इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, परन्तु वह अनित्य न होकर नित्य है । अतः इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय होने से शब्द भी नित्य सिद्ध होता है । तब वादी दृष्टान्तभूत घट की नित्यता स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार घट की नित्यता स्वीकार करने पर वादी के पक्ष की हानि होने से उसके लिए यह विप्रतिपत्ति के कारण निग्रहस्थान होता है । तथा यह प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान है । अप्रतिपत्ति के कारण निग्रहस्थान तब होता है जब वादी द्वारा किसी विषय के अनेक बार कहने पर भी यदि प्रतिवादी उस विषय को नहीं समझ सकने के कारण चुप रह जाता है तो यह प्रतिवादी के लिए अप्रतिपत्ति के कारण निग्रहस्थान होता है । इस प्रकार यहाँ न्यायदर्शन के अनुसार वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति और निग्रहस्थान का स्वरूप बतलाया गया है ।
जैनदर्शन के अनुसार वाद के चार अंग होते हैं - वादी, प्रतिवादी, प्राश्निक और सभापति । किन्तु यौग वाद के चार अंग नहीं मानते हैं । उनके मत में वाद को विजिगीषु कथा के रूप में न मानकर वीतराग कथा के रूप में माना गया है । इसलिए वहाँ वाद के चार अंग भी नहीं माने गये हैं। नैयायिक - वैशेषिक जल्प और वितण्डा को तत्त्वसंरक्षण के लिए मानते हैं और कहते कि तत्त्वसंरक्षण यदि असत् उपायों से भी होता है तो उसे करना चाहिए । किन्तु वे वाद को तत्त्वसंरक्षण के लिए नहीं मानते हैं ।
यौगों का उक्त कथन समीचीन नहीं है। जल्प और वितण्डा की तरह वाद भी जीतने की इच्छा रखने वाले लोगों में होता है तथा वाद से