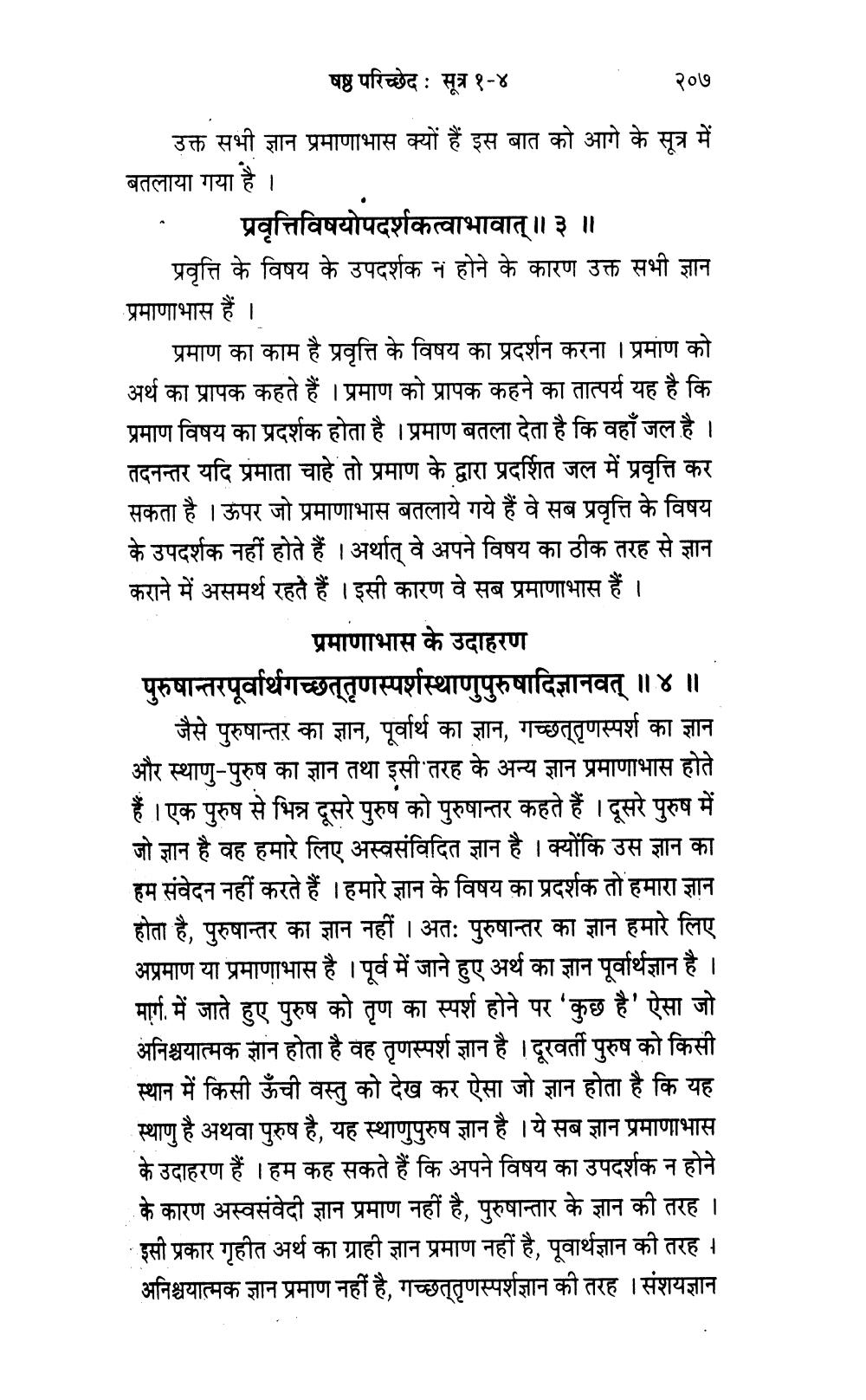________________
षष्ठ परिच्छेद : सूत्र १-४
२०७
उक्त सभी ज्ञान प्रमाणाभास क्यों हैं इस बात को आगे के सूत्र में बतलाया गया है। - प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वाभावात्॥३॥
प्रवृत्ति के विषय के उपदर्शक न होने के कारण उक्त सभी ज्ञान प्रमाणाभास हैं ।
प्रमाण का काम है प्रवृत्ति के विषय का प्रदर्शन करना । प्रमाण को अर्थ का प्रापक कहते हैं । प्रमाण को प्रापक कहने का तात्पर्य यह है कि प्रमाण विषय का प्रदर्शक होता है । प्रमाण बतला देता है कि वहाँ जल है । तदनन्तर यदि प्रमाता चाहे तो प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित जल में प्रवृत्ति कर सकता है । ऊपर जो प्रमाणाभास बतलाये गये हैं वे सब प्रवृत्ति के विषय के उपदर्शक नहीं होते हैं । अर्थात् वे अपने विषय का ठीक तरह से ज्ञान कराने में असमर्थ रहते हैं । इसी कारण वे सब प्रमाणाभास हैं ।
प्रमाणाभास के उदाहरण पुरुषान्तरपूर्वार्थगच्छत्तृणस्पर्शस्थाणुपुरुषादिज्ञानवत् ॥४॥ ___ जैसे पुरुषान्तर का ज्ञान, पूर्वार्थ का ज्ञान, गच्छत्तृणस्पर्श का ज्ञान और स्थाणु-पुरुष का ज्ञान तथा इसी तरह के अन्य ज्ञान प्रमाणाभास होते हैं । एक पुरुष से भिन्न दूसरे पुरुष को पुरुषान्तर कहते हैं । दूसरे पुरुष में जो ज्ञान है वह हमारे लिए अस्वसंविदित ज्ञान है । क्योंकि उस ज्ञान का हम संवेदन नहीं करते हैं । हमारे ज्ञान के विषय का प्रदर्शक तो हमारा ज्ञान होता है, पुरुषान्तर का ज्ञान नहीं । अतः पुरुषान्तर का ज्ञान हमारे लिए अप्रमाण या प्रमाणाभास है । पूर्व में जाने हुए अर्थ का ज्ञान पूर्वार्थज्ञान है । मार्ग. में जाते हुए पुरुष को तृण का स्पर्श होने पर 'कुछ है' ऐसा जो अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है वह तृणस्पर्श ज्ञान है । दूरवर्ती पुरुष को किसी स्थान में किसी ऊँची वस्तु को देख कर ऐसा जो ज्ञान होता है कि यह स्थाणु है अथवा पुरुष है, यह स्थाणुपुरुष ज्ञान है । ये सब ज्ञान प्रमाणाभास के उदाहरण हैं । हम कह सकते हैं कि अपने विषय का उपदर्शक न होने के कारण अस्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण नहीं है, पुरुषान्तार के ज्ञान की तरह । इसी प्रकार गृहीत अर्थ का ग्राही ज्ञान प्रमाण नहीं है, पूवार्थज्ञान की तरह । अनिश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण नहीं है, गच्छत्तृणस्पर्शज्ञान की तरह । संशयज्ञान