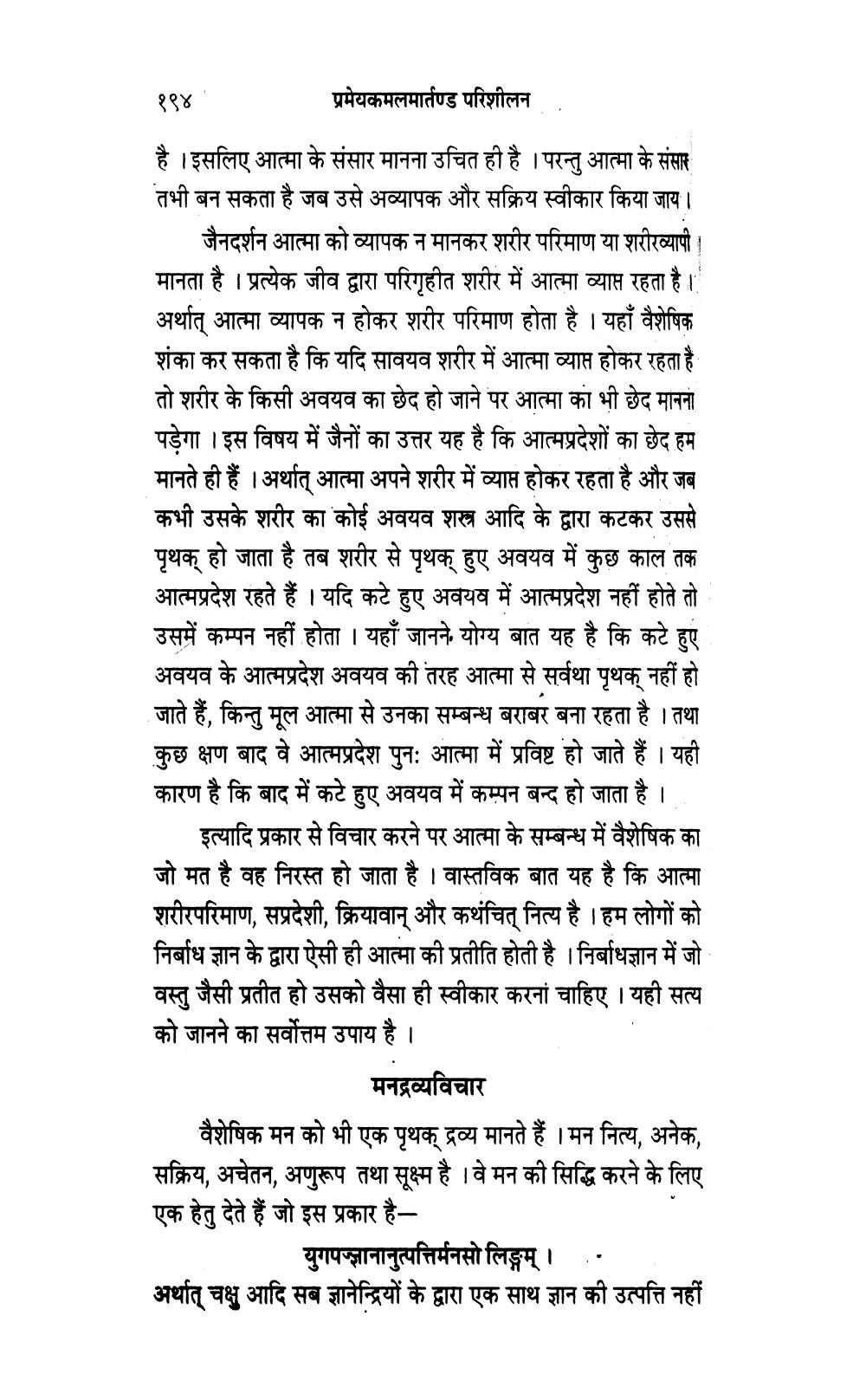________________
१९४
प्रमेयकमलमार्तण्ड परिशीलन .. है । इसलिए आत्मा के संसार मानना उचित ही है । परन्तु आत्मा के संसार तभी बन सकता है जब उसे अव्यापक और सक्रिय स्वीकार किया जाय।
जैनदर्शन आत्मा को व्यापक न मानकर शरीर परिमाण या शरीरव्यापी मानता है । प्रत्येक जीव द्वारा परिगृहीत शरीर में आत्मा व्याप्त रहता है। अर्थात् आत्मा व्यापक न होकर शरीर परिमाण होता है । यहाँ वैशेषिक शंका कर सकता है कि यदि सावयव शरीर में आत्मा व्याप्त होकर रहता है तो शरीर के किसी अवयव का छेद हो जाने पर आत्मा का भी छेद मानना पड़ेगा । इस विषय में जैनों का उत्तर यह है कि आत्मप्रदेशों का छेद हम मानते ही हैं । अर्थात् आत्मा अपने शरीर में व्याप्त होकर रहता है और जब कभी उसके शरीर का कोई अवयव शस्त्र आदि के द्वारा कटकर उससे पृथक् हो जाता है तब शरीर से पृथक् हुए अवयव में कुछ काल तक आत्मप्रदेश रहते हैं । यदि कटे हुए अवयव में आत्मप्रदेश नहीं होते तो उसमें कम्पन नहीं होता । यहाँ जानने योग्य बात यह है कि कटे हुए अवयव के आत्मप्रदेश अवयव की तरह आत्मा से सर्वथा पृथक् नहीं हो जाते हैं, किन्तु मूल आत्मा से उनका सम्बन्ध बराबर बना रहता है । तथा कुछ क्षण बाद वे आत्मप्रदेश पुनः आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं । यही कारण है कि बाद में कटे हुए अवयव में कम्पन बन्द हो जाता है। . ___इत्यादि प्रकार से विचार करने पर आत्मा के सम्बन्ध में वैशेषिक का जो मत है वह निरस्त हो जाता है । वास्तविक बात यह है कि आत्मा शरीरपरिमाण, सप्रदेशी, क्रियावान् और कथंचित् नित्य है । हम लोगों को निर्बाध ज्ञान के द्वारा ऐसी ही आत्मा की प्रतीति होती है । निर्बाधज्ञान में जो वस्तु जैसी प्रतीत हो उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए । यही सत्य को जानने का सर्वोत्तम उपाय है ।
मनद्रव्यविचार वैशेषिक मन को भी एक पृथक् द्रव्य मानते हैं । मन नित्य, अनेक, सक्रिय, अचेतन, अणुरूप तथा सूक्ष्म है । वे मन की सिद्धि करने के लिए एक हेतु देते हैं जो इस प्रकार है
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् । .. अर्थात् चक्षु आदि सब ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं