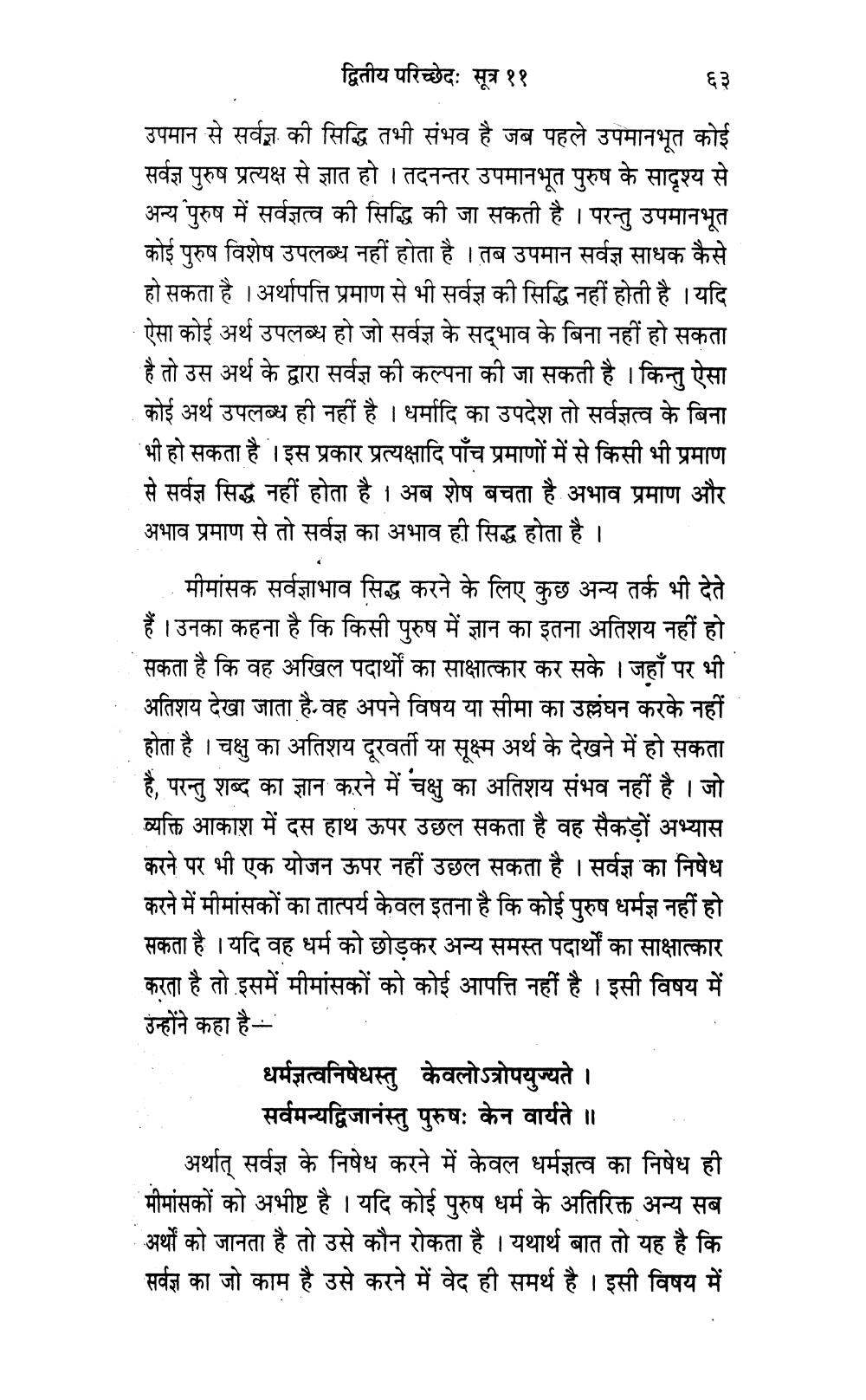________________
द्वितीय परिच्छेदः सूत्र ११
६३
उपमान से सर्वज्ञ की सिद्धि तभी संभव है जब पहले उपमानभूत कोई सर्वज्ञ पुरुष प्रत्यक्ष से ज्ञात हो । तदनन्तर उपमानभूत पुरुष के सादृश्य से अन्य पुरुष में सर्वज्ञत्व की सिद्धि की जा सकती है । परन्तु उपमानभूत कोई पुरुष विशेष उपलब्ध नहीं होता है । तब उपमान सर्वज्ञ साधक कैसे हो सकता है । अर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती है । यदि ऐसा कोई अर्थ उपलब्ध हो जो सर्वज्ञ के सद्भाव के बिना नहीं हो सकता है तो उस अर्थ के द्वारा सर्वज्ञ की कल्पना की जा सकती है । किन्तु ऐसा कोई अर्थ उपलब्ध ही नहीं है । धर्मादि का उपदेश तो सर्वज्ञत्व के बिना भी हो सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है । अब शेष बचता है अभाव प्रमाण और अभाव प्रमाण से तो सर्वज्ञ का अभाव ही सिद्ध होता है ।
1
मीमांसक सर्वज्ञाभाव सिद्ध करने के लिए कुछ अन्य तर्क भी देते हैं । उनका कहना है कि किसी पुरुष में ज्ञान का इतना अतिशय नहीं हो सकता है कि वह अखिल पदार्थों का साक्षात्कार कर सके । जहाँ पर भी अतिशय देखा जाता है. वह अपने विषय या सीमा का उल्लंघन करके नहीं होता है । चक्षु का अतिशय दूरवर्ती या सूक्ष्म अर्थ के देखने में हो सकता हैं, परन्तु शब्द का ज्ञान करने में चक्षु का अतिशय संभव नहीं है । जो व्यक्ति आकाश में दस हाथ ऊपर उछल सकता है वह सैकड़ों अभ्यास करने पर भी एक योजन ऊपर नहीं उछल सकता है । सर्वज्ञ का निषेध करने में मीमांसकों का तात्पर्य केवल इतना है कि कोई पुरुष धर्मज्ञ नहीं हो सकता है । यदि वह धर्म को छोड़कर अन्य समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करता है तो इसमें मीमांसकों को कोई आपत्ति नहीं है । इसी विषय में उन्होंने कहा है
-
धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥
अर्थात् सर्वज्ञ के निषेध करने में केवल धर्मज्ञत्व का निषेध ही मीमांसकों को अभीष्ट है । यदि कोई पुरुष धर्म के अतिरिक्त अन्य सब अर्थों को जानता है तो उसे कौन रोकता है । यथार्थ बात तो यह है कि सर्वज्ञ का जो काम है उसे करने में वेद ही समर्थ है । इसी विषय में