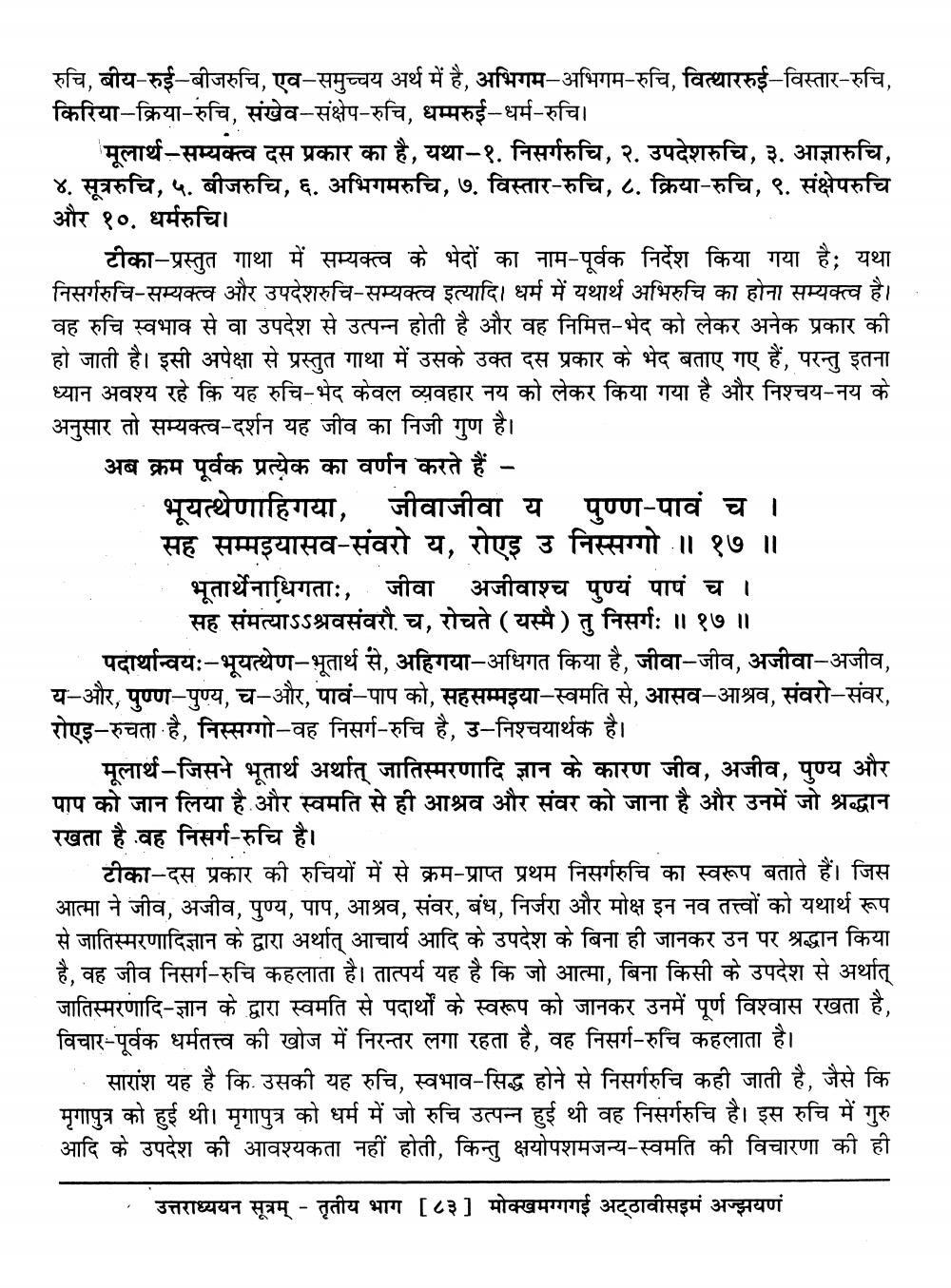________________
रुचि, बीय-रुई-बीजरुचि, एव-समुच्चय अर्थ में है, अभिगम-अभिगम-रुचि, वित्थाररुई-विस्तार-रुचि, किरिया-क्रिया-रुचि, संखेव-संक्षेप-रुचि, धम्मरुई-धर्म-रुचि।
मूलार्थ-सम्यक्त्व दस प्रकार का है, यथा-१. निसर्गरुचि, २. उपदेशरुचि, ३. आज्ञारुचि, ४. सूत्ररुचि, ५. बीजरुचि, ६. अभिगमरुचि, ७. विस्तार-रुचि, ८. क्रिया-रुचि, ९. संक्षेपरुचि और १०. धर्मरुचि।
टीका-प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के भेदों का नाम-पूर्वक निर्देश किया गया है; यथा निसर्गरुचि-सम्यक्त्व और उपदेशरुचि-सम्यक्त्व इत्यादि। धर्म में यथार्थ अभिरुचि का होना सम्यक्त्व है। वह रुचि स्वभाव से वा उपदेश से उत्पन्न होती है और वह निमित्त-भेद को लेकर अनेक प्रकार की हो जाती है। इसी अपेक्षा से प्रस्तुत गाथा में उसके उक्त दस प्रकार के भेद बताए गए हैं, परन्तु इतना ध्यान अवश्य रहे कि यह रुचि-भेद केवल व्यवहार नय को लेकर किया गया है और निश्चय-नय के अनुसार तो सम्यक्त्व-दर्शन यह जीव का निजी गुण है। अब क्रम पूर्वक प्रत्येक का वर्णन करते हैं -
भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च । सह सम्मइयासव-संवरो य, रोएइ उ निस्सग्गो ॥ १७ ॥ . भूतार्थेनाधिगताः, जीवा अजीवाश्च पुण्यं पापं च ।
सह संमत्याऽऽश्रवसंवरौ. च, रोचते (यस्मै) तु निसर्गः ॥ १७ ॥ पदार्थान्वयः-भूयत्थेण-भूतार्थ से, अहिगया-अधिगत किया है, जीवा-जीव, अजीवा-अजीव, य-और, पुण्ण-पुण्य, च-और, पावं-पाप को, सहसम्मइया-स्वमति से, आसव-आश्रव, संवरो-संवर, रोएइ-रुचता है, निस्सग्गो-वह निसर्ग-रुचि है, उ-निश्चयार्थक है।
मूलार्थ-जिसने भूतार्थ अर्थात् जातिस्मरणादि ज्ञान के कारण जीव, अजीव, पुण्य और पाप को जान लिया है और स्वमति से ही आश्रव और संवर को जाना है और उनमें जो श्रद्धान रखता है वह निसर्ग-रुचि है।।
टीका-दस प्रकार की रुचियों में से क्रम-प्राप्त प्रथम निसर्गरुचि का स्वरूप बताते हैं। जिस आत्मा ने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष इन नव तत्त्वों को यथार्थ रूप से जातिस्मरणादिज्ञान के द्वारा अर्थात् आचार्य आदि के उपदेश के बिना ही जानकर उन पर श्रद्धान किया है, वह जीव निसर्ग-रुचि कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जो आत्मा, बिना किसी के उपदेश से अर्थात् जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा स्वमति से पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनमें पूर्ण विश्वास रखता है, विचार-पूर्वक धर्मतत्त्व की खोज में निरन्तर लगा रहता है, वह निसर्ग-रुचि कहलाता है। .. सारांश यह है कि उसकी यह रुचि, स्वभाव-सिद्ध होने से निसर्गरुचि कही जाती है, जैसे कि मृगापुत्र को हुई थी। मृगापुत्र को धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई थी वह निसर्गरुचि है। इस रुचि में गुरु आदि के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु क्षयोपशमजन्य-स्वमति की विचारणा की ही
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [८३] मोक्खमग्गगई अट्ठावीसइमं अज्झयणं