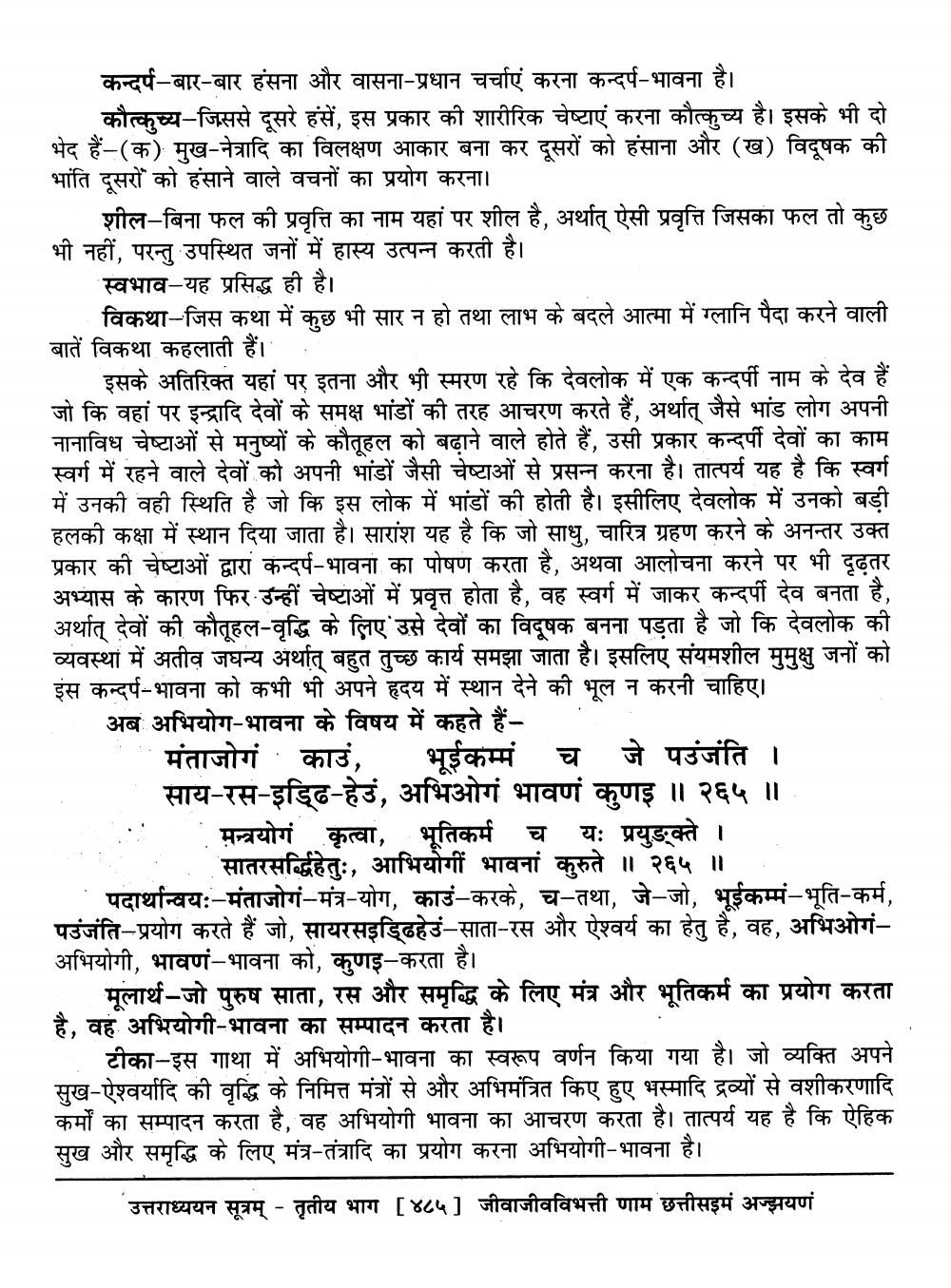________________
कन्दर्प - बार-बार हंसना और वासना - प्रधान चर्चाएं करना कन्दर्प - भावना है।
कौत्कुच्य - जिससे दूसरे हंसें, इस प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं करना कौत्कुच्य है। इसके भी दो भेद हैं- (क) मुख-नेत्रादि का विलक्षण आकार बना कर दूसरों को हंसाना और (ख) विदूषक की भांति दूसरों को हंसाने वाले वचनों का प्रयोग करना ।
शील - बिना फल की प्रवृत्ति का नाम यहां पर शील है, अर्थात् ऐसी प्रवृत्ति जिसका फल तो कुछ भी नहीं, परन्तु उपस्थित जनों में हास्य उत्पन्न करती है ।
स्वभाव - यह प्रसिद्ध ही है।
विकथा - जिस कथा में कुछ भी सार न हो तथा लाभ के बदले आत्मा में ग्लानि पैदा करने वाली बातें विकथा कहलाती हैं।
इसके अतिरिक्त यहां पर इतना और भी स्मरण रहे कि देवलोक में एक कन्दर्पी नाम के देव हैं जो कि वहां पर इन्द्रादि देवों के समक्ष भांडों की तरह आचरण करते हैं, अर्थात् जैसे भांड लोग अपनी नानाविध चेष्टाओं से मनुष्यों के कौतूहल को बढ़ाने वाले होते हैं, उसी प्रकार कन्दर्पी देवों का काम स्वर्ग में रहने वाले देवों को अपनी भांडों जैसी चेष्टाओं से प्रसन्न करना है। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग में उनकी वही स्थिति है जो कि इस लोक में भांडों की होती है। इसीलिए देवलोक में उनको बड़ी हलकी कक्षा में स्थान दिया जाता है । सारांश यह है कि जो साधु, चारित्र ग्रहण करने के अनन्तर उक्त प्रकार की चेष्टाओं द्वारा कन्दर्प- भावना का पोषण करता है, अथवा आलोचना करने पर भी दृढ़तर अभ्यास के कारण फिर उन्हीं चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है, वह स्वर्ग में जाकर कन्दर्पी देव बनता है, अर्थात् देवों की कौतूहल - वृद्धि के लिए उसे देवों का विदूषक बनना पड़ता है जो कि देवलोक की व्यवस्था में अतीव जघन्य अर्थात् बहुत तुच्छ कार्य समझा जाता है। इसलिए संयमशील मुमुक्षु जनों को इस कन्दर्प - भावना को कभी भी अपने हृदय में स्थान देने की भूल न करनी चाहिए ।
अब अभियोग- भावना के विषय में कहते हैं
मंताजोगं काउं, भूईकम्मं च जे पउंजंति । साय-रस- इड्ढि - हेडं, अभिओगं भावणं कुणइ ॥ २६५ ॥ मन्त्रयोगं कृत्वा, भूतिकर्म च यः प्रयुङ्क्ते । सातरसर्द्धिहेतुः, आभियोगीं भावनां कुरुते ॥ २६५ ॥
पदार्थान्वयः - मंताजोगं-मंत्र-योग, काउं-करके, च-तथा, जे - जो, भूईकम्मं - भूति - कर्म, पउंजंति-प्रयोग करते हैं जो, सायरसइड्ढिहेउ - - साता - रस और ऐश्वर्य का हेतु है, वह, अभिओगंअभियोगी, भावणं- भावना को, कुणइ - करता है।
मूलार्थ - जो पुरुष साता, रस और समृद्धि के लिए मंत्र और भूतिकर्म का प्रयोग करता है, वह अभियोगी - भावना का सम्पादन करता है।
टीका - इस गाथा में अभियोगी - भावना का स्वरूप वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति अपने सुख - ऐश्वर्यादि की वृद्धि के निमित्त मंत्रों से और अभिमंत्रित किए हुए भस्मादि द्रव्यों से वशीकरणादि कर्मों का सम्पादन करता है, वह अभियोगी भावना का आचरण करता है। तात्पर्य यह है कि ऐहिक सुख और समृद्धि के लिए मंत्र-तंत्रादि का प्रयोग करना अभियोगी - भावना है।
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ ४८५ ] जीवाजीवविभत्ती णाम छत्तीसइमं अज्झयणं