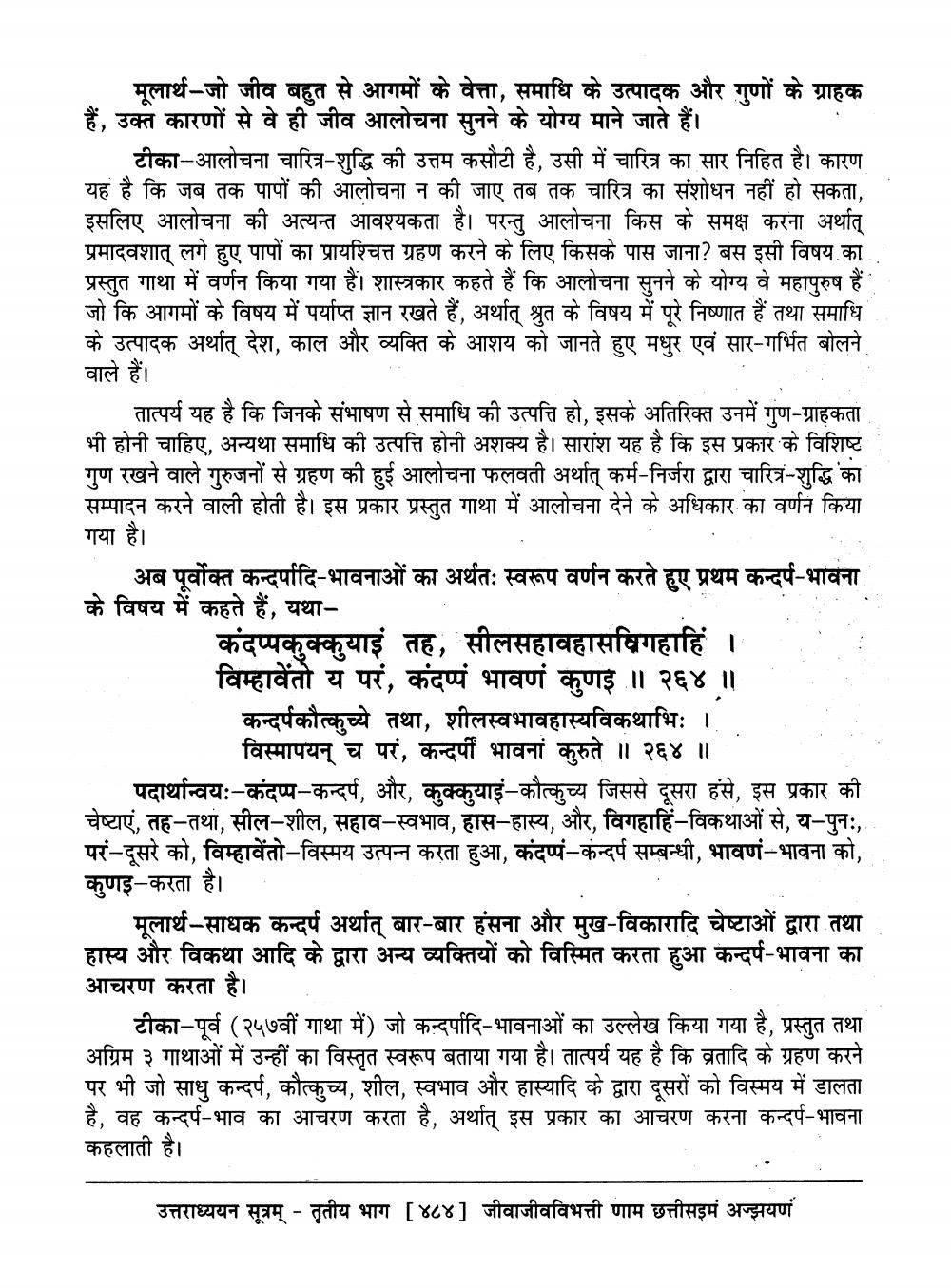________________
मूलार्थ-जो जीव बहुत से आगमों के वेत्ता, समाधि के उत्पादक और गुणों के ग्राहक हैं, उक्त कारणों से वे ही जीव आलोचना सुनने के योग्य माने जाते हैं।
टीका-आलोचना चारित्र-शुद्धि की उत्तम कसौटी है, उसी में चारित्र का सार निहित है। कारण यह है कि जब तक पापों की आलोचना न की जाए तब तक चारित्र का संशोधन न इसलिए आलोचना की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु आलोचना किस के समक्ष करना प्रमादवशात् लगे हुए पापों का प्रायश्चित्त ग्रहण करने के लिए किसके पास जाना? बस इसी विषय का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आलोचना सुनने के योग्य वे महापुरुष हैं जो कि आगमों के विषय में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, अर्थात् श्रुत के विषय में पूरे निष्णात हैं तथा समाधि के उत्पादक अर्थात् देश, काल और व्यक्ति के आशय को जानते हुए मधुर एवं सार-गर्भित बोलने वाले हैं।
तात्पर्य यह है कि जिनके संभाषण से समाधि की उत्पत्ति हो, इसके अतिरिक्त उनमें गुण-ग्राहकता भी होनी चाहिए, अन्यथा समाधि की उत्पत्ति होनी अशक्य है। सारांश यह है कि इस प्रकार के विशिष्ट गुण रखने वाले गुरुजनों से ग्रहण की हुई आलोचना फलवती अर्थात् कर्म-निर्जरा द्वारा चारित्र-शुद्धिका सम्पादन करने वाली होती है। इस प्रकार प्रस्तुत गाथा में आलोचना देने के अधिकार का वर्णन किया गया है।
अब पूर्वोक्त कन्दर्पादि-भावनाओं का अर्थतः स्वरूप वर्णन करते हुए प्रथम कन्दर्प-भावना के विषय में कहते हैं, यथा
कंदप्पकुक्कुयाइं तह, सीलसहावहासविगहाहिं । विम्हावेतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥ २६४ ॥
कन्दर्पकौत्कुच्ये तथा, शीलस्वभावहास्यविकथाभिः ।
विस्मापयन् च परं, कन्दी भावनां कुरुते ॥ २६४ ॥ पदार्थान्वयः-कंदप्प-कन्दर्प, और, कुक्कुयाइं-कौत्कुच्य जिससे दूसरा हंसे, इस प्रकार की चेष्टाएं, तह-तथा, सील-शील, सहाव-स्वभाव, हास-हास्य, और, विगहाहि-विकथाओं से, य-पुनः, परं-दूसरे को, विम्हावेंतो-विस्मय उत्पन्न करता हुआ, कंदप्पं-कन्दर्प सम्बन्धी, भावणं-भावना को, कुणइ-करता है।
मूलार्थ-साधक कन्दर्प अर्थात् बार-बार हंसना और मुख-विकारादि चेष्टाओं द्वारा तथा हास्य और विकथा आदि के द्वारा अन्य व्यक्तियों को विस्मित करता हुआ कन्दर्प-भावना का आचरण करता है।
टीका-पूर्व (२५७वीं गाथा में) जो कन्दर्पादि-भावनाओं का उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत तथा अग्रिम ३ गाथाओं में उन्हीं का विस्तृत स्वरूप बताया गया है। तात्पर्य यह है कि व्रतादि के ग्रहण करने पर भी जो साधु कन्दर्प, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव और हास्यादि के द्वारा दूसरों को विस्मय में डालता है, वह कन्दर्प-भाव का आचरण करता है, अर्थात् इस प्रकार का आचरण करना कन्दर्प-भावना कहलाती है।
.
.
.
.
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ ४८४] जीवाजीवविभत्ती णाम छत्तीसइमं अज्झयणं