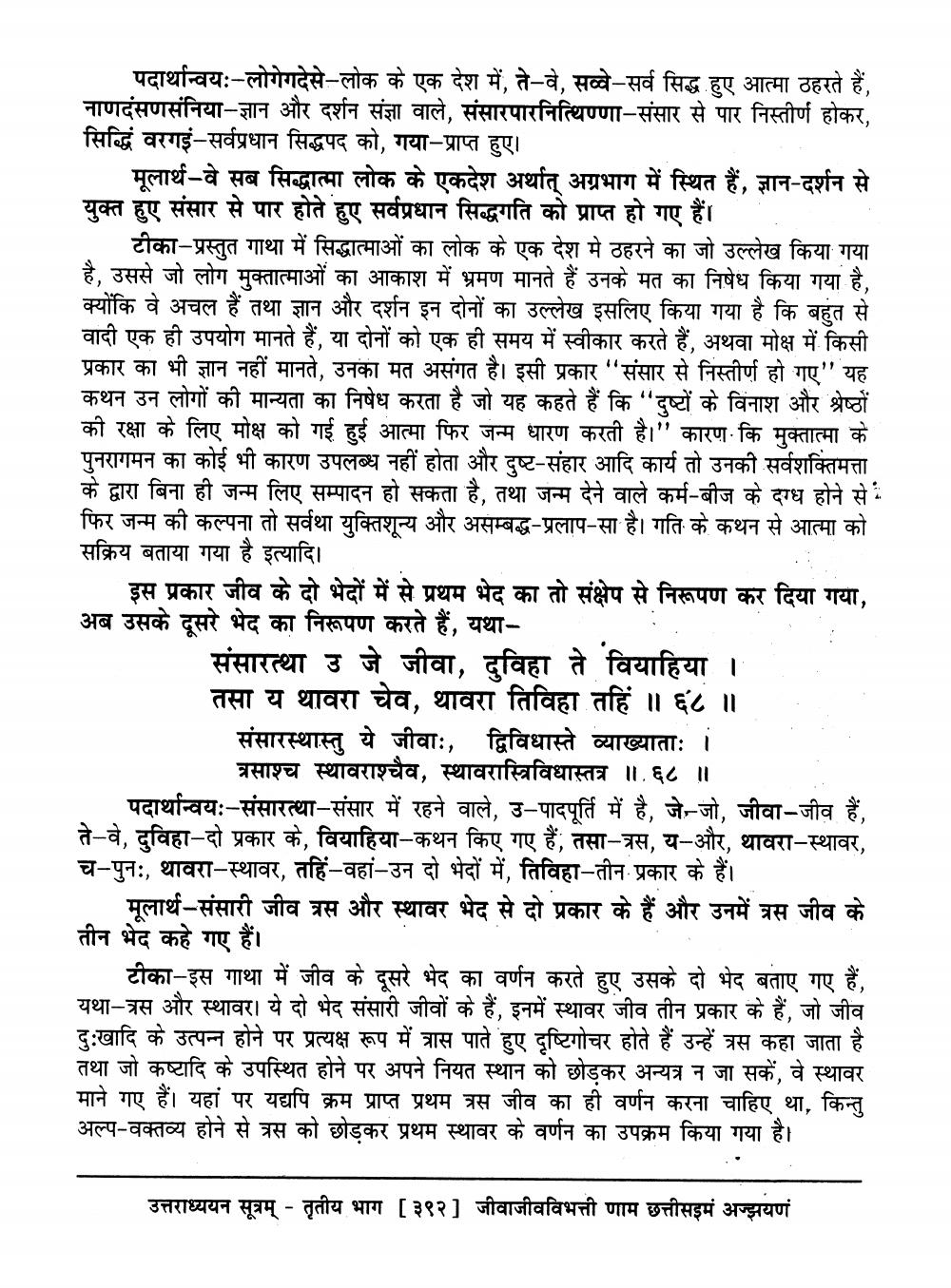________________
पदार्थान्वयः-लोगेगदेसे-लोक के एक देश में, ते-वे, सव्वे-सर्व सिद्ध हुए आत्मा ठहरते हैं, नाणदंसणसंनिया-ज्ञान और दर्शन संज्ञा वाले, संसारपारनित्थिण्णा-संसार से पार निस्तीर्ण होकर, सिद्धिं वरगई-सर्वप्रधान सिद्धपद को, गया-प्राप्त हुए।
मूलार्थ-वे सब सिद्धात्मा लोक के एकदेश अर्थात् अग्रभाग में स्थित हैं, ज्ञान-दर्शन से युक्त हुए संसार से पार होते हुए सर्वप्रधान सिद्धगति को प्राप्त हो गए हैं। ___टीका-प्रस्तुत गाथा में सिद्धात्माओं का लोक के एक देश मे ठहरने का जो उल्लेख किया गया है, उससे जो लोग मुक्तात्माओं का आकाश में भ्रमण मानते हैं उनके मत का निषेध किया गया है, क्योंकि वे अचल हैं तथा ज्ञान और दर्शन इन दोनों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि बहुत से वादी एक ही उपयोग मानते हैं, या दोनों को एक ही समय में स्वीकार करते हैं, अथवा मोक्ष में किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं मानते, उनका मत असंगत है। इसी प्रकार "संसार से निस्तीर्ण हो गए" यह कथन उन लोगों की मान्यता का निषेध करता है जो यह कहते हैं कि "दुष्टों के विनाश और श्रेष्ठों की रक्षा के लिए मोक्ष को गई हुई आत्मा फिर जन्म धारण करती है।" कारण कि मुक्तात्मा के पुनरागमन का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता और दुष्ट-संहार आदि कार्य तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा बिना ही जन्म लिए सम्पादन हो सकता है, तथा जन्म देने वाले कर्म-बीज के दग्ध होने से फिर जन्म की कल्पना तो सर्वथा युक्तिशून्य और असम्बद्ध-प्रलाप-सा है। गति के कथन से आत्मा को सक्रिय बताया गया है इत्यादि।
इस प्रकार जीव के दो भेदों में से प्रथम भेद का तो संक्षेप से निरूपण कर दिया गया, अब उसके दूसरे भेद का निरूपण करते हैं, यथा
संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया । तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहिं ॥ ६८ ॥ संसारस्थास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।
त्रसाश्च स्थावराश्चैव, स्थावरास्त्रिविधास्तत्र ॥.६८ ॥ पदार्थान्वयः-संसारत्था-संसार में रहने वाले, उ-पादपूर्ति में है, जे-जो, जीवा-जीव हैं, ते-वे, दुविहा-दो प्रकार के, वियाहिया-कथन किए गए हैं, तसा-त्रस, य-और, थावरा-स्थावर, च-पुनः, थावरा-स्थावर, तहिं-वहां-उन दो भेदों में, तिविहा-तीन प्रकार के हैं।
मूलार्थ-संसारी जीव त्रस और स्थावर भेद से दो प्रकार के हैं और उनमें त्रस जीव के तीन भेद कहे गए हैं।
___टीका-इस गाथा में जीव के दूसरे भेद का वर्णन करते हुए उसके दो भेद बताए गए हैं, यथा-वस और स्थावर। ये दो भेद संसारी जीवों के हैं, इनमें स्थावर जीव तीन प्रकार के हैं, जो जीव दुःखादि के उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष रूप में त्रास पाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें त्रस कहा जाता है तथा जो कष्टादि के उपस्थित होने पर अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्यत्र न जा सकें, वे स्थावर माने गए हैं। यहां पर यद्यपि क्रम प्राप्त प्रथम त्रस जीव का ही वर्णन करना चाहिए था, किन्तु अल्प-वक्तव्य होने से त्रस को छोड़कर प्रथम स्थावर के वर्णन का उपक्रम किया गया है।
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [३९२] जीवाजीवविभत्ती णाम छत्तीसइमं अज्झयणं