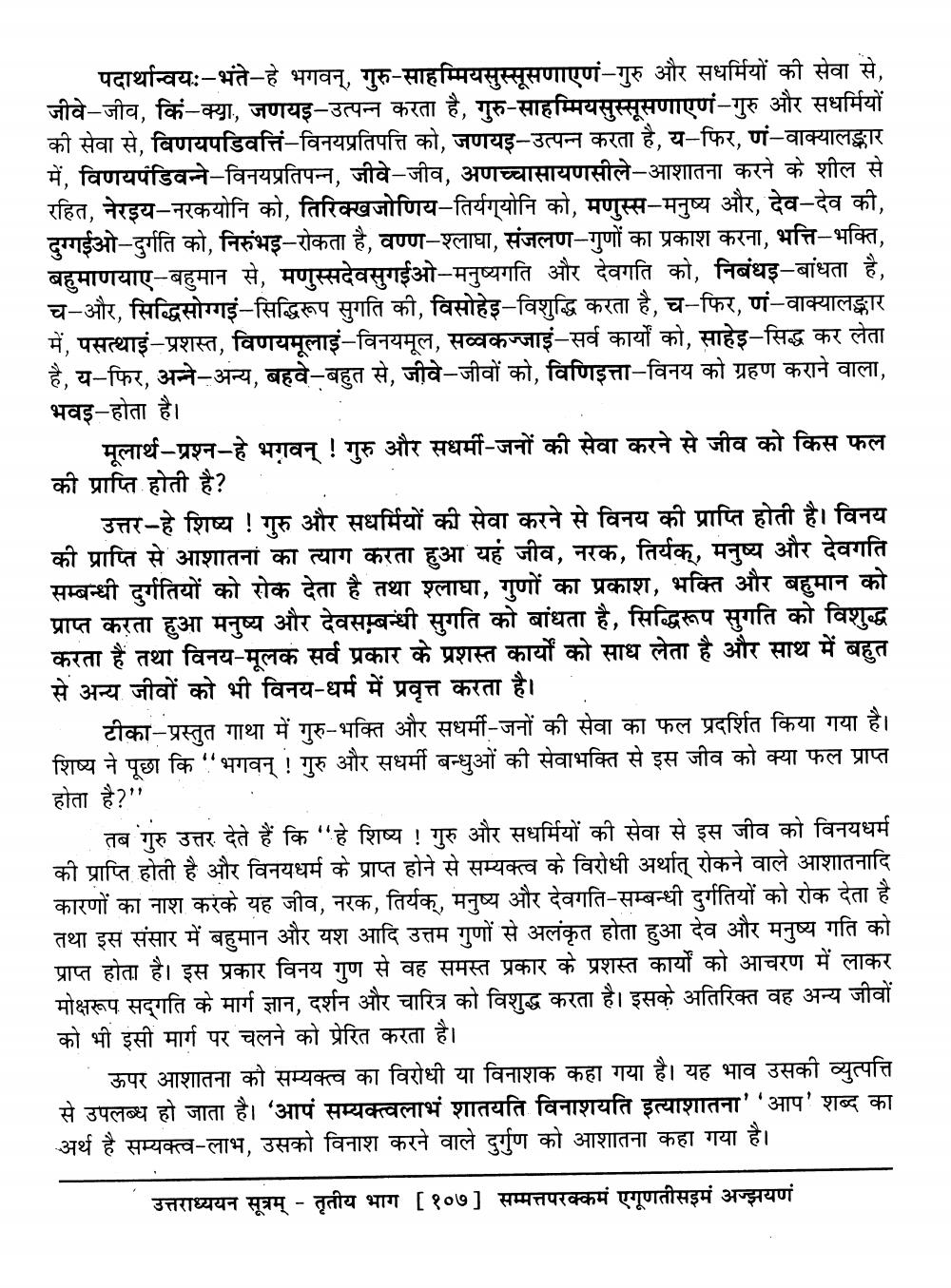________________
पदार्थान्वयः-भंते-हे भगवन्, गुरु-साहम्मियसुस्सूसणाएणं-गुरु और सधर्मियों की सेवा से, जीवे-जीव, किं-क्या, जणयइ-उत्पन्न करता है, गुरु-साहम्मियसुस्सूसणाएणं-गुरु और सधर्मियों की सेवा से, विणयपडिवत्तिं-विनयप्रतिपत्ति को, जणयइ-उत्पन्न करता है, य-फिर, णं-वाक्यालङ्कार में, विणयपंडिवन्ने-विनयप्रतिपन्न, जीव-जीव, अणच्चासायणसीले-आशातना करने के शील से रहित, नेरइय-नरकयोनि को, तिरिक्खजोणिय-तिर्यग्योनि को, मणुस्स-मनुष्य और, देव-देव की, दुग्गईओ-दुर्गति को, निरंभइ-रोकता है, वण्ण-श्लाघा, संजलण-गुणों का प्रकाश करना, भत्ति-भक्ति, बहुमाणयाए-बहुमान से, मणुस्सदेवसुगईओ-मनुष्यगति और देवगति को, निबंधइ-बांधता है, च-और, सिद्धिसोग्गइं-सिद्धिरूप सुगति की, विसोहेइ-विशुद्धि करता है, च-फिर, णं-वाक्यालङ्कार में, पसत्थाई-प्रशस्त, विणयमूलाई-विनयमूल, सव्वकज्जाइं-सर्व कार्यों को, साहेइ-सिद्ध कर लेता है, य-फिर, अन्ने-अन्य, बहवे-बहुत से, जीवे-जीवों को, विणिइत्ता-विनय को ग्रहण कराने वाला, भवइ-होता है। ___ मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! गुरु और सधर्मी-जनों की सेवा करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है?
उत्तर-हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा करने से विनय की प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति से आशातनां का त्याग करता हुआ यह जीव, नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगति सम्बन्धी दुर्गतियों को रोक देता है तथा श्लाघा, गुणों का प्रकाश, भक्ति और बहुमान को प्राप्त करता हुआ मनुष्य और देवसम्बन्धी सुगति को बांधता है, सिद्धिरूप सुगति को विशुद्ध करता हैं तथा विनय-मूलक सर्व प्रकार के प्रशस्त कार्यों को साध लेता है और साथ में बहुत से अन्य जीवों को भी विनय-धर्म में प्रवृत्त करता है।
टीका-प्रस्तुत गाथा में गुरु-भक्ति और सधर्मी-जनों की सेवा का फल प्रदर्शित किया गया है। शिष्य ने पूछा कि "भगवन् ! गुरु और सधर्मी बन्धुओं की सेवाभक्ति से इस जीव को क्या फल प्राप्त
होता है?"
___ तब गुरु उत्तर देते हैं कि "हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा से इस जीव को विनयधर्म की प्राप्ति होती है और विनयधर्म के प्राप्त होने से सम्यक्त्व के विरोधी अर्थात् रोकने वाले आशातनादि कारणों का नाश करके यह जीव, नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगति-सम्बन्धी दुर्गतियों को रोक देता है तथा इस संसार में बहुमान और यश आदि उत्तम गुणों से अलंकृत होता हुआ देव और मनुष्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विनय गुण से वह समस्त प्रकार के प्रशस्त कार्यों को आचरण में लाकर मोक्षरूप सद्गति के मार्ग ज्ञान, दर्शन और चारित्र को विशुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य जीवों को भी इसी मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है।
ऊपर आशातना को सम्यक्त्व का विरोधी या विनाशक कहा गया है। यह भाव उसकी व्युत्पत्ति से उपलब्ध हो जाता है। 'आपं सम्यक्त्वलाभं शातयति विनाशयति इत्याशातना' 'आप' शब्द का अर्थ है सम्यक्त्व-लाभ, उसको विनाश करने वाले दुर्गुण को आशातना कहा गया है।
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ १०७] सम्मत्तपरक्कम एगूणतीसइमं अज्झयणं