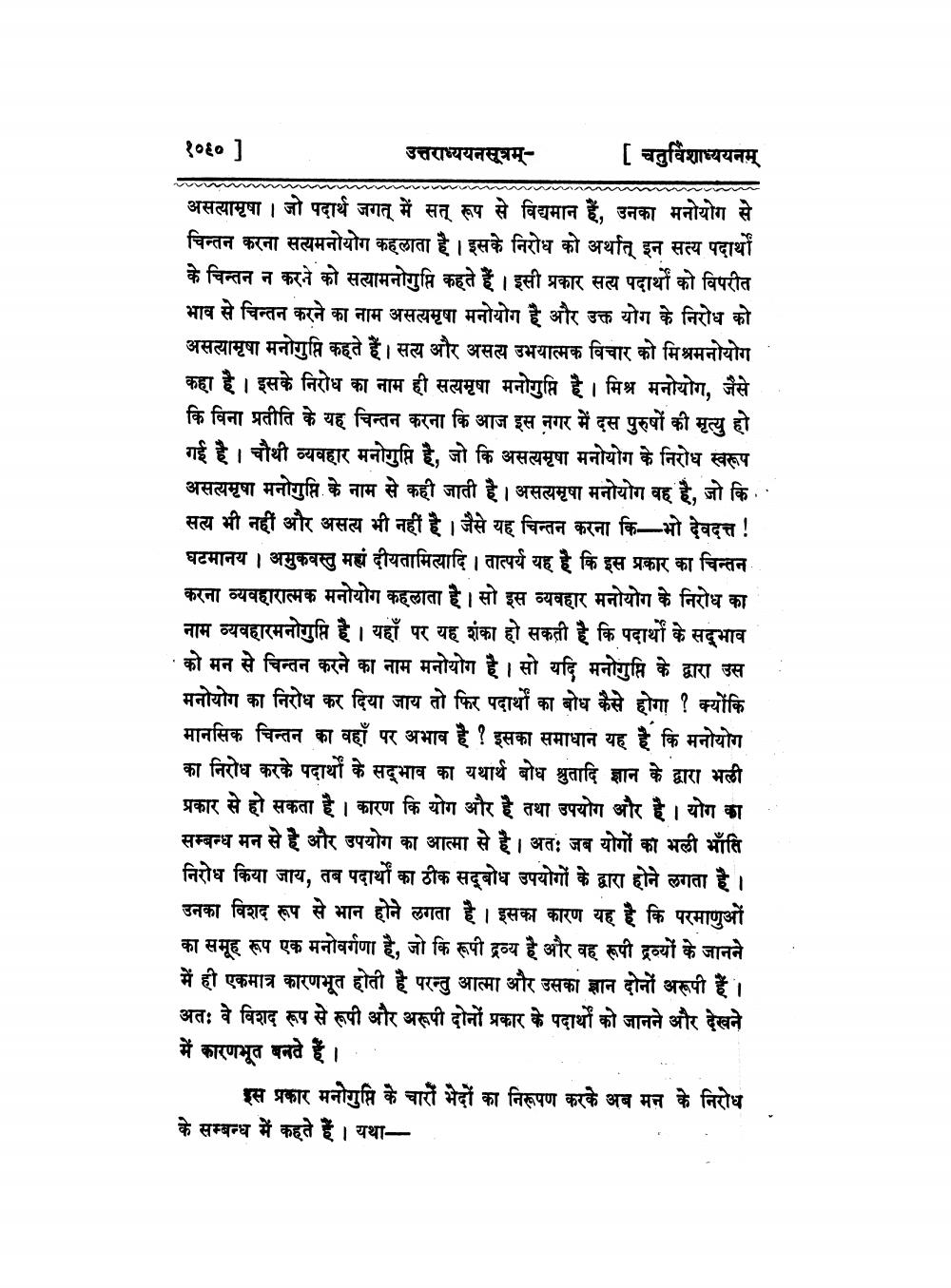________________
१०६० ]
उत्तराध्ययनसूत्रम्-
[चतुर्विंशाध्ययनम्
असत्यामृषा । जो पदार्थ जगत् में सत् रूप से विद्यमान हैं, उनका मनोयोग से चिन्तन करना सत्यमनोयोग कहलाता है । इसके निरोध को अर्थात् इन सत्य पदार्थों के चिन्तन न करने को सत्यामनोगुप्ति कहते हैं । इसी प्रकार सत्य पदार्थों को विपरीत भाव से चिन्तन करने का नाम असत्यमृषा मनोयोग है और उक्त योग के निरोध को असत्यामृषा मनोगुप्ति कहते हैं। सत्य और असत्य उभयात्मक विचार को मिश्रमनोयोग कहा है। इसके निरोध का नाम ही सत्यमृषा मनोगुप्ति है। मिश्र मनोयोग, जैसे कि विना प्रतीति के यह चिन्तन करना कि आज इस नगर में दस पुरुषों की मृत्यु हो गई है। चौथी व्यवहार मनोगुप्ति है, जो कि असत्यमृषा मनोयोग के निरोध स्वरूप असत्यमृषा मनोगुप्ति के नाम से कही जाती है। असत्यमृषा मनोयोग वह है, जो कि . . सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है । जैसे यह चिन्तन करना कि-भो देवदत्त ! घटमानय । अमुकवस्तु मह्यं दीयतामित्यादि । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का चिन्तन करना व्यवहारात्मक मनोयोग कहलाता है। सो इस व्यवहार मनोयोग के निरोध का नाम व्यवहारमनोगुप्ति है। यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि पदार्थों के सद्भाव को मन से चिन्तन करने का नाम मनोयोग है । सो यदि मनोगुप्ति के द्वारा उस मनोयोग का निरोध कर दिया जाय तो फिर पदार्थों का बोध कैसे होगा ? क्योंकि मानसिक चिन्तन का वहाँ पर अभाव है ? इसका समाधान यह है कि मनोयोग का निरोध करके पदार्थों के सद्भाव का यथार्थ बोध श्रुतादि ज्ञान के द्वारा भली प्रकार से हो सकता है। कारण कि योग और है तथा उपयोग और है। योग का सम्बन्ध मन से है और उपयोग का आत्मा से है। अतः जब योगों का भली भाँति निरोध किया जाय, तब पदार्थों का ठीक सद्बोध उपयोगों के द्वारा होने लगता है। उनका विशद रूप से भान होने लगता है। इसका कारण यह है कि परमाणुओं का समूह रूप एक मनोवर्गणा है, जो कि रूपी द्रव्य है और वह रूपी द्रव्यों के जानने में ही एकमात्र कारणभूत होती है परन्तु आत्मा और उसका ज्ञान दोनों अरूपी हैं। अतः वे विशद रूप से रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जानने और देखने में कारणभूत बनते हैं।
इस प्रकार मनोगुप्ति के चारों भेदों का निरूपण करके अब मन के निरोध के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा