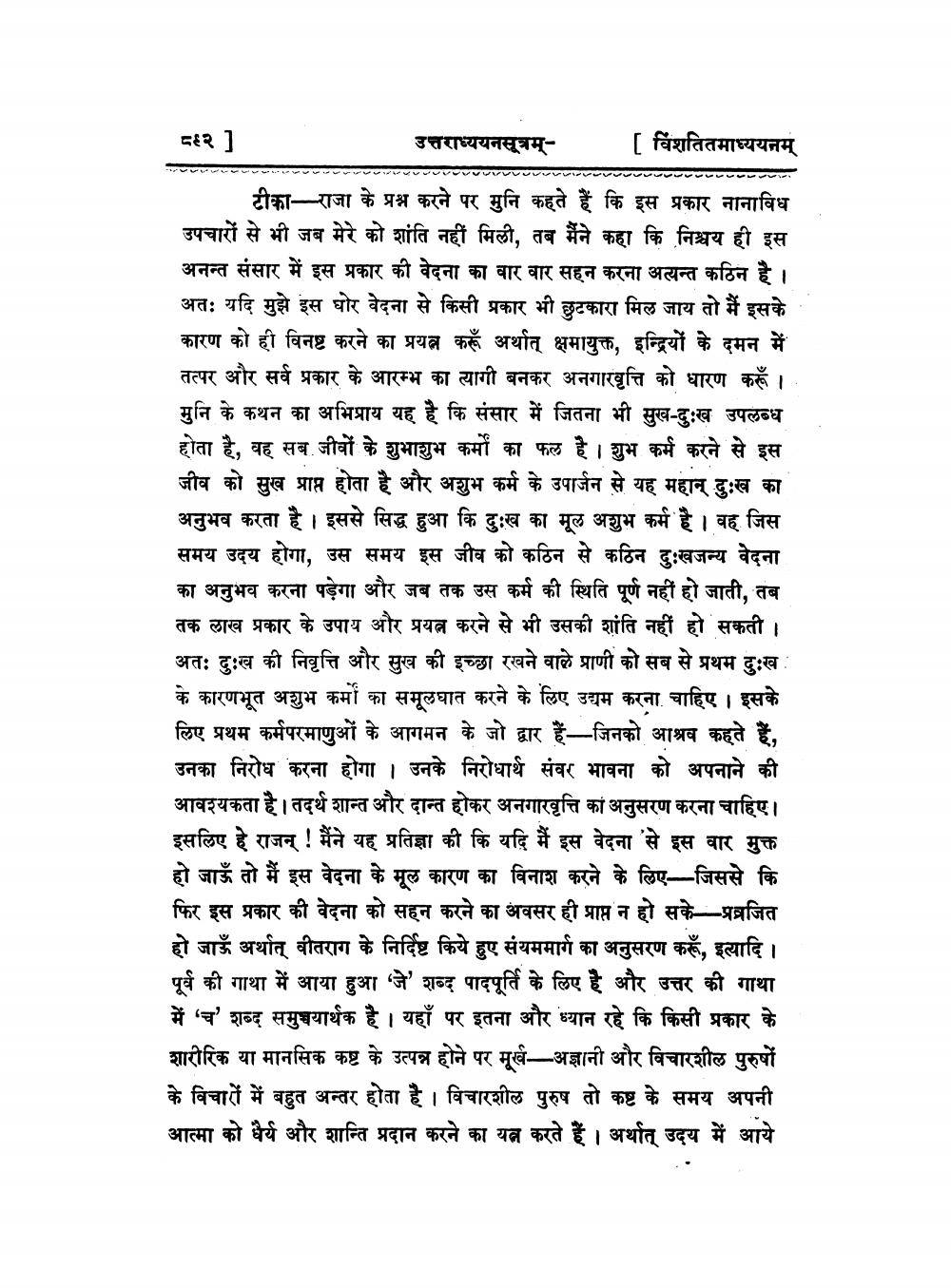________________
८२]
उत्तराध्ययनसूत्रम्-
[विंशतितमाध्ययनम्
पन्न
टीका-राजा के प्रश्न करने पर मुनि कहते हैं कि इस प्रकार नानाविध उपचारों से भी जब मेरे को शांति नहीं मिली, तब मैंने कहा कि निश्चय ही इस अनन्त संसार में इस प्रकार की वेदना का वार वार सहन करना अत्यन्त कठिन है। अतः यदि मुझे इस घोर वेदना से किसी प्रकार भी छुटकारा मिल जाय तो मैं इसके कारण को ही विनष्ट करने का प्रयत्न करूँ अर्थात् क्षमायुक्त, इन्द्रियों के दमन में तत्पर और सर्व प्रकार के आरम्भ का त्यागी बनकर अनगारवृत्ति को धारण करूँ । मुनि के कथन का अभिप्राय यह है कि संसार में जितना भी सुख-दुःख उपलब्ध होता है, वह सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल है। शुभ कर्म करने से इस जीव को सुख प्राप्त होता है और अशुभ कर्म के उपार्जन से यह महान् दुःख का अनुभव करता है। इससे सिद्ध हुआ कि दुःख का मूल अशुभ कर्म है। वह जिस समय उदय होगा, उस समय इस जीव को कठिन से कठिन दुःखजन्य वेदना का अनुभव करना पड़ेगा और जब तक उस कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक लाख प्रकार के उपाय और प्रयत्न करने से भी उसकी शांति नहीं हो सकती। अतः दुःख की निवृत्ति और सुख की इच्छा रखने वाले प्राणी को सब से प्रथम दुःख के कारणभूत अशुभ कर्मों का समूलघात करने के लिए उद्यम करना चाहिए । इसके लिए प्रथम कर्मपरमाणुओं के आगमन के जो द्वार हैं—जिनको आश्रव कहते हैं, उनका निरोध करना होगा । उनके निरोधार्थ संवर भावना को अपनाने की आवश्यकता है। तदर्थ शान्त और दान्त होकर अनगारवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हे राजन् ! मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस वेदना से इस वार मुक्त हो जाऊँ तो मैं इस वेदना के मूल कारण का विनाश करने के लिए-जिससे कि फिर इस प्रकार की वेदना को सहन करने का अवसर ही प्राप्त न हो सके—प्रव्रजित हो जाऊँ अर्थात् वीतराग के निर्दिष्ट किये हुए संयममार्ग का अनुसरण करूँ, इत्यादि । पूर्व की गाथा में आया हुआ 'जे' शब्द पादपूर्ति के लिए है और उत्तर की गाथा में 'च' शब्द समुच्चयार्थक है । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के उत्पन्न होने पर मूर्ख-अज्ञानी और विचारशील पुरुषों के विचारों में बहुत अन्तर होता है । विचारशील पुरुष तो कष्ट के समय अपनी आत्मा को धैर्य और शान्ति प्रदान करने का यत्न करते हैं । अर्थात् उदय में आये