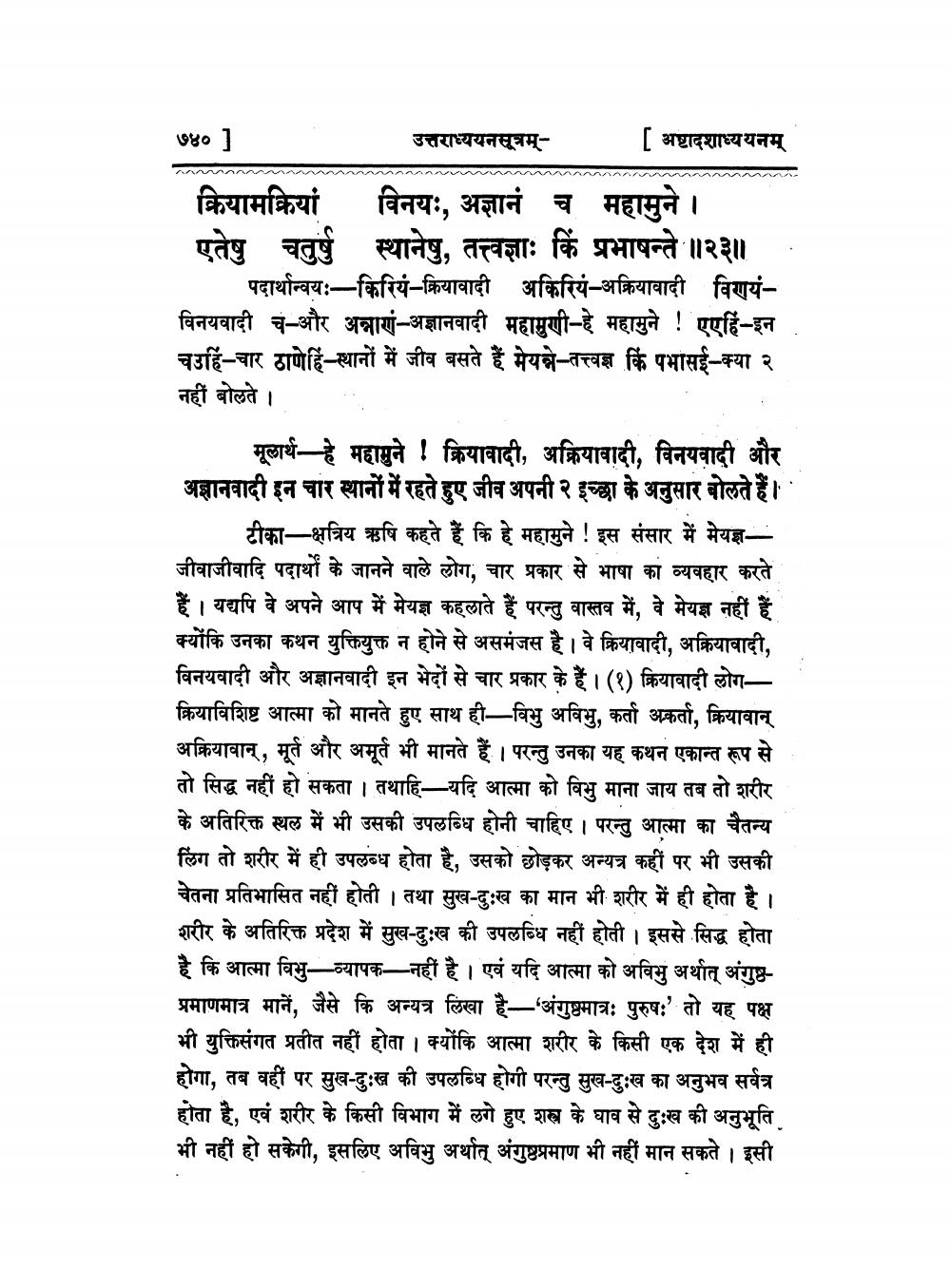________________
७४० ]
[ अष्टादशाध्ययनम्
उत्तराध्ययनसूत्रम् -
विनयः, अज्ञानं च महामुने । स्थानेषु, तत्त्वज्ञाः किं प्रभाषन्ते ॥२३॥
क्रियामक्रियां एतेषु चतुर्षु
पदार्थान्वयः —– किरियं - क्रियावादी विनयवादी च - और अन्नाणं - अज्ञानवादी चउहिं - चार ठाणेहिं - स्थानों में जीव बसते नहीं बोलते।
अकिरियं-अक्रियावादी विणयंमहामुखी - हे महामुने ! एएहिं इन मेयने - तत्त्वज्ञ किं पभासई - क्या २
हैं
मूलार्थ - हे महामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चार स्थानों में रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अनुसार बोलते हैं।
टीका - क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे महामुने ! इस संसार में मेयज्ञ - जीवाजीवादि पदार्थों के जानने वाले लोग, चार प्रकार से भाषा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते हैं परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं. क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमंजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन भेदों से चार प्रकार के हैं। (१) क्रियावादी लोगक्रियाविशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही — विभु अविभु, कर्ता अकर्ता, क्रियावान् अक्रियावान्, मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन एकान्त रूप से तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि - यदि आत्मा को विभु माना जाय तब तो शरीर के अतिरिक्त स्थल में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु आत्मा का चैतन्य लिंग तो शरीर में ही उपलब्ध होता है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी चेतना प्रतिभासित नहीं होती । तथा सुख-दुःख का मान भी शरीर में ही होता है । शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुख-दुःख की उपलब्धि नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा विभु — व्यापक — नहीं है । एवं यदि आत्मा को अविभु अर्थात् अंगुष्ठप्रमाणमात्र मानें, जैसे कि अन्यत्र लिखा है— 'अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ' तो यह पक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के किसी एक देश में ही होगा, तब वहीं पर सुख-दुःख की उपलब्धि होगी परन्तु सुख - दुःख का अनुभव सर्वत्र होता है, एवं शरीर के किसी विभाग में लगे हुए शस्त्र के घाव से दुःख की अनुभूति भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अविभु अर्थात् अंगुष्ठप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी