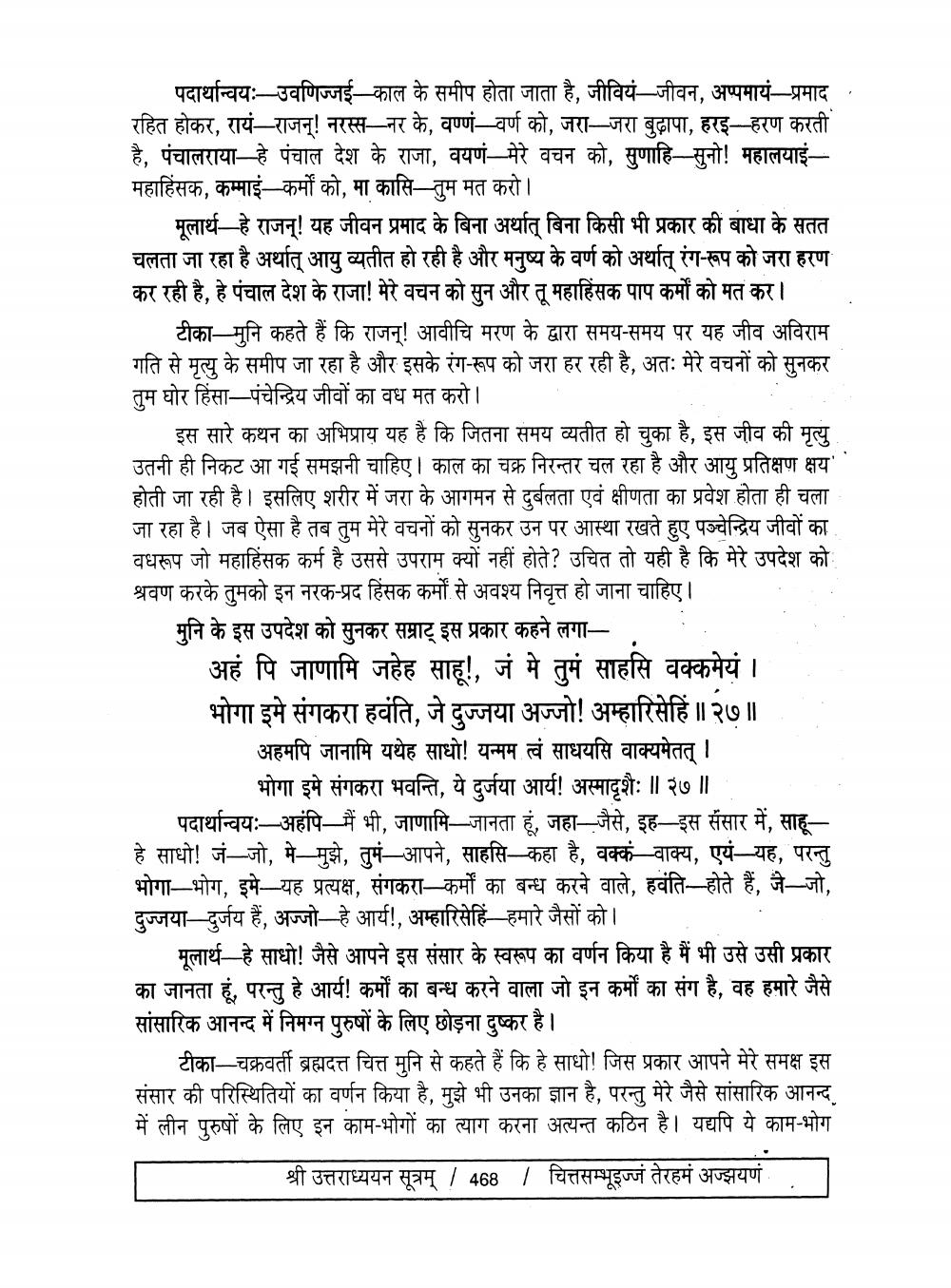________________
पदार्थान्वयः–उवणिज्जई—काल के समीप होता जाता है, जीवियं—जीवन, अप्पमायं—प्रमाद , रहित होकर, रायं–राजन्! नरस्स–नर के, वण्णं—वर्ण को, जरा-जरा बुढ़ापा, हरइ—हरण करती है, पंचालराया हे पंचाल देश के राजा, वयणं—मेरे वचन को, सुणाहि—सुनो! महालयाईमहाहिंसक, कम्माई–कर्मों को, मा कासि—तुम मत करो।
मूलार्थ हे राजन्! यह जीवन प्रमाद के बिना अर्थात् बिना किसी भी प्रकार की बाधा के सतत चलता जा रहा है अर्थात् आयु व्यतीत हो रही है और मनुष्य के वर्ण को अर्थात् रंग-रूप को जरा हरण कर रही है, हे पंचाल देश के राजा! मेरे वचन को सुन और तू महाहिंसक पाप कर्मों को मत कर।
टीका—मुनि कहते हैं कि राजन्! आवीचि मरण के द्वारा समय-समय पर यह जीव अविराम गति से मृत्यु के समीप जा रहा है और इसके रंग-रूप को जरा हर रही है, अतः मेरे वचनों को सुनकर तुम घोर हिंसा-पंचेन्द्रिय जीवों का वध मत करो।
इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि जितना समय व्यतीत हो चुका है. इस जीव की मत्य उतनी ही निकट आ गई समझनी चाहिए। काल का चक्र निरन्तर चल रहा है और आयु प्रतिक्षण क्षय' होती जा रही है। इसलिए शरीर में जरा के आगमन से दुर्बलता एवं क्षीणता का प्रवेश होता ही चला जा रहा है। जब ऐसा है तब तुम मेरे वचनों को सुनकर उन पर आस्था रखते हुए पञ्चेन्द्रिय जीवों का वधरूप जो महाहिंसक कर्म है उससे उपराम क्यों नहीं होते? उचित तो यही है कि मेरे उपदेश को श्रवण करके तुमको इन नरक-प्रद हिंसक कर्मों से अवश्य निवृत्त हो जाना चाहिए। मुनि के इस उपदेश को सुनकर सम्राट् इस प्रकार कहने लगा
अहं पि जाणामि जहेह साहू!, जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं । भोगा इमे संगकरा हवंति, जे दुज्जया अज्जो! अम्हारिसेहिं ॥२७॥
अहमपि जानामि यथेह साधो! यन्मम त्वं साधयसि वाक्यमेतत् ।
भोगा इमे संगकरा भवन्ति, ये दुर्जया आर्य! अस्मादृशैः ॥ २७ ॥ पदार्थान्वयः-अहंपि—मैं भी, जाणामि-जानता हूं, जहा—जैसे, इह—इस संसार में, साहूहे साधो! जं—जो, मे—मुझे, तुमं—आपने, साहसि—कहा है, वक्कं वाक्य, एयं—यह, परन्तु भोगा—भोग, इमे—यह प्रत्यक्ष, संगकरा—कर्मों का बन्ध करने वाले, हवंति–होते हैं, जे–जो, दुज्जया दुर्जय हैं, अज्जो—हे आर्य!, अम्हारिसेहिं—हमारे जैसों को। ___मूलार्थ हे साधो! जैसे आपने इस संसार के स्वरूप का वर्णन किया है मैं भी उसे उसी प्रकार का जानता हूं, परन्तु हे आर्य! कर्मों का बन्ध करने वाला जो इन कर्मों का संग है, वह हमारे जैसे सांसारिक आनन्द में निमग्न पुरुषों के लिए छोड़ना दुष्कर है।
टीका—चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चित्त मुनि से कहते हैं कि हे साधो! जिस प्रकार आपने मेरे समक्ष इस संसार की परिस्थितियों का वर्णन किया है, मुझे भी उनका ज्ञान है, परन्तु मेरे जैसे सांसारिक आनन्द में लीन पुरुषों के लिए इन काम-भोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि ये काम-भोग
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् / 468 / चित्तसम्भूइज्जं तेरहमं अज्झयणं ।