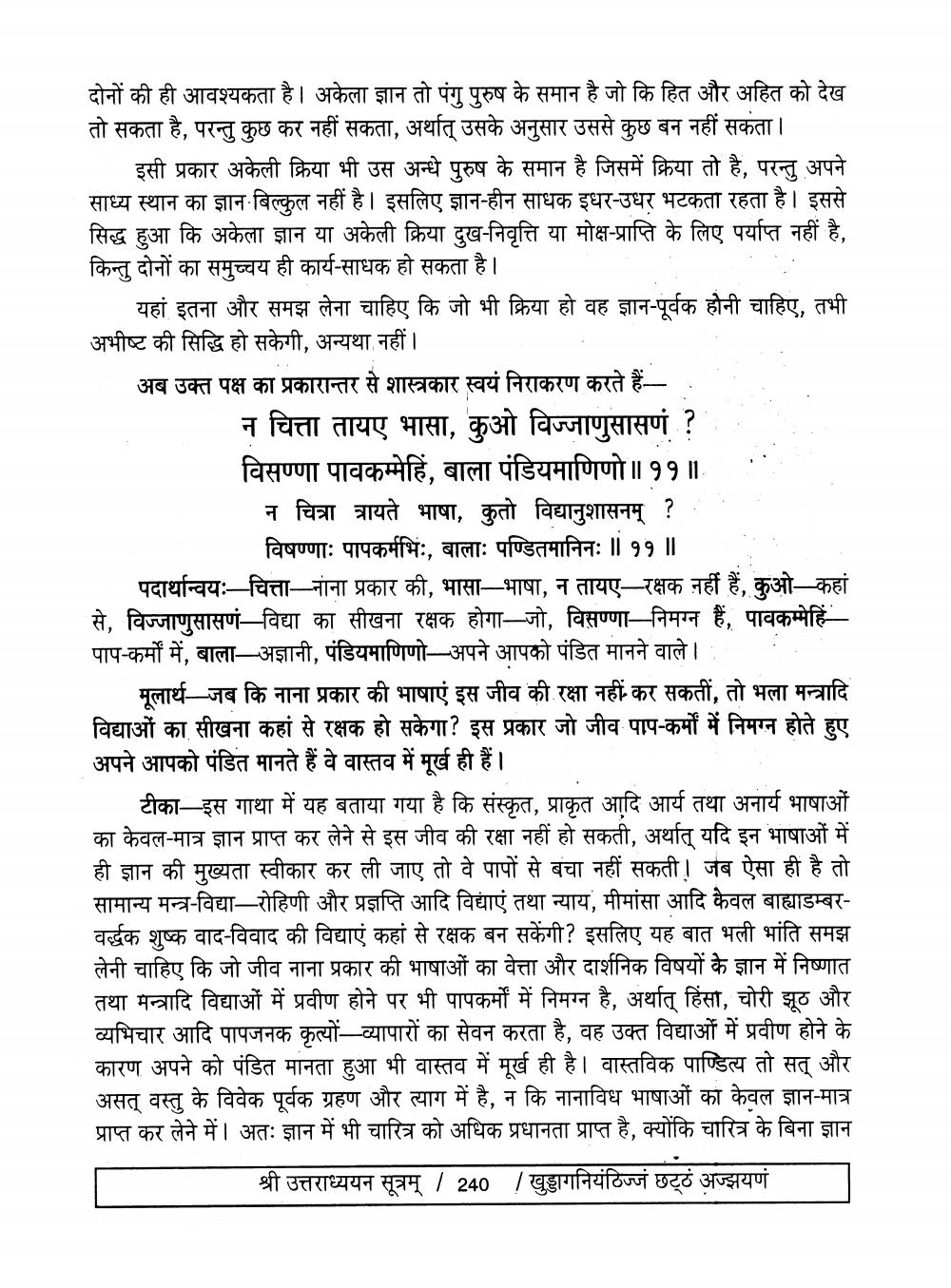________________
दोनों की ही आवश्यकता है। अकेला ज्ञान तो पंगु पुरुष के समान है जो कि हित और अहित को देख तो सकता है, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, अर्थात् उसके अनुसार उससे कुछ बन नहीं सकता ।
इसी प्रकार अकेली क्रिया भी उस अन्धे पुरुष के समान है जिसमें क्रिया तो हैं, परन्तु अपने साध्य स्थान का ज्ञान- बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज्ञान-हीन साधक इधर-उधर भटकता रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया दुख - निवृत्ति या मोक्ष - प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, किन्तु दोनों का समुच्चय ही कार्य साधक हो सकता है।
यहां इतना और समझ लेना चाहिए कि जो भी क्रिया हो वह ज्ञान- पूर्वक होनी चाहिए, तभी अभीष्ट की सिद्धि हो सकेगी, अन्यथा नहीं ।
अब उक्त पक्ष का प्रकारान्तर से शास्त्रकार स्वयं निराकरण करते हैं
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ? विसण्णा पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥ ११ ॥
न चित्रा त्रायते भाषा, कुतो विद्यानुशासनम् ? विषण्णाः पापकर्मभिः, बालाः पण्डितमानिनः || ११ ||
पदार्थान्वयः–चित्ता—नाना प्रकार की, भासा – भाषा, न तायए — रक्षक नहीं हैं, कुओ-कहां से, विज्जाणुसास - विद्या का सीखना रक्षक होगा - जो, विसण्णा — निमग्न हैं, पावकम्मेहिं— पाप कर्मों में, बाला - अज्ञानी, पंडियमाणिणो अपने आपको पंडित मानने वाले ।
मूलार्थ- जब कि नाना प्रकार की भाषाएं इस जीव की रक्षा नहीं कर सकतीं, तो भला मन्त्रादि विद्याओं का सीखना कहां से रक्षक हो सकेगा? इस प्रकार जो जीव पाप कर्मों में निमग्न होते हुए अपने आपको पंडित मानते हैं वे वास्तव में मूर्ख ही हैं ।
टीका - इस गाथा में यह बताया गया है कि संस्कृत, प्राकृत आदि आर्य तथा अनार्य भाषाओं का केवल मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेने से इस जीव की रक्षा नहीं हो सकती, अर्थात् यदि इन भाषाओं में ही ज्ञान की मुख्यता स्वीकार कर ली जाए तो वे पापों से बचा नहीं सकती। जब ऐसा ही है तो सामान्य मन्त्र - विद्या— रोहिणी और प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं तथा न्याय, मीमांसा आदि केवल बाह्याडम्बरवर्द्धक शुष्क वाद-विवाद की विद्याएं कहां से रक्षक बन सकेंगी? इसलिए यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि जो जीव नाना प्रकार की भाषाओं का वेत्ता और दार्शनिक विषयों के ज्ञान में निष्णात तथा मन्त्रादि विद्याओं में प्रवीण होने पर भी पापकर्मों निमग्न है, अर्थात् हिंसा, चोरी झूठ और व्यभिचार आदि पापजनक कृत्यों – व्यापारों का सेवन करता है, वह उक्त विद्याओं में प्रवीण होने के कारण अपने को पंडित मानता हुआ भी वास्तव में मूर्ख ही है । वास्तविक पाण्डित्य तो सत् और असत् वस्तु के विवेक पूर्वक ग्रहण और त्याग में है, न कि नानाविध भाषाओं का केवल ज्ञान - मात्र प्राप्त कर लेने में । अतः ज्ञान में भी चारित्र को अधिक प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि चारित्र के बिना ज्ञान
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् / 240
/ खुड्डागनियंठिज्जं छट्ठं अज्झयणं