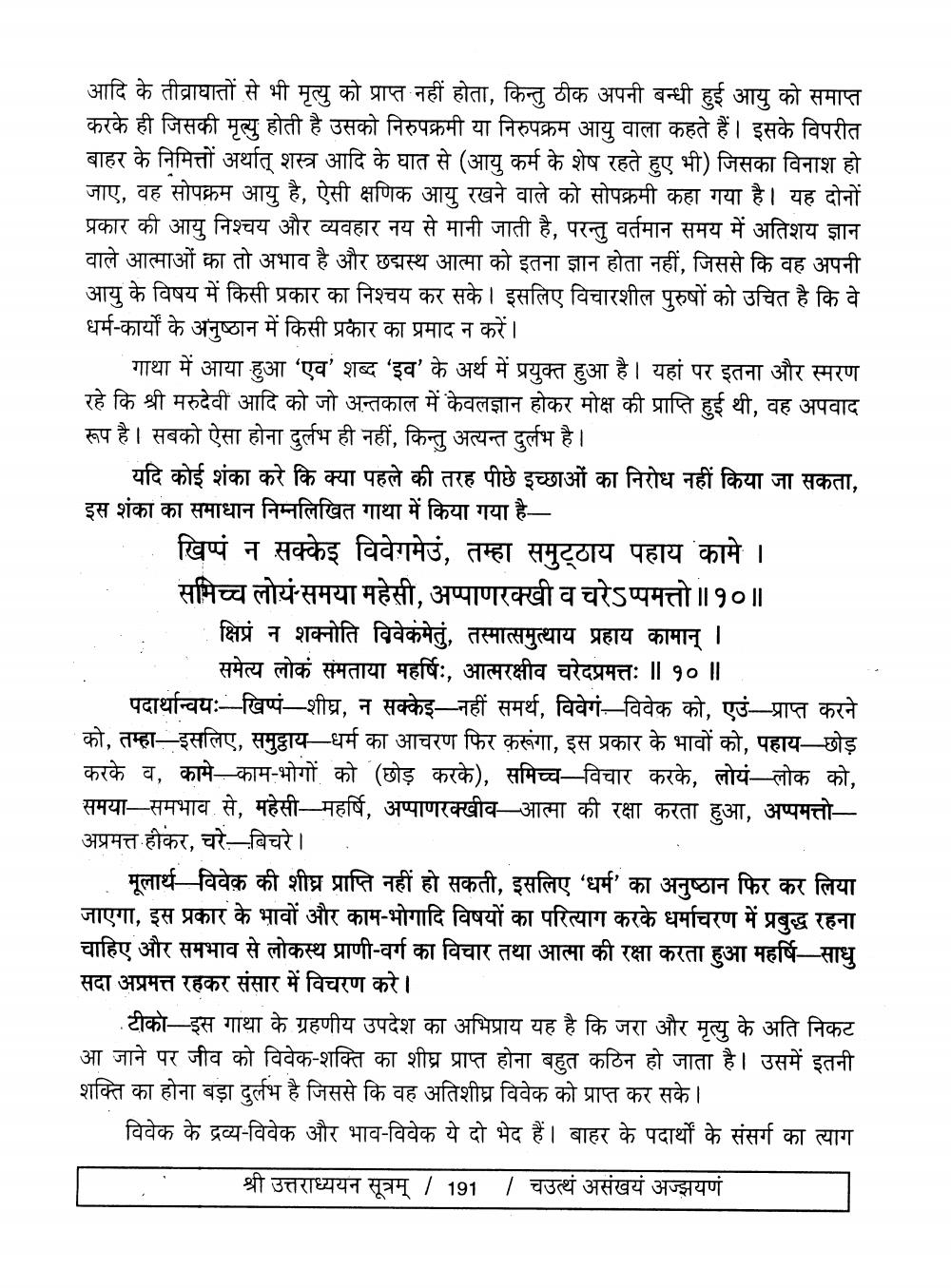________________
आदि के तीव्राघातों से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किन्तु ठीक अपनी बन्धी हुई आयु को समाप्त करके ही जिसकी मृत्यु होती है उसको निरुपक्रमी या निरुपक्रम आयु वाला कहते हैं। इसके विपरीत बाहर के निमित्तों अर्थात् शस्त्र आदि के घात से (आयु कर्म के शेष रहते हुए भी) जिसका विनाश हो जाए, वह सोपक्रम आयु है, ऐसी क्षणिक आयु रखने वाले को सोपक्रमी कहा गया है। यह दोनों प्रकार की आयु निश्चय और व्यवहार नय से मानी जाती है, परन्तु वर्तमान समय में अतिशय ज्ञान वाले आत्माओं का तो अभाव है और छद्मस्थ आत्मा को इतना ज्ञान होता नहीं, जिससे कि वह अपनी आयु के विषय में किसी प्रकार का निश्चय कर सके। इसलिए विचारशील पुरुषों को उचित है कि वे धर्म-कार्यों के अनुष्ठान में किसी प्रकार का प्रमाद न करें। ___गाथा में आया हुआ ‘एव' शब्द 'इव' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहां पर इतना और स्मरण रहे कि श्री मरुदेवी आदि को जो अन्तकाल में केवलज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वह अपवाद रूप है। सबको ऐसा होना दुर्लभ ही नहीं, किन्तु अत्यन्त दुर्लभ है।
यदि कोई शंका करे कि क्या पहले की तरह पीछे इच्छाओं का निरोध नहीं किया जा सकता, इस शंका का समाधान निम्नलिखित गाथा में किया गया है
खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं, तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे | समिच्च लोयं-समया महेसी, अप्पाणरक्खी व चरेऽप्पमत्तो॥१०॥ - क्षिप्रं न शक्नोति विवेकमेतुं, तस्मात्समुत्थाय प्रहाय कामान् ।
समेत्य लोकं समताया महर्षिः, आत्मरक्षीव चरेदप्रमत्तः ॥ १० ॥ पदार्थान्वयः खिप्पं—शीघ्र, न सक्केइ–नहीं समर्थ, विवेगं—विवेक को, एउं—प्राप्त करने को, तम्हा—इसलिए, समुट्ठाय धर्म का आचरण फिर करूंगा, इस प्रकार के भावों को, पहाय—छोड़ करके व, कामे-काम-भोगों को (छोड़ करके), समिच्च-विचार करके, लोयं—लोक को, समया—समभाव से, महेसी—महर्षि, अप्पाणरक्खीव आत्मा की रक्षा करता हुआ, अप्पमत्तोअप्रमत्त हीकर, चरे–बिचरे। .
मूलार्थ विवेक की शीघ्र प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए 'धर्म' का अनुष्ठान फिर कर लिया जाएगा, इस प्रकार के भावों और काम-भोगादि विषयों का परित्याग करके धर्माचरण में प्रबुद्ध रहना चाहिए और समभाव से लोकस्थ प्राणी-वर्ग का विचार तथा आत्मा की रक्षा करता हुआ महर्षि–साधु सदा अप्रमत्त रहकर संसार में विचरण करे ।
टीको—इस गाथा के ग्रहणीय उपदेश का अभिप्राय यह है कि जरा और मृत्यु के अति निकट आ जाने पर जीव को विवेक-शक्ति का शीघ्र प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति का होना बड़ा दुर्लभ है जिससे कि वह अतिशीघ्र विवेक को प्राप्त कर सके।
विवेक के द्रव्य-विवेक और भाव-विवेक ये दो भेद हैं। बाहर के पदार्थों के संसर्ग का त्याग । श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् | 191 / चउत्थं असंखयं अज्झयणं
।