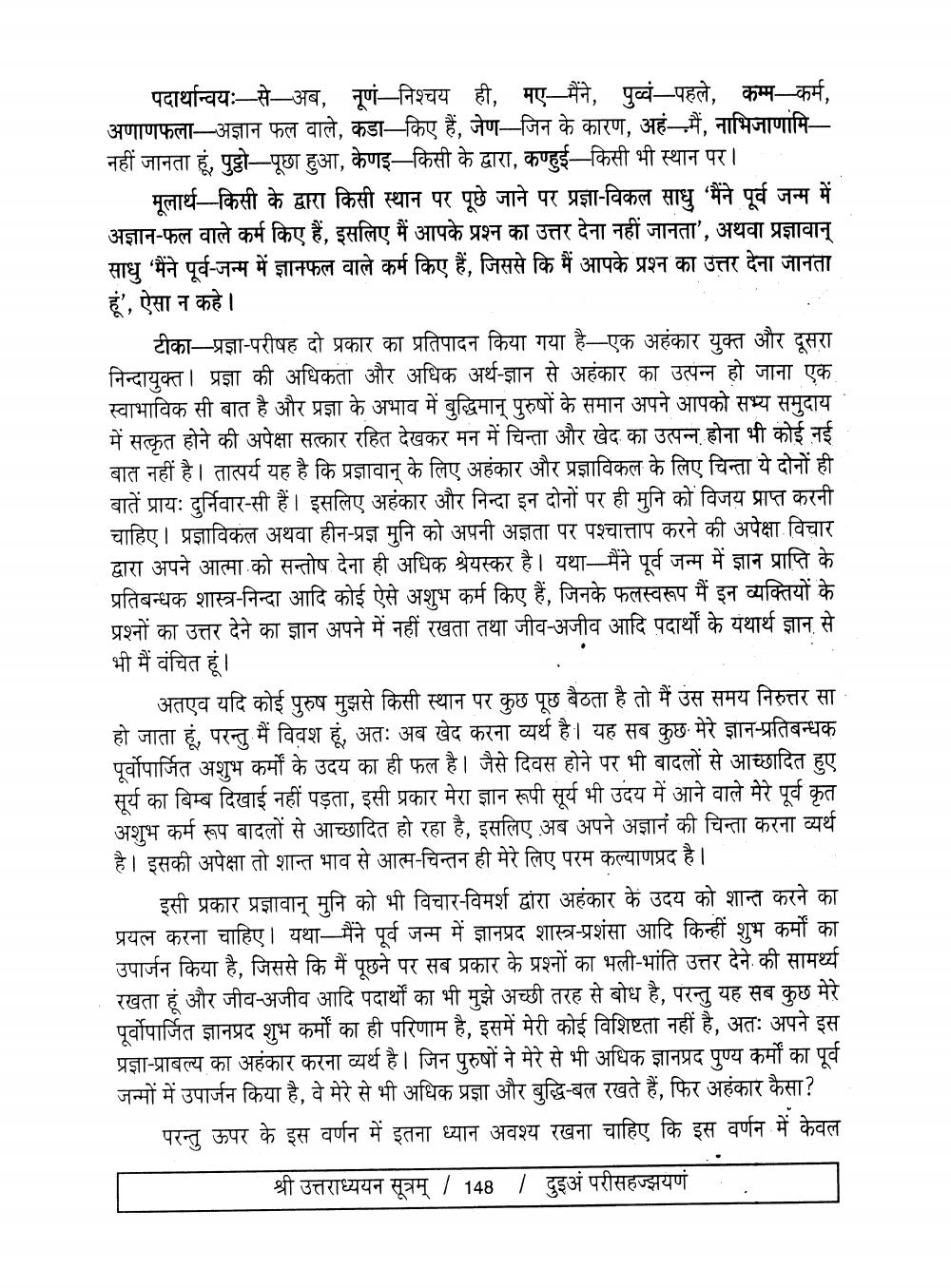________________
पदार्थान्वयः – से—– अब, नूणं निश्चय ही, मए मैंने, पुव्वं – पहले, कम्म—–कर्म, अणाणफला—अज्ञान फल वाले, कडा – किए हैं, जेण - जिन के कारण, अहं मैं, नाभिजाणामि— नहीं जानता हूं, पुट्ठो – पूछा हुआ, केणइ – किसी के द्वारा, कण्हुई— किसी भी स्थान पर ।
मूलार्थ - किसी के द्वारा किसी स्थान पर पूछे जाने पर प्रज्ञा - विकल साधु 'मैंने पूर्व जन्म में अज्ञान-फल वाले कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं जानता', अथवा प्रज्ञावान् साधु 'मैंने पूर्व जन्म में ज्ञानफल वाले कर्म किए हैं, जिससे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना जानता हूं', ऐसा न कहे ।
टीका – प्रज्ञा - परीषह दो प्रकार का प्रतिपादन किया गया है— एक अहंकार युक्त और दूसरा निन्दायुक्त । प्रज्ञा की अधिकता और अधिक अर्थ-ज्ञान से अहंकार का उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है और प्रज्ञा के अभाव में बुद्धिमान् पुरुषों के समान अपने आपको सभ्य समुदाय में • सत्कृत होने की अपेक्षा सत्कार रहित देखकर मन में चिन्ता और खेद का उत्पन्न होना भी कोई नई बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रज्ञावान् के लिए अहंकार और प्रज्ञाविकल के लिए चिन्ता ये दोनों ही बातें प्रायः दुर्निवार-सी हैं। इसलिए अहंकार और निन्दा इन दोनों पर ही मुनि को विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रज्ञाविकल अथवा हीन - प्रज्ञ मुनि को अपनी अज्ञता पर पश्चात्ताप करने की अपेक्षा विचार द्वारा अपने आत्मा को सन्तोष देना ही अधिक श्रेयस्कर है । यथा— मैंने पूर्व जन्म में ज्ञान प्राप्ति के प्रतिबन्धक शास्त्र-निन्दा आदि कोई ऐसे अशुभ कर्म किए हैं, जिनके फलस्वरूप मैं इन व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देने का ज्ञान अपने में नहीं रखता तथा जीव - अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से भी मैं वंचित हूं।
अतएव यदि कोई पुरुष मुझसे किसी स्थान पर कुछ पूछ बैठता है तो मैं उस समय निरुत्तर सा हो जाता हूं, परन्तु मैं विवश हूं, अतः अब खेद करना व्यर्थ है । यह सब कुछ मेरे ज्ञान प्रतिबन्धक पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों के उदय का ही फल है। जैसे दिवस होने पर भी बादलों से आच्छादित हुए सूर्य का बिम्ब दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार मेरा ज्ञान रूपी सूर्य भी उदय में आने वाले मेरे पूर्व कृत अशुभ कर्म रूप बादलों से आच्छादित हो रहा है, इसलिए अब अपने अज्ञानं की चिन्ता करना व्यर्थ है । इसकी अपेक्षा तो शान्त भाव से आत्म-चिन्तन ही मेरे लिए परम कल्याणप्रद है ।
इसी प्रकार प्रज्ञावान् मुनि को भी विचार-विमर्श द्वारा अहंकार के उदय को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यथा— मैंने पूर्व जन्म में ज्ञानप्रद शास्त्र - प्रशंसा आदि किन्हीं शुभ कर्मों का उपार्जन किया है, जिससे कि मैं पूछने पर सब प्रकार के प्रश्नों का भली-भांति उत्तर देने की सामर्थ्य रखता हूं और जीव-अजीव आदि पदार्थों का भी मुझे अच्छी तरह से बोध है, परन्तु यह सब कुछ मेरे पूर्वोपार्जित ज्ञानप्रद शुभ कर्मों का ही परिणाम है, इसमें मेरी कोई विशिष्टता नहीं है, अतः अपने इस प्रज्ञा-प्राबल्य का अहंकार करना व्यर्थ है । जिन पुरुषों ने मेरे से भी अधिक ज्ञानप्रद पुण्य कर्मों का पूर्व जन्मों में उपार्जन किया है, वे मेरे से भी अधिक प्रज्ञा और बुद्धि-बल रखते हैं, फिर अहंकार कैसा ?
परन्तु ऊपर के इस वर्णन में इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस वर्णन में केवल श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् / 148 / दुइअं परीसहज्झयणं