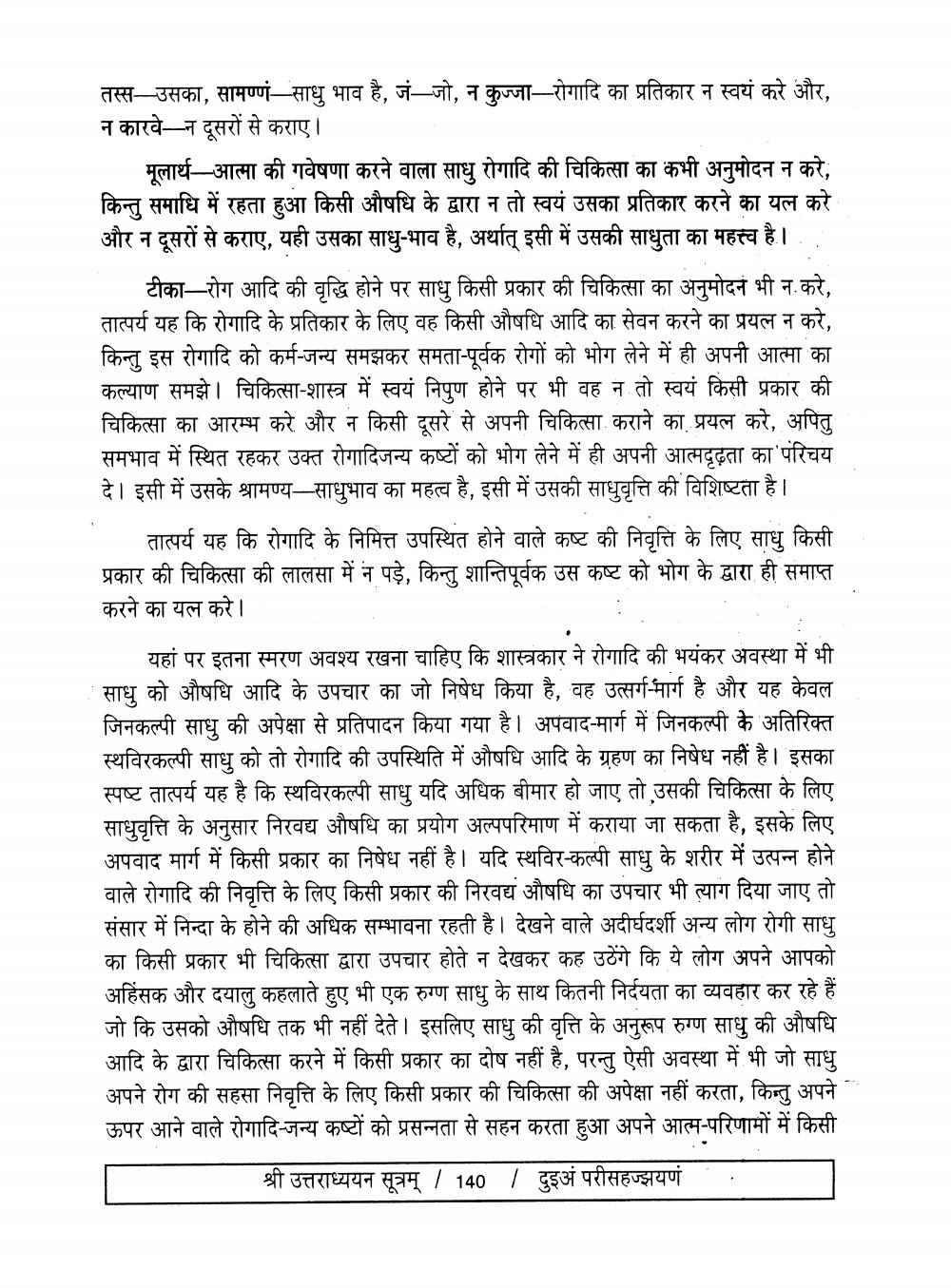________________
तस्स — उसका, सामण्णं साधु भाव है, जं- जो, न कुज्जा - रोगादि का प्रतिकार न स्वयं करे और, न कारवे- न दूसरों से कराए।
मूलार्थ – अ — आत्मा की गवेषणा करने वाला साधु रोगादि की चिकित्सा का कभी अनुमोदन न करे, किन्तु समाधि में रहता हुआ किसी औषधि के द्वारा न तो स्वयं उसका प्रतिकार करने का यत्न करे और न दूसरों से कराए, यही उसका साधु-भाव है, अर्थात् इसी में उसकी साधुता का महत्त्व है।
टीका — रोग आदि की वृद्धि होने पर साधु किसी प्रकार की चिकित्सा का अनुमोदन भी न करे, तात्पर्य यह कि रोगादि के प्रतिकार के लिए वह किसी औषधि आदि का सेवन करने का प्रयत्न न करे, किन्तु इस रोगादि को कर्म-जन्य समझकर समता - पूर्वक रोगों को भोग लेने में ही अपनी आत्मा का कल्याण समझे । चिकित्सा - शास्त्र में स्वयं निपुण होने पर भी वह न तो स्वयं किसी प्रकार की चिकित्सा का आरम्भ करे और न किसी दूसरे से अपनी चिकित्सा कराने का प्रयत्न करे, अपितु समभाव में स्थित रहकर उक्त रोगादिजन्य कष्टों को भोग लेने में ही अपनी आत्मदृढ़ता का परिचय दे। इसी में उसके श्रामण्य - साधुभाव का महत्व है, इसी में उसकी साधुवृत्ति की विशिष्टता है ।
तात्पर्य यह कि रोगादि के निमित्त उपस्थित होने वाले कष्ट की निवृत्ति के लिए साधु किसी प्रकार की चिकित्सा की लालसा में न पड़े, किन्तु शान्तिपूर्वक उस कष्ट को भोग के द्वारा ही समाप्त करने का यत्न करे ।
यहां पर इतना स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि शास्त्रकार ने रोगादि की भयंकर अवस्था में भी साधु को औषधि आदि के उपचार का जो निषेध किया है, वह उत्सर्ग-मार्ग है और यह केवल जिनकल्पी साधु की अपेक्षा से प्रतिपादन किया गया है। अपवाद-मार्ग में जिनकल्पी के अतिरिक्त स्थविरकल्पी साधु को तो रोगादि की उपस्थिति में औषधि आदि के ग्रहण का निषेध नहीं है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि स्थविरकल्पी साधु यदि अधिक बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए साधुवृत्ति के अनुसार निरवद्य औषधि का प्रयोग अल्पपरिमाण में कराया जा सकता है, इसके लिए अपवाद मार्ग में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। यदि स्थविर - कल्पी साधु के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगादि की निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की निरवद्यं औषधि का उपचार भी त्याग दिया जाए तो संसार में निन्दा के होने की अधिक सम्भावना रहती है। देखने वाले अदीर्घदर्शी अन्य लोग रोगी साधु का किसी प्रकार भी चिकित्सा द्वारा उपचार होते न देखकर कह उठेंगे कि ये लोग अपने आपको अहिंसक और दयालु कहलाते हुए भी एक रुग्ण साधु के साथ कितनी निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं जो कि उसको औषधि तक भी नहीं देते। इसलिए साधु की वृत्ति के अनुरूप रुग्ण साधु की आदि के द्वारा चिकित्सा करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है, परन्तु ऐसी अवस्था में भी जो साधु अपने रोग की सहसा निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की चिकित्सा की अपेक्षा नहीं करता, किन्तु अपने ऊपर आने वाले रोगादि-जन्य कष्टों को प्रसन्नता से सहन करता हुआ अपने आत्म-परिणामों में किसी
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् / 140 / दुइअं परीसहज्झयणं