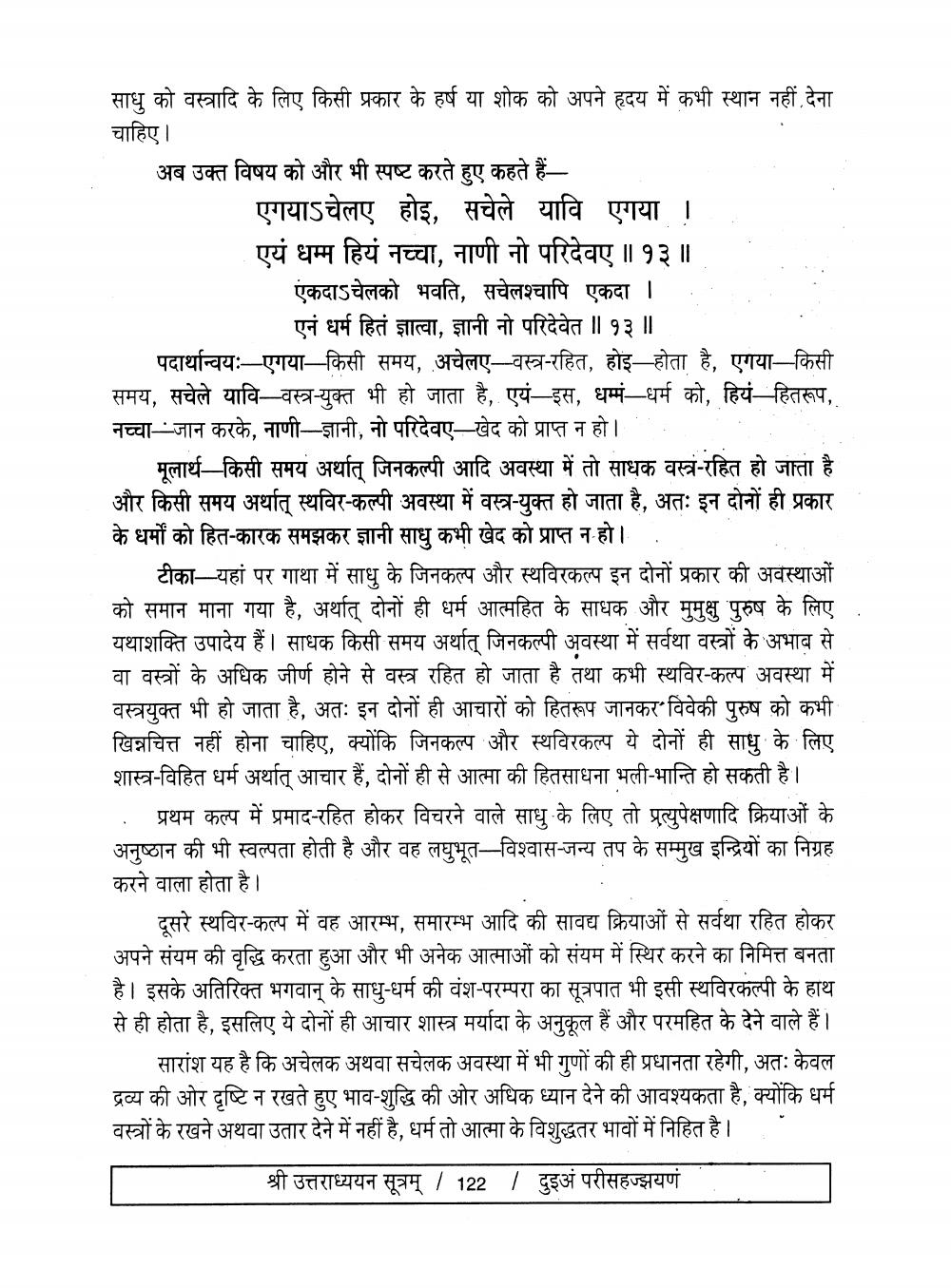________________
साधु को वस्त्रादि के लिए किसी प्रकार के हर्ष या शोक को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं देना चाहिए।
अब उक्त विषय को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं—
एगयाऽचेलए होइ, सचेले यावि एगया ! एयं धम्म हियं नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥ १३ ॥ एकदाऽचेलको भवति, सचेलश्चापि एकदा | एनं धर्म हितं ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत ॥ १३ ॥
पदार्थान्वयः–एगया—किसी समय, अचेलए - वस्त्र -रहित, होंइ — होता है, एगया – किसी समय, सचेले यावि-वस्त्र-युक्त भी हो जाता है, एवं इस, धम्मं-धर्म को, हियं – हितरूप, नच्चा -- जान करके, नाणी – ज्ञानी, नो परिदेवए - खेद को प्राप्त न हो ।
मूलार्थ - किसी समय अर्थात् जिनकल्पी आदि अवस्था में तो साधक वस्त्र-रहित हो जाता है और किसी समय अर्थात् स्थविर - कल्पी अवस्था में वस्त्र - युक्त हो जाता है, अतः इन दोनों ही प्रकार के धर्मों को हित-कारक समझकर ज्ञानी साधु कभी खेद को प्राप्त न हो ।
टीका - यहां पर गाथा में साधु के जिनकल्प और स्थविरकल्प इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं को समान माना गया है, अर्थात् दोनों ही धर्म आत्महित के साधक और मुमुक्षु पुरुष के लिए यथाशक्ति उपादेय हैं। साधक किसी समय अर्थात् जिनकल्पी अवस्था में सर्वथा वस्त्रों के अभाव से वा वस्त्रों के अधिक जीर्ण होने से वस्त्र रहित हो जाता है तथा कभी स्थविर-कल्प अवस्था में वस्त्रयुक्त भी हो जाता है, अतः इन दोनों ही आचारों को हितरूप जानकर विवेकी पुरुष को कभी खिन्नचित्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकल्प और स्थविरकल्प ये दोनों ही साधु के लिए शास्त्र-विहित धर्म अर्थात् आचार हैं, दोनों ही से आत्मा की हितसाधना भली- भान्ति हो सकती है ।
प्रथम कल्प में प्रमाद-रहित होकर विचरने वाले साधु के लिए तो प्रत्युपेक्षणादि क्रियाओं के अनुष्ठान की भी स्वल्पता होती है और वह लघुभूत - विश्वास जन्य तप के सम्मुख इन्द्रियों का निग्रह करने वाला होता है ।
दूसरे स्थविर - कल्प में वह आरम्भ, समारम्भ आदि की सावद्य क्रियाओं से सर्वथा रहित होकर अपने संयम की वृद्धि करता हुआ और भी अनेक आत्माओं को संयम में स्थिर करने का निमित्त बनता है। इसके अतिरिक्त भगवान् के साधु-धर्म की वंश-परम्परा का सूत्रपात भी इसी स्थविरकल्प से ही होता है, इसलिए ये दोनों ही आचार शास्त्र मर्यादा के अनुकूल हैं और परमहित के देने वाले हैं।
सारांश यह है कि अचेलक अथवा सचेलक अवस्था में भी गुणों की ही प्रधानता रहेगी, अतः केवल द्रव्य की ओर दृष्टि न रखते हुए भाव -शुद्धि की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म वस्त्रों के रखने अथवा उतार देने में नहीं है, धर्म तो आत्मा के विशुद्धतर भावों में निहित है ।
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् / 122 / दुइअं परीसहज्झयणं