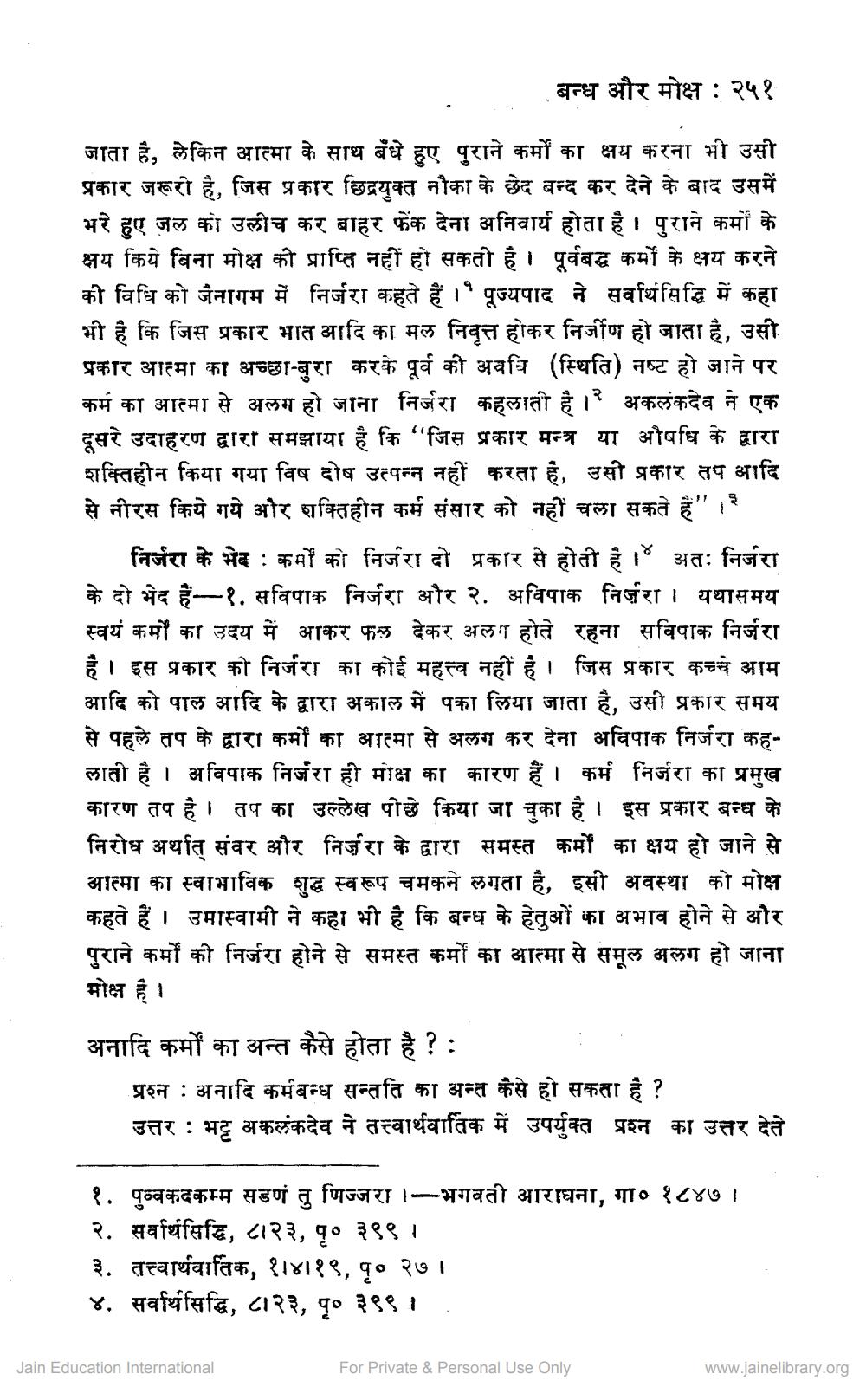________________
बन्ध और मोक्ष : २५१
जाता है, लेकिन आत्मा के साथ बँधे हुए पुराने कर्मों का क्षय करना भी उसी प्रकार जरूरी है, जिस प्रकार छिद्रयुक्त नौका के छेद बन्द कर देने के बाद उसमें भरे हुए जल को उलीच कर बाहर फेंक देना अनिवार्य होता है। पुराने कर्मों के क्षय किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूर्वबद्ध कर्मों के क्षय करने की विधि को जैनागम में निर्जरा कहते हैं । पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा भी है कि जिस प्रकार भात आदि का मल निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का अच्छा-बुरा करके पूर्व की अवधि (स्थिति) नष्ट हो जाने पर कर्म का आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा कहलाती है।२ अकलंकदेव ने एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझाया है कि "जिस प्रकार मन्त्र या औषधि के द्वारा शक्तिहीन किया गया विष दोष उत्पन्न नहीं करता है, उसी प्रकार तप आदि से नीरस किये गये और शक्तिहीन कर्म संसार को नहीं चला सकते हैं" ।
निर्जरा के भेद : कर्मों को निर्जरा दो प्रकार से होती है। अतः निर्जरा के दो भेद हैं-१. सविपाक निर्जरा और २. अविपाक निर्जरा । यथासमय स्वयं कर्मों का उदय में आकर फल देकर अलग होते रहना सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार को निर्जरा का कोई महत्त्व नहीं है। जिस प्रकार कच्चे आम आदि को पाल आदि के द्वारा अकाल में पका लिया जाता है, उसी प्रकार समय से पहले तप के द्वारा कर्मों का आत्मा से अलग कर देना अविपाक निर्जरा कहलाती है । अविपाक निर्जरा ही मोक्ष का कारण हैं। कर्म निर्जरा का प्रमुख कारण तप है। तप का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इस प्रकार बन्ध के निरोध अर्थात् संवर और निर्जरा के द्वारा समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप चमकने लगता है, इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं । उमास्वामी ने कहा भी है कि बन्ध के हेतुओं का अभाव होने से और पुराने कर्मों की निर्जरा होने से समस्त कर्मों का आत्मा से समूल अलग हो जाना मोक्ष है।
अनादि कर्मों का अन्त कैसे होता है ? :
प्रश्न : अनादि कर्मबन्ध सन्तति का अन्त कैसे हो सकता है ? उत्तर : भट्ट अकलंकदेव ने तत्त्वार्थवार्तिक में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते
१. पुवकदकम्म सडणं तु णिज्जरा ।-भगवती आराधना, गा० १८४७ । २. सर्वार्थसिद्धि, ८।२३, पृ० ३९९ । ३. तत्त्वार्थवार्तिक, १।४।१९, पृ० २७ । ४. सर्वार्थसिद्धि, ८।२३, पृ० ३९९ ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org