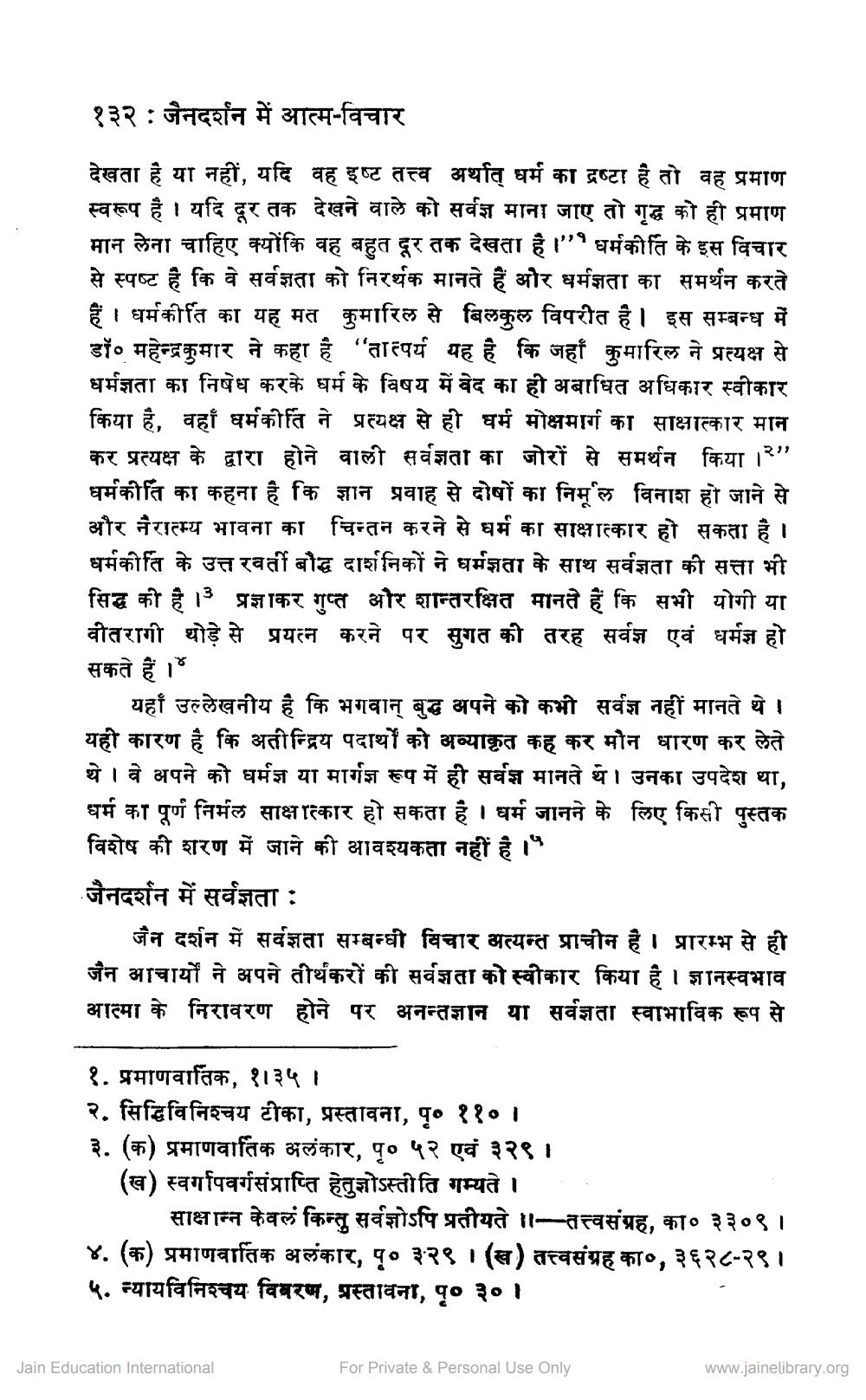________________
१३२ : जैनदर्शन में आत्म- विचार
देखता है या नहीं, यदि वह इष्ट तत्त्व अर्थात् धर्म का द्रष्टा है तो वह प्रमाण स्वरूप है । यदि दूर तक देखने वाले को सर्वज्ञ माना जाए तो गृद्ध को ही प्रमाण मान लेना चाहिए क्योंकि वह बहुत दूर तक देखता है ।"" धर्मकीर्ति के इस विचार से स्पष्ट है कि वे सर्वज्ञता को निरर्थक मानते हैं और धर्मज्ञता का समर्थन करते हैं । धर्मकीर्ति का यह मत कुमारिल से बिलकुल विपरीत है । इस सम्बन्ध में डॉ० महेन्द्रकुमार ने कहा है "तात्पर्य यह है कि जहाँ कुमारिल ने प्रत्यक्ष से धर्मज्ञता का निषेध करके धर्म के विषय में वेद का ही अबाधित अधिकार स्वीकार किया है, वहाँ धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष से ही धर्म मोक्षमार्ग का साक्षात्कार मान कर प्रत्यक्ष के द्वारा होने वाली सर्वज्ञता का जोरों से समर्थन किया । २" धर्म का कहना है कि ज्ञान प्रवाह से दोषों का निर्मूल विनाश हो जाने से और नैरात्म्य भावना का चिन्तन करने से धर्म का साक्षात्कार हो सकता है । धर्मकीर्ति के उत्तरवर्ती बौद्ध दार्शनिकों ने धर्मज्ञता के साथ सर्वज्ञता की सत्ता भी सिद्ध की है । 3 प्रज्ञाकर गुप्त और शान्तरक्षित मानते हैं कि सभी योगी या वीतरागी थोड़े से प्रयत्न करने पर सुगत की तरह सर्वज्ञ एवं धर्मज्ञ हो सकते हैं ।
४
यहाँ उल्लेखनीय है कि भगवान् बुद्ध अपने को कभी सर्वज्ञ नहीं मानते थे । यही कारण है कि अतीन्द्रिय पदार्थों को अव्याकृत कह कर मौन धारण कर लेते थे । वे अपने को धर्मज्ञ या मार्गज्ञ रूप में ही सर्वज्ञ मानते थे । उनका उपदेश था, धर्म का पूर्ण निर्मल साक्षात्कार हो सकता है । धर्म जानने के लिए किसी पुस्तक विशेष की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है ।
I
जैनदर्शन में सर्वज्ञता :
जैन दर्शन में सर्वज्ञता सम्बन्धी विचार अत्यन्त प्राचीन है । प्रारम्भ से ही जैन आचार्यों ने अपने तीर्थंकरों की सर्वज्ञता को स्वीकार किया है । ज्ञानस्वभाव आत्मा के निरावरण होने पर अनन्तज्ञान या सर्वज्ञता स्वाभाविक रूप से
१. प्रमाणवार्तिक १।३५ ।
२. सिद्धिविनिश्चय टीका, प्रस्तावना, पृ० ११० ।
३. ( क ) प्रमाणवार्तिक अलंकार, पृ० ५२ एवं ३२९ ।
(ख) स्वर्गापवर्गसंप्राप्ति हेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते ।
साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ॥ - तत्त्वसंग्रह, का० ३३०९ । ४. ( क ) प्रमाणवार्तिक अलंकार, पृ० ३२९ । (ख) तत्त्वसंग्रह का०, ३६२८-२९ । ५. न्यायविनिश्चय विवरण, प्रस्तावना, पृ० ३० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org