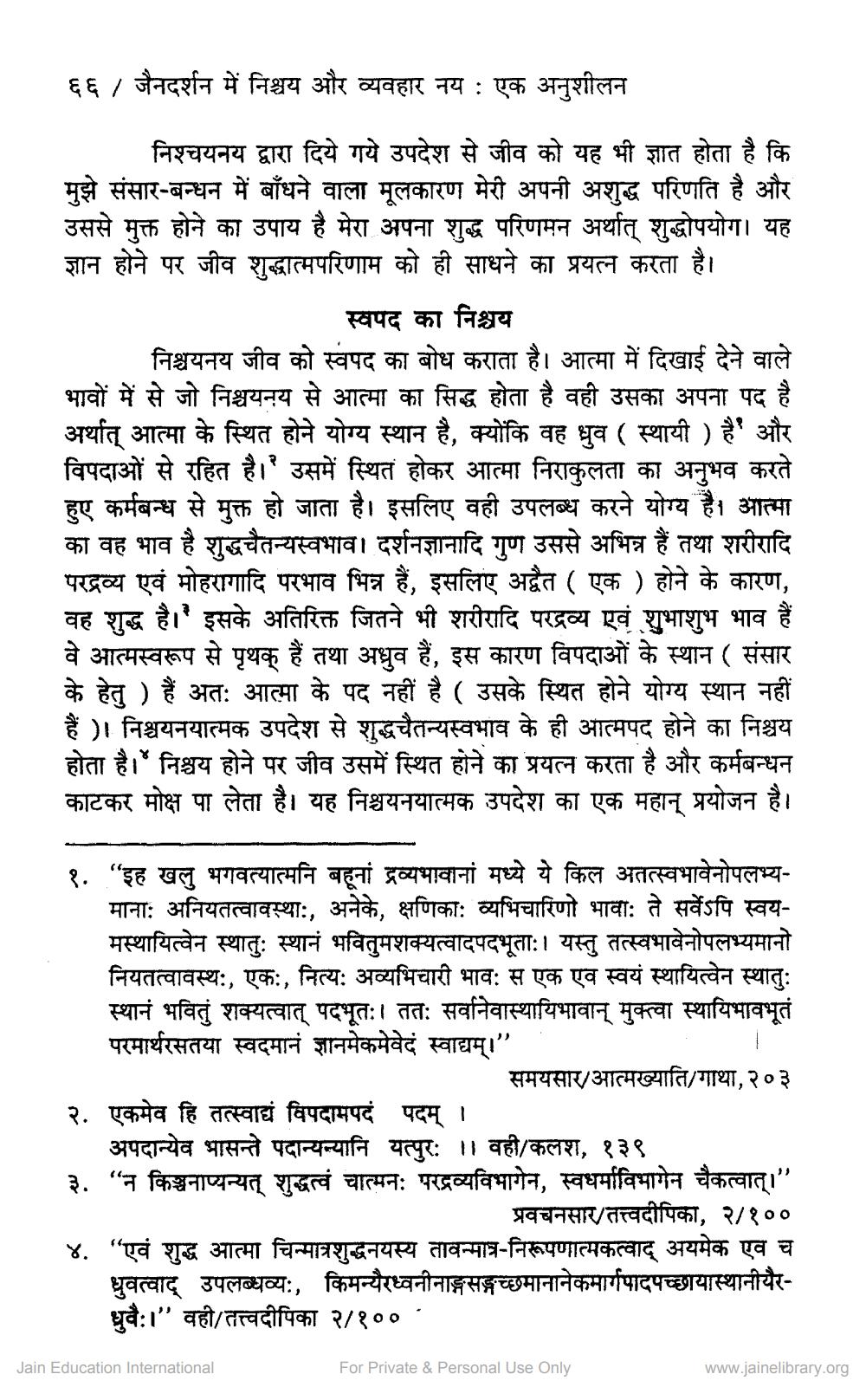________________
६६ / जैनदर्शन में निश्चय और व्यवहार नय : एक अनुशीलन
निश्चयनय द्वारा दिये गये उपदेश से जीव को यह भी ज्ञात होता है कि मुझे संसार-बन्धन में बाँधने वाला मूलकारण मेरी अपनी अशुद्ध परिणति है और उससे मुक्त होने का उपाय है मेरा अपना शुद्ध परिणमन अर्थात् शुद्धोपयोग। यह ज्ञान होने पर जीव शुद्धात्मपरिणाम को ही साधने का प्रयत्न करता है।
स्वपद का निश्चय निश्चयनय जीव को स्वपद का बोध कराता है। आत्मा में दिखाई देने वाले भावों में से जो निश्चयनय से आत्मा का सिद्ध होता है वही उसका अपना पद है अर्थात आत्मा के स्थित होने योग्य स्थान है, क्योंकि वह ध्रुव ( स्थायी ) है और विपदाओं से रहित है। उसमें स्थित होकर आत्मा निराकुलता का अनुभव करते हुए कर्मबन्ध से मुक्त हो जाता है। इसलिए वही उपलब्ध करने योग्य है। आत्मा का वह भाव है शुद्धचैतन्यस्वभाव। दर्शनज्ञानादि गुण उससे अभिन्न हैं तथा शरीरादि परद्रव्य एवं मोहरागादि परभाव भिन्न हैं, इसलिए अद्वैत ( एक ) होने के कारण, वह शुद्ध है। इसके अतिरिक्त जितने भी शरीरादि परद्रव्य एवं शुभाशुभ भाव हैं वे आत्मस्वरूप से पृथक् हैं तथा अध्रुव हैं, इस कारण विपदाओं के स्थान ( संसार के हेतु ) हैं अत: आत्मा के पद नहीं है ( उसके स्थित होने योग्य स्थान नहीं हैं )। निश्चयनयात्मक उपदेश से शुद्धचैतन्यस्वभाव के ही आत्मपद होने का निश्चय होता है। निश्चय होने पर जीव उसमें स्थित होने का प्रयत्न करता है और कर्मबन्धन काटकर मोक्ष पा लेता है। यह निश्चयनयात्मक उपदेश का एक महान् प्रयोजन है।
१. "इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्वभावेनोपलभ्य
माना: अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिका: व्यभिचारिणो भावा: ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वादपदभूताः। यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानो नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः अव्यभिचारी भावः स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः। तत: सर्वानेवास्थायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यम्।"
समयसार/आत्मख्याति/गाथा, २०३ २. एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ।। वही/कलश, १३९ ३. “न किञ्चनाप्यन्यत् शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन, स्वधर्माविभागेन चैकत्वात्।"
प्रवचनसार/तत्त्वदीपिका, २/१०० ४. “एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्र-निरूपणात्मकत्वाद् अयमेक एव च
ध्रुवत्वाद् उपलब्धव्यः, किमन्यैरध्वनीनाङ्गसङ्गच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानीयैरध्रुवैः।" वही/तत्त्वदीपिका २/१०० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org