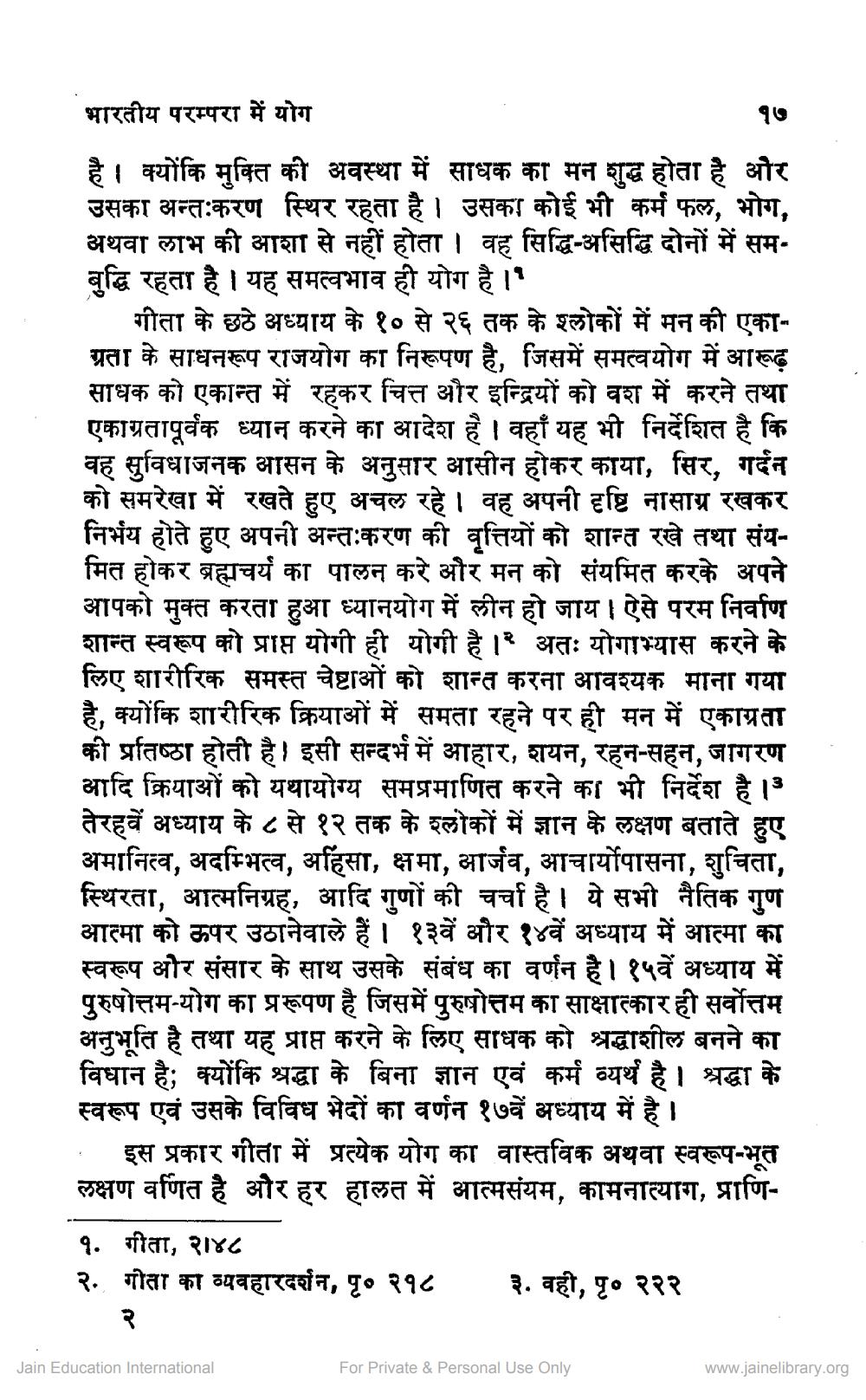________________
भारतीय परम्परा में योग
१७
है । क्योंकि मुक्ति की अवस्था में साधक का मन शुद्ध होता है और उसका अन्तःकरण स्थिर रहता है । उसका कोई भी कर्म फल, भोग, अथवा लाभ की आशा से नहीं होता । वह सिद्धि-असिद्धि दोनों में समबुद्धि रहता है । यह समत्वभाव ही योग है । "
गीता के छठे अध्याय के १० से २६ तक के श्लोकों में मन की एकाग्रता के साधनरूप राजयोग का निरूपण है, जिसमें समत्वयोग में आरूढ़ साधक को एकान्त में रहकर चित्त और इन्द्रियों को वश में करने तथा एकाग्रतापूर्वक ध्यान करने का आदेश है । वहाँ यह भी निर्देशित है कि वह सुविधाजनक आसन के अनुसार आसीन होकर काया, सिर, गर्दन को समरेखा में रखते हुए अचल रहे । वह अपनी दृष्टि नासाग्र रखकर निर्भय होते हुए अपनी अन्तःकरण की वृत्तियों को शान्त रखे तथा संयमित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे और मन को संयमित करके अपने आपको मुक्त करता हुआ ध्यानयोग में लीन हो जाय । ऐसे परम निर्वाण शान्त स्वरूप को प्राप्त योगी ही योगी है । अतः योगाभ्यास करने के लिए शारीरिक समस्त चेष्टाओं को शान्त करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं में समता रहने पर ही मन में एकाग्रता की प्रतिष्ठा होती है। इसी सन्दर्भ में आहार, शयन, रहन-सहन, जागरण आदि क्रियाओं को यथायोग्य समप्रमाणित करने का भी निर्देश है । 3 तेरहवें अध्याय के ८ से १२ तक के श्लोकों में ज्ञान के लक्षण बताते हुए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्योपासना, शुचिता, स्थिरता, आत्मनिग्रह, आदि गुणों की चर्चा है । ये सभी नैतिक गुण आत्मा को ऊपर उठानेवाले हैं । १३वें और १४वें अध्याय में आत्मा का स्वरूप और संसार के साथ उसके संबंध का वर्णन है । १५ वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का प्ररूपण है जिसमें पुरुषोत्तम का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम अनुभूति है तथा यह प्राप्त करने के लिए साधक को श्रद्धाशील बनने का विधान है; क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान एवं कर्म व्यर्थ है । श्रद्धा के स्वरूप एवं उसके विविध भेदों का वर्णन १७ वें अध्याय में है ।
इस प्रकार गीता में प्रत्येक योग का वास्तविक अथवा स्वरूप भूत लक्षण वर्णित है और हर हालत में आत्मसंयम, कामनात्याग, प्राणि
१. गीता, २।४८
२. गीता का व्यवहारदर्शन, पृ० २१८
२
Jain Education International
३. वही, पृ० २२२
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org