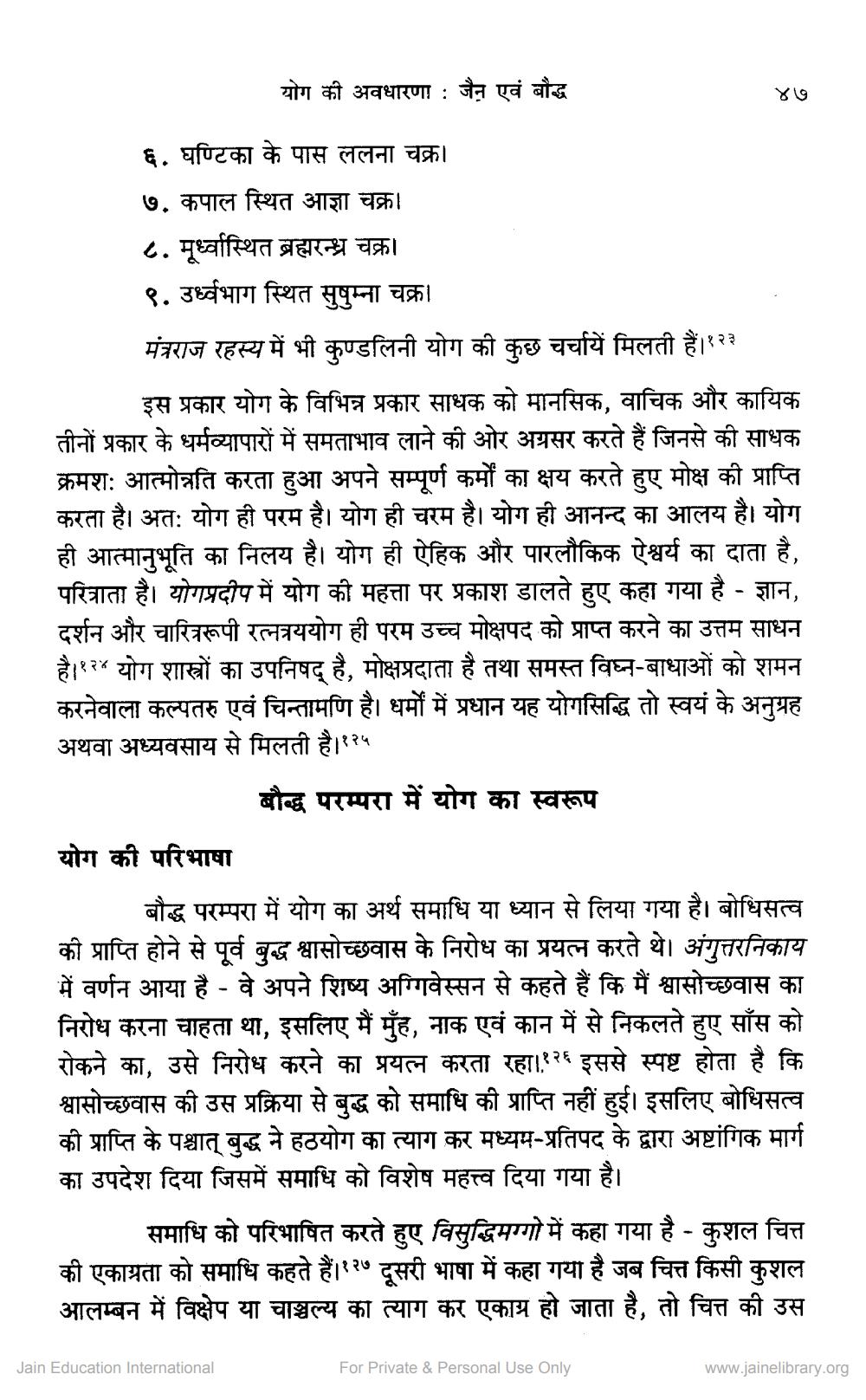________________
योग की अवधारणा : जैन एवं बौद्ध
६. घण्टिका के पास ललना चक्र ।
७. कपाल स्थित आज्ञा चक्र ।
८. मूर्ध्वास्थित ब्रह्मरन्ध्र चक्र ।
९. उर्ध्वभाग स्थित सुषुम्ना चक्र ।
मंत्रराज रहस्य में भी कुण्डलिनी योग की कुछ चर्चायें मिलती हैं । १२३
इस प्रकार योग के विभिन्न प्रकार साधक को मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार के धर्मव्यापारों में समताभाव लाने की ओर अग्रसर करते हैं जिनसे की साधक क्रमशः आत्मोन्नति करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। अतः योग ही परम है। योग ही चरम है। योग ही आनन्द का आलय है। योग ही आत्मानुभूति का निलय है। योग ही ऐहिक और पारलौकिक ऐश्वर्य का दाता है, परित्राता है। योगप्रदीप में योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है - ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी रत्नत्रययोग ही परम उच्च मोक्षपद को प्राप्त करने का उत्तम साधन है । १२४ योग शास्त्रों का उपनिषद् है, मोक्षप्रदाता है तथा समस्त विघ्न-बाधाओं को शमन करनेवाला कल्पतरु एवं चिन्तामणि है। धर्मों में प्रधान यह योगसिद्धि तो स्वयं के अनुग्रह अथवा अध्यवसाय से मिलती है । १२५
बौद्ध परम्परा में योग का स्वरूप
४७
योग की परिभाषा
बौद्ध परम्परा में योग का अर्थ समाधि या ध्यान से लिया गया है। बोधिसत्व की प्राप्ति होने से पूर्व बुद्ध श्वासोच्छवास के निरोध का प्रयत्न करते थे । अंगुत्तरनिकाय में वर्णन आया है - वे अपने शिष्य अग्गिवेस्सन से कहते हैं कि मैं श्वासोच्छवास का निरोध करना चाहता था, इसलिए मैं मुँह, नाक एवं कान में से निकलते हुए साँस को रोकने का उसे निरोध करने का प्रयत्न करता रहा । १२६ इससे स्पष्ट होता है कि श्वासोच्छवास की उस प्रक्रिया से बुद्ध को समाधि की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए बोधिसत्व की प्राप्ति के पश्चात् बुद्ध ने हठयोग का त्याग कर मध्यम- प्रतिपद के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जिसमें समाधि को विशेष महत्त्व दिया गया है।
Jain Education International
समाधि को परिभाषित करते हुए विसुद्धिमग्गो में कहा गया है - कुशल चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं । ' | १२७ दूसरी भाषा में कहा गया है जब चित्त किसी कुशल आलम्बन में विक्षेप या चाञ्चल्य का त्याग कर एकाग्र हो जाता है, तो चित्त की उस
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org