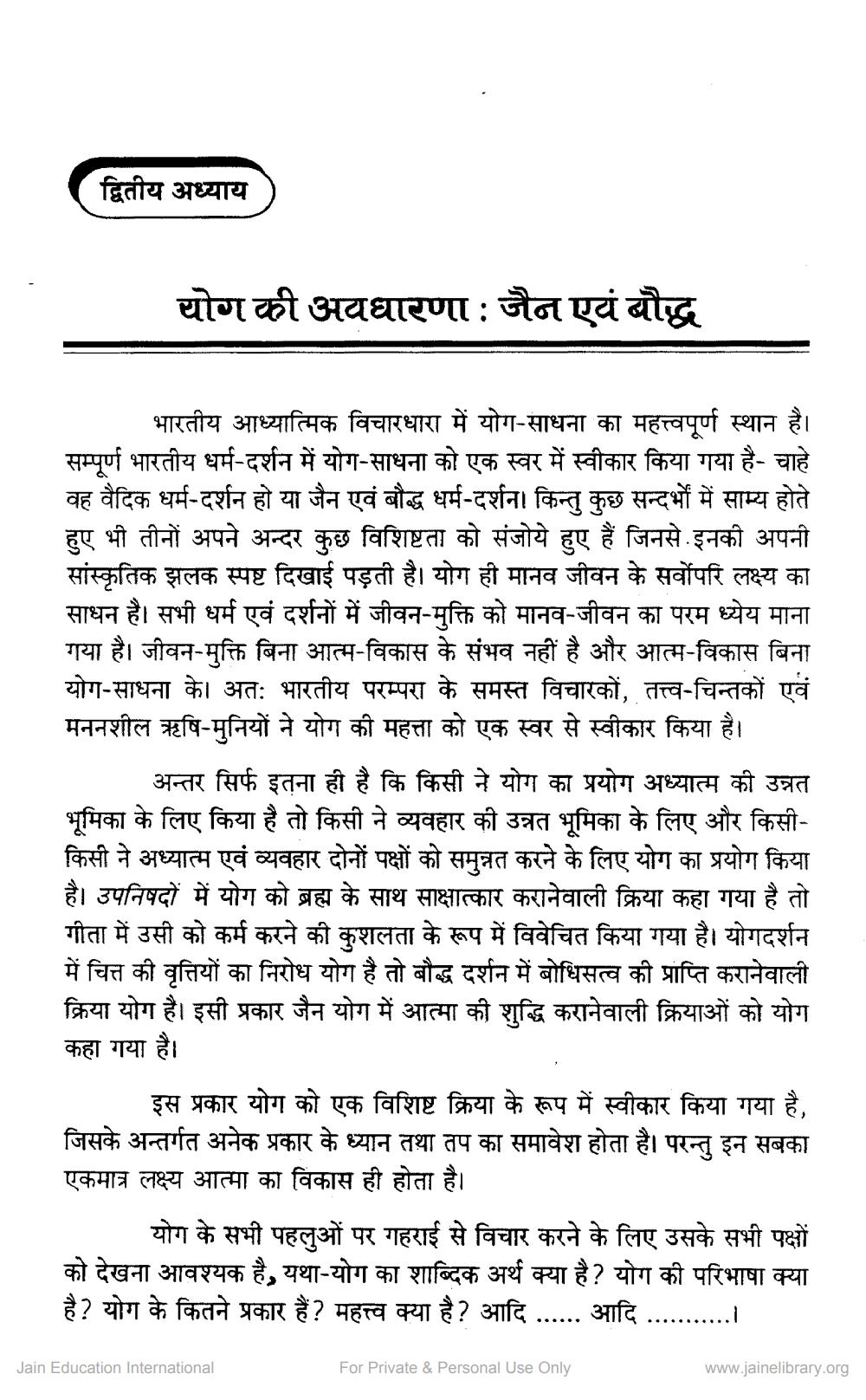________________
द्वितीय अध्याय
योग की अवधारणा : जैन एवं बौद्ध
भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा में योग-साधना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण भारतीय धर्म-दर्शन में योग-साधना को एक स्वर में स्वीकार किया गया है - चाहे वह वैदिक धर्म-दर्शन हो या जैन एवं बौद्ध धर्म-दर्शन । किन्तु कुछ सन्दर्भों में साम्य होते हुए भी तीनों अपने अन्दर कुछ विशिष्टता को संजोये हुए हैं जिनसे इनकी अपनी सांस्कृतिक झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। योग ही मानव जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य का साधन है। सभी धर्म एवं दर्शनों में जीवन-मुक्ति को मानव-जीवन का परम ध्येय माना गया है । जीवन - मुक्ति बिना आत्म-विकास के संभव नहीं है और आत्म-विकास बिना योग-साधना के। अतः भारतीय परम्परा के समस्त विचारकों, तत्त्व- -चिन्तकों एवं मननशील ऋषि-मुनियों ने योग की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार किया है।
अन्तर सिर्फ इतना ही है कि किसी ने योग का प्रयोग अध्यात्म की उन्नत भूमिका के लिए किया है तो किसी ने व्यवहार की उन्नत भूमिका के लिए और किसीकिसी ने अध्यात्म एवं व्यवहार दोनों पक्षों को समुन्नत करने के लिए योग का प्रयोग किया है। उपनिषदों में योग को ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करानेवाली क्रिया कहा गया है तो गीता में उसी को कर्म करने की कुशलता के रूप में विवेचित किया गया है। योगदर्शन में चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है तो बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व की प्राप्ति करानेवाली क्रिया योग है। इसी प्रकार जैन योग में आत्मा की शुद्धि करानेवाली क्रियाओं को योग कहा गया है।
इस प्रकार योग को एक विशिष्ट क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के ध्यान तथा तप का समावेश होता है । परन्तु इन सबका एकमात्र लक्ष्य आत्मा का विकास ही होता है।
योग के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए उसके सभी पक्षों को देखना आवश्यक है, यथा-योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग की परिभाषा क्या है? योग के कितने प्रकार हैं ? महत्त्व क्या है ? आदि आदि ......
Jain Education International
......
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org