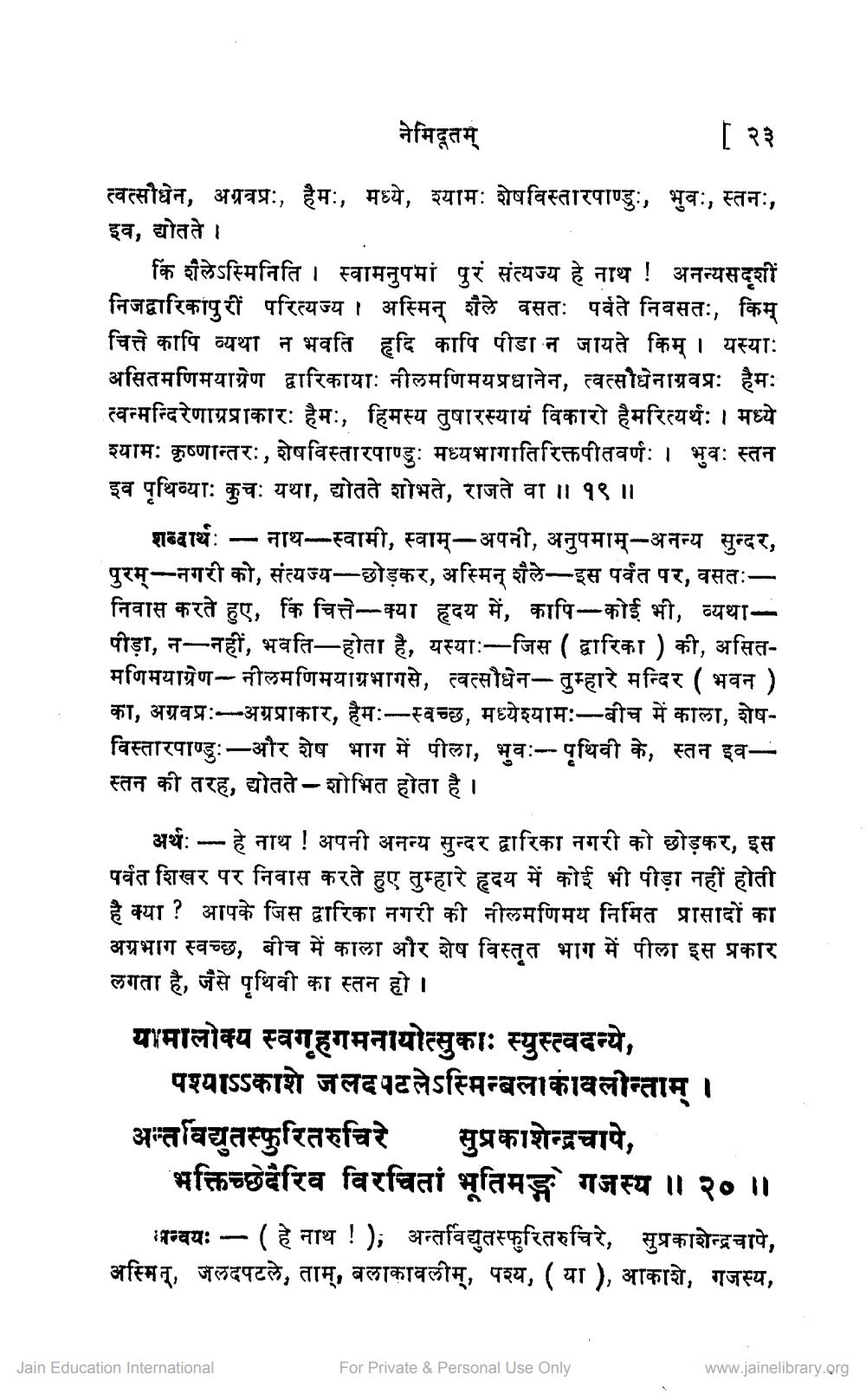________________
नेमिदूतम्
[ २३
त्वत्सोधेन, अग्रवप्रः, हैम:, मध्ये, श्यामः शेषविस्तारपाण्डुः, भुवः, स्तनः, इव, द्योतते ।
किं शैलेऽस्मिनिति । स्वामनुपमां पुरं संत्यज्य हे नाथ ! अनन्यसदृशीं निजद्वारिकापुरी परित्यज्य । अस्मिन् शैले वसतः पर्वते निवसतः, किम् चित्ते कापि व्यथा न भवति हृदि कापि पीडा न जायते किम् । यस्या: असितमणिमयाग्रेण द्वारिकायाः नीलमणिमयप्रधानेन त्वत्सौधनाग्रवप्र: हैम: त्वन्मन्दिरेणाग्रप्राकार: हैम:, हिमस्य तुषारस्यायं विकारो हैमरित्यर्थः । मध्ये श्यामः कृष्णान्तरः, शेषविस्तारपाण्डुः मध्यभागातिरिक्तपीतवर्णः । भुवः स्तन इव पृथिव्याः कुच: यथा, द्योतते शोभते, राजते वा ॥ १९ ॥
शब्दार्थ : - नाथ - स्वामी, स्वाम् — अपनी, अनुपमाम् - अनन्य सुन्दर, पुरम् - नगरी को, संत्यज्य - छोड़कर, अस्मिन् शैले- इस पर्वत पर, वसतःनिवास करते हुए, किं चित्ते - क्या हृदय में, कापि - कोई भी, व्यथा - पीड़ा, न- नहीं, भवति — होता है, यस्याः - 1 :- जिस ( द्वारिका ) की, असितमणिमयाग्रेण - नीलमणिमयाग्रभागसे, त्वत्सौधेन - तुम्हारे मन्दिर ( भवन ) का, अग्रवप्रः --- अग्रप्राकार, हैमः - स्वच्छ, मध्येश्यामः -बीच में काला, शेषविस्तारपाण्डुः — और शेष भाग में पीला, भुवः - पृथिवी के, स्तन इवस्तन की तरह, द्योतते - शोभित होता है ।
अर्थ: हे नाथ ! अपनी अनन्य सुन्दर द्वारिका नगरी को छोड़कर, इस पर्वत शिखर पर निवास करते हुए तुम्हारे हृदय में कोई भी पीड़ा नहीं होती है क्या ? आपके जिस द्वारिका नगरी की नीलमणिमय निर्मित प्रासादों का अग्रभाग स्वच्छ, बीच में काला और शेष विस्तृत भाग में पीला इस प्रकार लगता है, जैसे पृथिवी का स्तन हो ।
-
यामालोक्य स्वगृहगमनायोत्सुकाः स्युस्त्वदन्ये,
पश्याकाशे जलद पटलेऽस्मिन्बला कावलीन्ताम् । सुप्रकाशेन्द्रचापे,
अन्तविद्युतस्फुरितरुचिरे
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्ग गजस्य ॥ २० ॥
अन्वयः ( हे नाथ ! ), अन्तर्विद्युतस्फुरितरुचिरे, सुप्रकाशेन्द्रचापे, अस्मिन् जलदपटले, ताम्, बलाकावलीम्, पश्य, (या ), आकाशे, गजस्य,
Jain Education International
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org