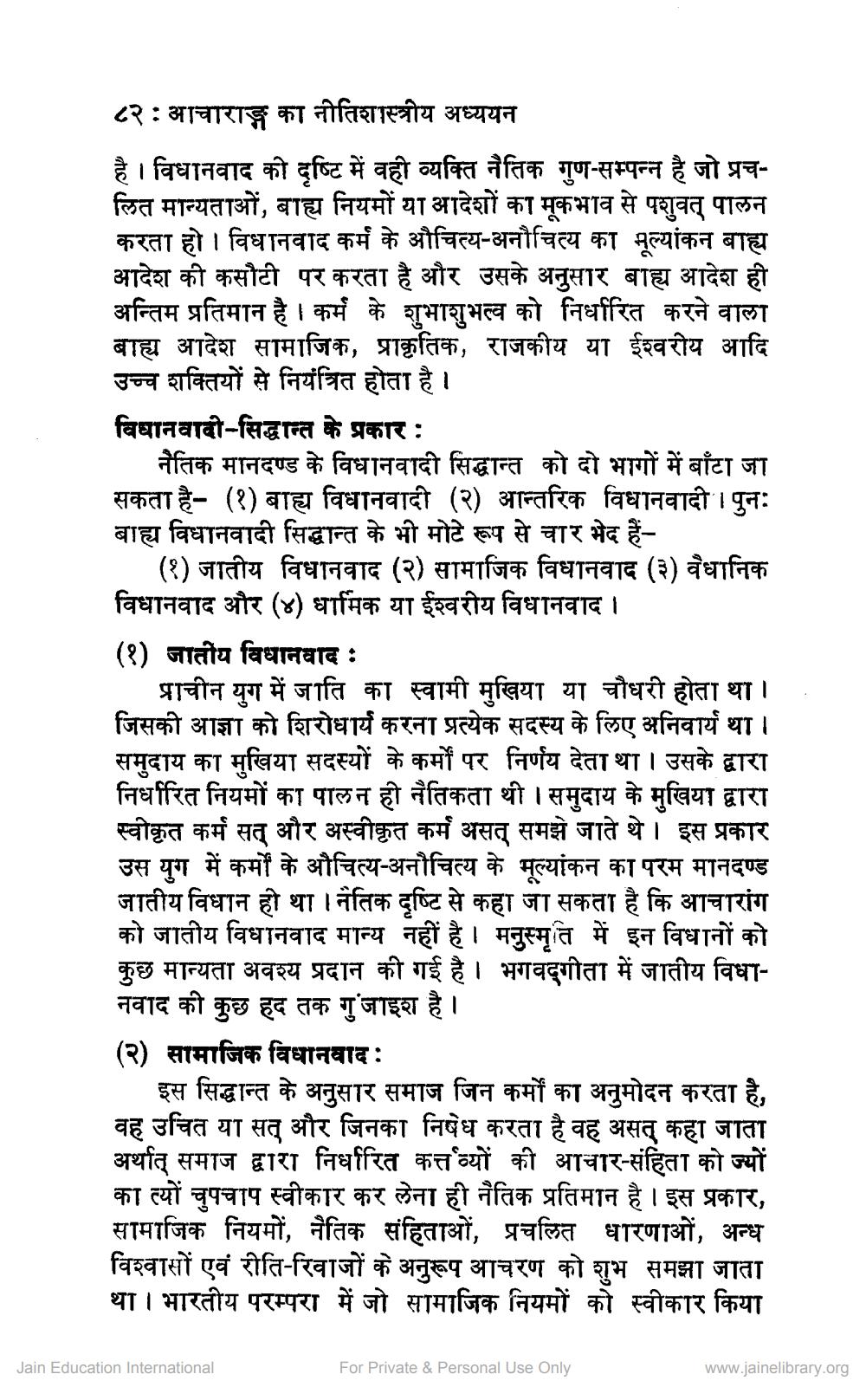________________
८२ : आचाराङ्ग का नीतिशास्त्रीय अध्ययन
है । विधानवाद की दृष्टि में वही व्यक्ति नैतिक गुण सम्पन्न है जो प्रचलित मान्यताओं, बाह्य नियमों या आदेशों का मूकभाव से पशुवत् पालन करता हो । विधानवाद कर्म के औचित्य - अनौचित्य का मूल्यांकन बाह्य आदेश की कसौटी पर करता है और उसके अनुसार बाह्य आदेश ही अन्तिम प्रतिमान है । कर्म के शुभाशुभत्व को निर्धारित करने वाला बाह्य आदेश सामाजिक, प्राकृतिक, राजकीय या ईश्वरीय आदि उच्च शक्तियों से नियंत्रित होता है ।
विधानवादी - सिद्धान्त के प्रकार :
नैतिक मानदण्ड के विधानवादी सिद्धान्त को दो भागों में बाँटा जा सकता है- (१) बाह्य विधानवादी ( २ ) आन्तरिक विधानवादी । पुनः बाह्य विधानवादी सिद्धान्त के भी मोटे रूप से चार भेद हैं
(१) जातीय विधानवाद (२) सामाजिक विधानवाद (३) वैधानिक विधानवाद और (४) धार्मिक या ईश्वरीय विधानवाद ।
(१) जातीय विधानवाद :
प्राचीन युग में जाति का स्वामी मुखिया या चौधरी होता था । जिसकी आज्ञा को शिरोधार्य करना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य था । समुदाय का मुखिया सदस्यों के कर्मों पर निर्णय देता था । उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन ही नैतिकता थी । समुदाय के मुखिया द्वारा स्वीकृत कर्म सत् और अस्वीकृत कर्म असत् समझे जाते थे । इस प्रकार उस युग में कर्मों के औचित्य - अनौचित्य के मूल्यांकन का परम मानदण्ड जातीय विधान ही था । नैतिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि आचारांग को जातीय विधानवाद मान्य नहीं है । मनुस्मृति में इन विधानों को कुछ मान्यता अवश्य प्रदान की गई है । भगवद्गीता में जातीय विधानवाद की कुछ हद तक गुजाइश है ।
(२) सामाजिक विधानवाद :
इस सिद्धान्त के अनुसार समाज जिन कर्मों का अनुमोदन करता है, वह उचित या सत् और जिनका निषेध करता है वह असत् कहा जाता अर्थात् समाज द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों की आचार संहिता को ज्यों का त्यों चुपचाप स्वीकार कर लेना ही नैतिक प्रतिमान है । इस प्रकार, सामाजिक नियमों, नैतिक संहिताओं, प्रचलित धारणाओं, अन्ध विश्वासों एवं रीति-रिवाजों के अनुरूप आचरण को शुभ समझा जाता था । भारतीय परम्परा में जो सामाजिक नियमों को स्वीकार किया
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org