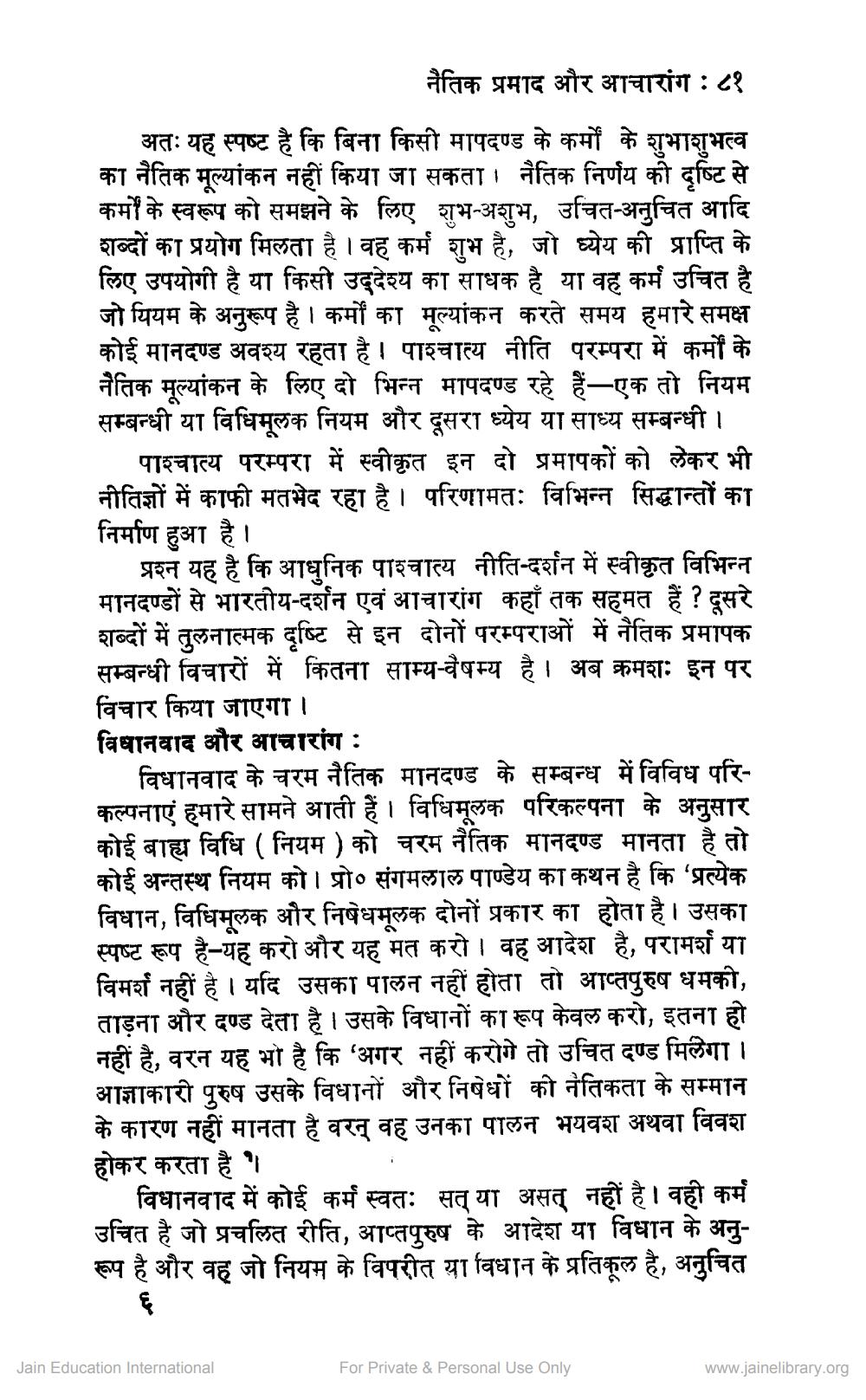________________
नैतिक प्रमाद और आचारांग : ८१
अतः यह स्पष्ट है कि बिना किसी मापदण्ड के कर्मों के शुभाशुभत्व का नैतिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नैतिक निर्णय की दृष्टि से कर्मों के स्वरूप को समझने के लिए शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है । वह कर्म शुभ है, जो ध्येय की प्राप्ति के लिए उपयोगी है या किसी उद्देश्य का साधक है या वह कर्म उचित है जो यियम के अनुरूप है । कर्मों का मूल्यांकन करते समय हमारे समक्ष कोई मानदण्ड अवश्य रहता है । पाश्चात्य नीति परम्परा में कर्मों के नैतिक मूल्यांकन के लिए दो भिन्न मापदण्ड रहे हैं - एक तो नियम सम्बन्धी या विधिमूलक नियम और दूसरा ध्येय या साध्य सम्बन्धी ।
पाश्चात्य परम्परा में स्वीकृत इन दो प्रमापकों को लेकर भी नीतिज्ञों में काफी मतभेद रहा है । परिणामतः विभिन्न सिद्धान्तों का निर्माण हुआ है ।
प्रश्न यह है कि आधुनिक पाश्चात्य नीति-दर्शन में स्वीकृत विभिन्न मानदण्डों से भारतीय-दर्शन एवं आचारांग कहाँ तक सहमत हैं ? दूसरे शब्दों में तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों परम्पराओं में नैतिक प्रमापक सम्बन्धी विचारों में कितना साम्य-वैषम्य है । अब क्रमशः इन पर विचार किया जाएगा ।
विधानवाद और आचारांग :
विधानवाद के चरम नैतिक मानदण्ड के सम्बन्ध में विविध परिकल्पनाएं हमारे सामने आती हैं । विधिमूलक परिकल्पना के अनुसार विधि (नियम ) को चरम नैतिक मानदण्ड मानता है तो कोई अन्तस्थ नियम को । प्रो० संगमलाल पाण्डेय का कथन है कि 'प्रत्येक विधान, विधिमूलक और निषेधमूलक दोनों प्रकार का होता है । उसका स्पष्ट रूप है - यह करो और यह मत करो । वह आदेश है, परामर्श या विमर्श नहीं है । यदि उसका पालन नहीं होता तो आप्तपुरुष धमकी, ताड़ना और दण्ड देता है । उसके विधानों का रूप केवल करो, इतना ही नहीं है, वरन यह भी है कि 'अगर नहीं करोगे तो उचित दण्ड मिलेगा । आज्ञाकारी पुरुष उसके विधानों और निषेधों की नैतिकता के सम्मान के कारण नहीं मानता है वरन् वह उनका पालन भयवश अथवा विवश होकर करता है ।
T
विधानवाद में कोई कर्म स्वतः सत् या असत् नहीं है । वही कर्म उचित है जो प्रचलित रीति, आप्तपुरुष के आदेश या विधान के अनुरूप है और वह जो नियम के विपरीत या विधान के प्रतिकूल है, अनुचित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org