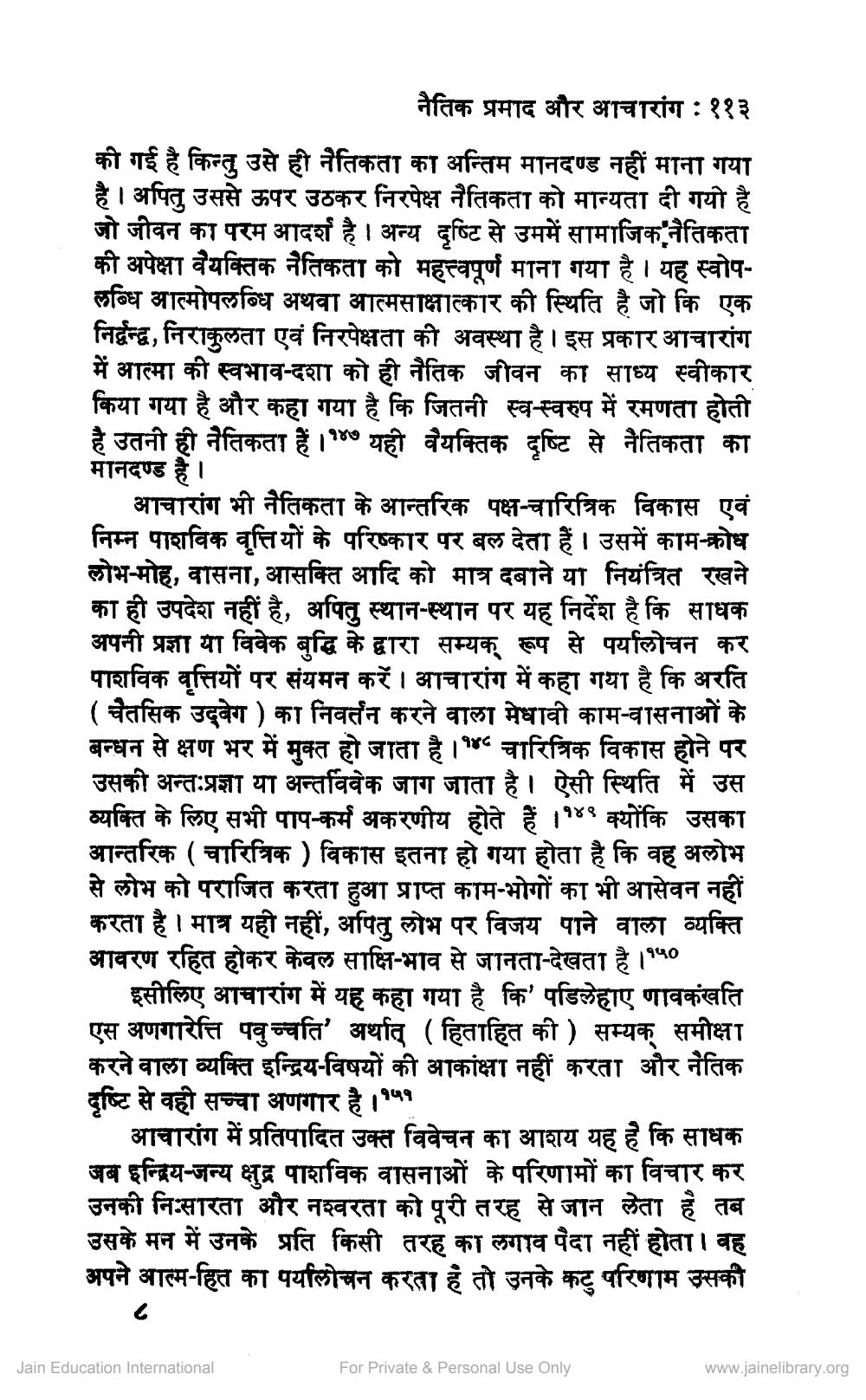________________
नैतिक प्रमाद और आचारांग : ११३ की गई है किन्तु उसे ही नैतिकता का अन्तिम मानदण्ड नहीं माना गया है। अपितु उससे ऊपर उठकर निरपेक्ष नैतिकता को मान्यता दी गयो है जो जीवन का परम आदर्श है । अन्य दृष्टि से उममें सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा वैयक्तिक नैतिकता को महत्त्वपूर्ण माना गया है । यह स्वोपलब्धि आत्मोपलब्धि अथवा आत्मसाक्षात्कार की स्थिति है जो कि एक निर्द्वन्द्व, निराकुलता एवं निरपेक्षता की अवस्था है। इस प्रकार आचारांग में आत्मा की स्वभाव-दशा को ही नैतिक जीवन का साध्य स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि जितनी स्व-स्वरुप में रमणता होती है उतनी ही नैतिकता हैं । १४७ यही वैयक्तिक दृष्टि से नैतिकता का मानदण्ड है। ____ आचारांग भी नैतिकता के आन्तरिक पक्ष-चारित्रिक विकास एवं निम्न पाशविक वृत्तियों के परिष्कार पर बल देता हैं। उसमें काम-क्रोध लोभ-मोह, वासना, आसक्ति आदि को मात्र दबाने या नियंत्रित रखने का ही उपदेश नहीं है, अपितु स्थान-स्थान पर यह निर्देश है कि साधक अपनी प्रज्ञा या विवेक बुद्धि के द्वारा सम्यक् रूप से पर्यालोचन कर पाशविक वृत्तियों पर संयमन करें। आचारांग में कहा गया है कि अरति (चैतसिक उद्वेग ) का निवर्तन करने वाला मेधावी काम-वासनाओं के बन्धन से क्षण भर में मुक्त हो जाता है । चारित्रिक विकास होने पर उसकी अन्तःप्रज्ञा या अन्तविवेक जाग जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए सभी पाप-कर्म अकरणीय होते हैं । १४९ क्योंकि उसका आन्तरिक ( चारित्रिक ) विकास इतना हो गया होता है कि वह अलोभ से लोभ को पराजित करता हुआ प्राप्त काम-भोगों का भी आसेवन नहीं करता है । मात्र यही नहीं, अपितु लोभ पर विजय पाने वाला व्यक्ति आवरण रहित होकर केवल साक्षि-भाव से जानता-देखता है ।१५०
इसीलिए आचारांग में यह कहा गया है कि' पडिलेहाए णावकंखति एस अणगारेत्ति पवुच्चति' अर्थात् (हिताहित की) सम्यक् समीक्षा करने वाला व्यक्ति इन्द्रिय-विषयों की आकांक्षा नहीं करता और नैतिक दृष्टि से वही सच्चा अणगार है ।१५१
आचारांग में प्रतिपादित उक्त विवेचन का आशय यह है कि साधक जब इन्द्रिय-जन्य क्षुद्र पाशविक वासनाओं के परिणामों का विचार कर उनकी निःसारता और नश्वरता को पूरी तरह से जान लेता है तब उसके मन में उनके प्रति किसी तरह का लगाव पैदा नहीं होता। वह अपने आत्म-हित का पर्यालोचन करता है तो उनके कटु परिणाम उसकी
८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org