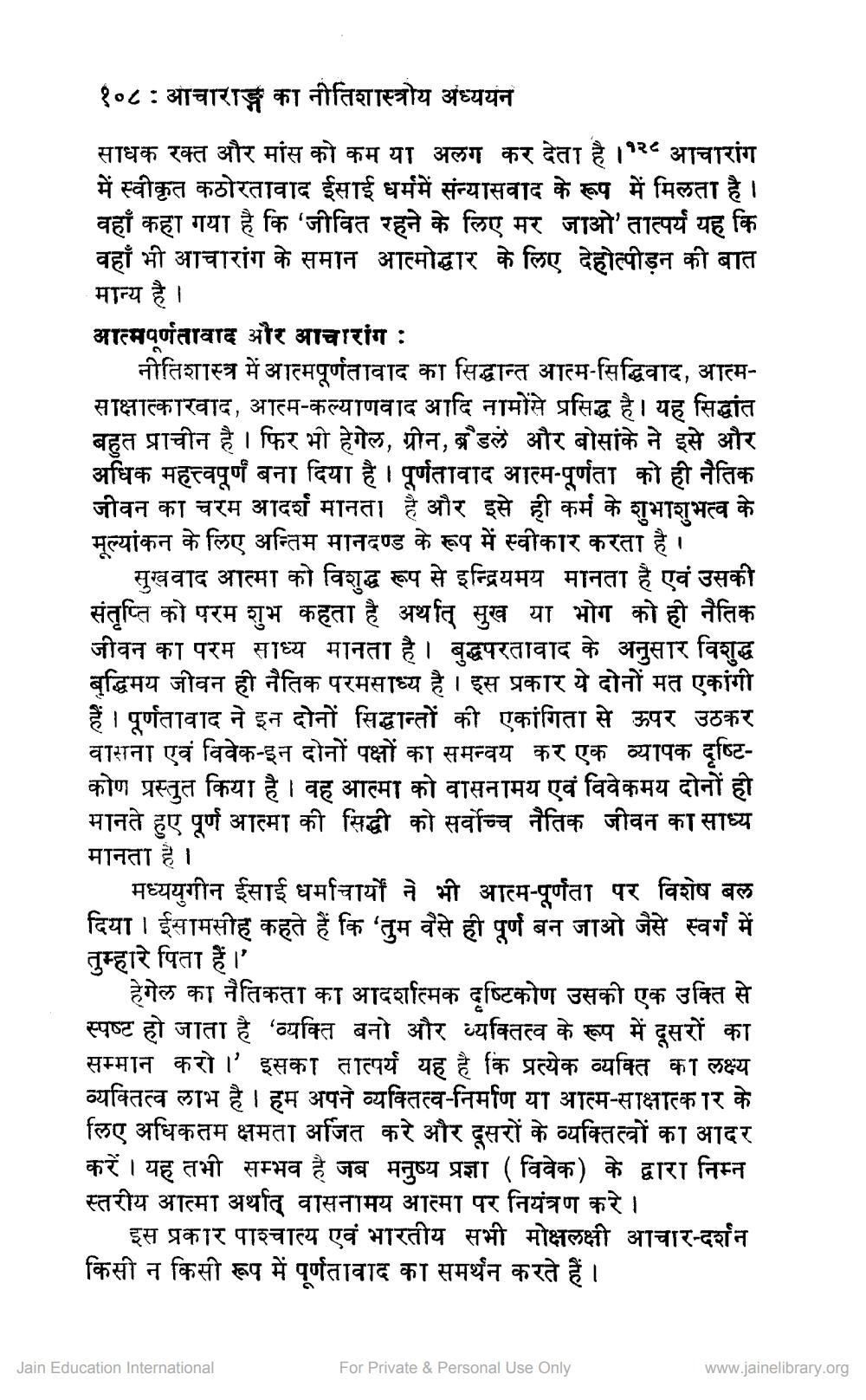________________
१०८ : आचाराङ्ग का नीतिशास्त्रीय अध्ययन
साधक रक्त और मांस को कम या अलग कर देता है ।१२८ आचारांग में स्वीकृत कठोरतावाद ईसाई धर्ममें संन्यासवाद के रूप में मिलता है। वहाँ कहा गया है कि 'जीवित रहने के लिए मर जाओ' तात्पर्य यह कि वहाँ भी आचारांग के समान आत्मोद्धार के लिए देहोत्पीड़न की बात मान्य है। आत्मपूर्णतावाद और आचारांग : __ नीतिशास्त्र में आत्मपूर्णतावाद का सिद्धान्त आत्म-सिद्धिवाद, आत्मसाक्षात्कारवाद, आत्म-कल्याणवाद आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत बहुत प्राचीन है । फिर भी हेगेल, ग्रीन, ब्रडले और बोसांके ने इसे और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। पूर्णतावाद आत्म-पूर्णता को ही नैतिक जीवन का चरम आदर्श मानता है और इसे ही कर्म के शुभाशुभत्व के मूल्यांकन के लिए अन्तिम मानदण्ड के रूप में स्वीकार करता है। __सुखवाद आत्मा को विशुद्ध रूप से इन्द्रियमय मानता है एवं उसकी संतृप्ति को परम शुभ कहता है अर्थात् सुख या भोग को ही नैतिक जीवन का परम साध्य मानता है। बुद्धपरतावाद के अनुसार विशुद्ध बद्धिमय जीवन ही नैतिक परमसाध्य है। इस प्रकार ये दोनों मत एकांगी हैं। पूर्णतावाद ने इन दोनों सिद्धान्तों की एकांगिता से ऊपर उठकर वासना एवं विवेक-इन दोनों पक्षों का समन्वय कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह आत्मा को वासनामय एवं विवेकमय दोनों ही मानते हुए पूर्ण आत्मा की सिद्धी को सर्वोच्च नैतिक जीवन का साध्य मानता है। ____मध्ययुगीन ईसाई धर्माचार्यों ने भी आत्म-पूर्णता पर विशेष बल दिया। ईसामसीह कहते हैं कि 'तुम वैसे ही पूर्ण बन जाओ जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता हैं।'
हेगेल का नैतिकता का आदर्शात्मक दृष्टिकोण उसकी एक उक्ति से स्पष्ट हो जाता है 'व्यक्ति बनो और व्यक्तित्व के रूप में दूसरों का सम्मान करो।' इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य व्यक्तित्व लाभ है। हम अपने व्यक्तित्व-
निर्माण या आत्म-साक्षात्कार के लिए अधिकतम क्षमता अजित करे और दूसरों के व्यक्तित्वों का आदर करें। यह तभी सम्भव है जब मनुष्य प्रज्ञा (विवेक) के द्वारा निम्न स्तरीय आत्मा अर्थात् वासनामय आत्मा पर नियंत्रण करे । __इस प्रकार पाश्चात्य एवं भारतीय सभी मोक्षलक्षी आचार-दर्शन किसी न किसी रूप में पूर्णतावाद का समर्थन करते हैं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org