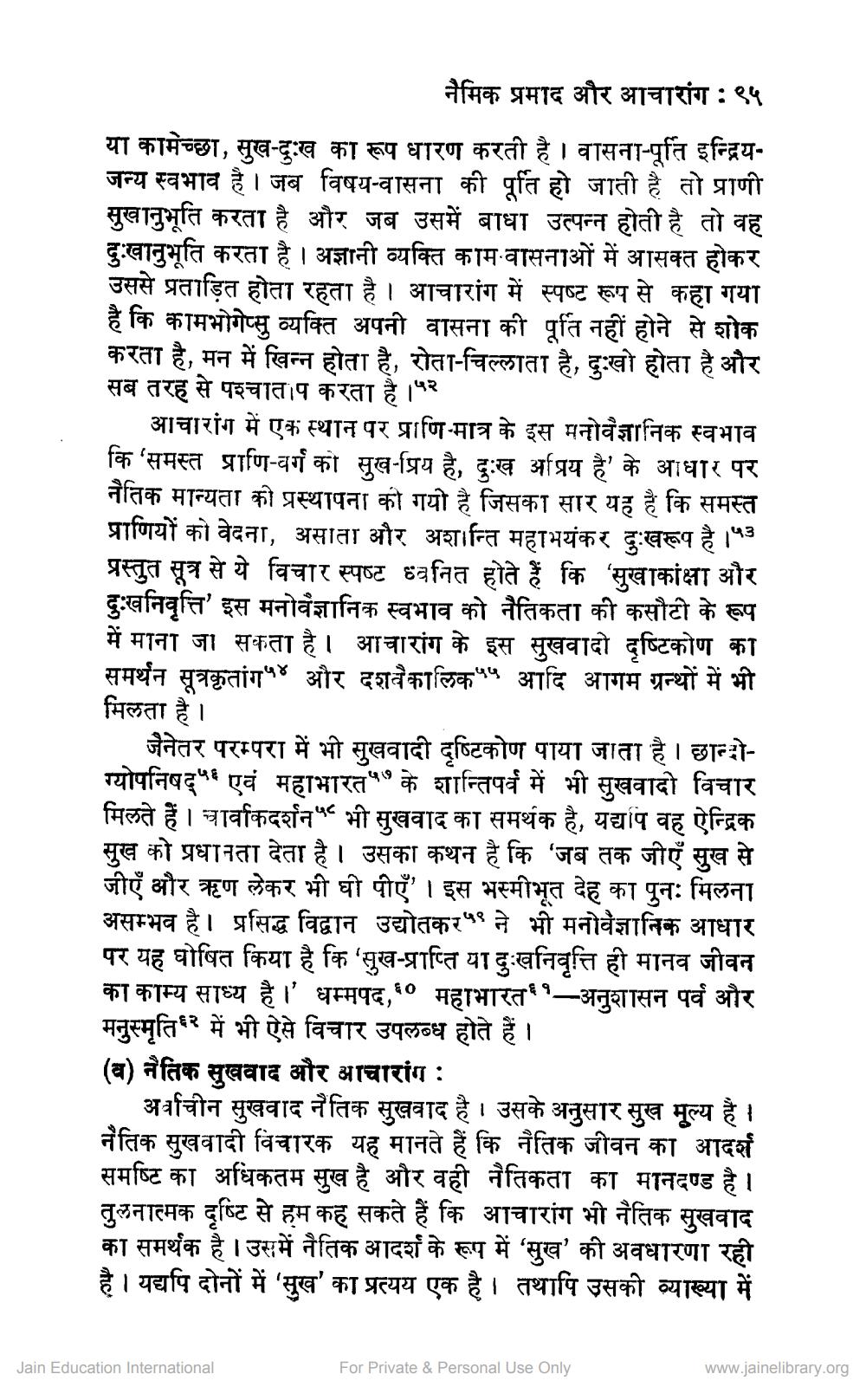________________
नैमिक प्रमाद और आचारांग : ९५
या कामेच्छा, सुख-दुःख का रूप धारण करती है। वासना-पूर्ति इन्द्रियजन्य स्वभाव है । जब विषय-वासना की पूर्ति हो जाती है तो प्राणी सुखानुभूति करता है और जब उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो वह दुःखानुभूति करता है । अज्ञानी व्यक्ति काम वासनाओं में आसक्त होकर उससे प्रताड़ित होता रहता है। आचारांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कामभोगेप्सु व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति नहीं होने से शोक करता है, मन में खिन्न होता है, रोता-चिल्लाता है, दुःखो होता है और सब तरह से पश्चाताप करता है ।५२
आचारांग में एक स्थान पर प्राणि-मात्र के इस मनोवैज्ञानिक स्वभाव कि 'समस्त प्राणि-वर्ग को सुख-प्रिय है, दुःख अप्रिय है' के आधार पर नैतिक मान्यता की प्रस्थापना को गयो है जिसका सार यह है कि समस्त प्राणियों को वेदना, असाता और अशान्ति महाभयंकर दुःखरूप है ।५३ प्रस्तुत सूत्र से ये विचार स्पष्ट ध्वनित होते हैं कि 'सुखाकांक्षा और दुःखनिवृत्ति' इस मनोवैज्ञानिक स्वभाव को नैतिकता की कसौटी के रूप में माना जा सकता है। आचारांग के इस सूखवादो दृष्टिकोण का समर्थन सूत्रकृतांग५४ और दशवैकालिक५५ आदि आगम ग्रन्थों में भी मिलता है।
जैनेतर परम्परा में भी सुखवादी दृष्टिकोण पाया जाता है । छान्दोग्योपनिषद्५६ एवं महाभारत के शान्तिपर्व में भी सुखवादी विचार मिलते हैं। चार्वाकदर्शन भी सुखवाद का समर्थक है, यद्यपि वह ऐन्द्रिक सुख को प्रधानता देता है। उसका कथन है कि 'जब तक जीएँ सुख से जीएँ और ऋण लेकर भी घी पीएँ' । इस भस्मीभूत देह का पुनः मिलना असम्भव है। प्रसिद्ध विद्वान उद्योतकर५९ ने भी मनोवैज्ञानिक आधार पर यह घोषित किया है कि 'सुख-प्राप्ति या दुःखनिवृत्ति ही मानव जीवन का काम्य साध्य है।' धम्मपद,६० महाभारत-अनुशासन पर्व और मनुस्मृति में भी ऐसे विचार उपलब्ध होते हैं। (व) नैतिक सुखवाद और आचारांग :
अर्वाचीन सुखवाद नैतिक सुखवाद है। उसके अनुसार सुख मूल्य है । नैतिक सूखवादी विचारक यह मानते हैं कि नैतिक जीवन का आदर्श समष्टि का अधिकतम सुख है और वही नैतिकता का मानदण्ड है। तुलनात्मक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आचारांग भी नैतिक सुखवाद का समर्थक है । उसमें नैतिक आदर्श के रूप में 'सुख' की अवधारणा रही है । यद्यपि दोनों में 'सुख' का प्रत्यय एक है। तथापि उसकी व्याख्या में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org